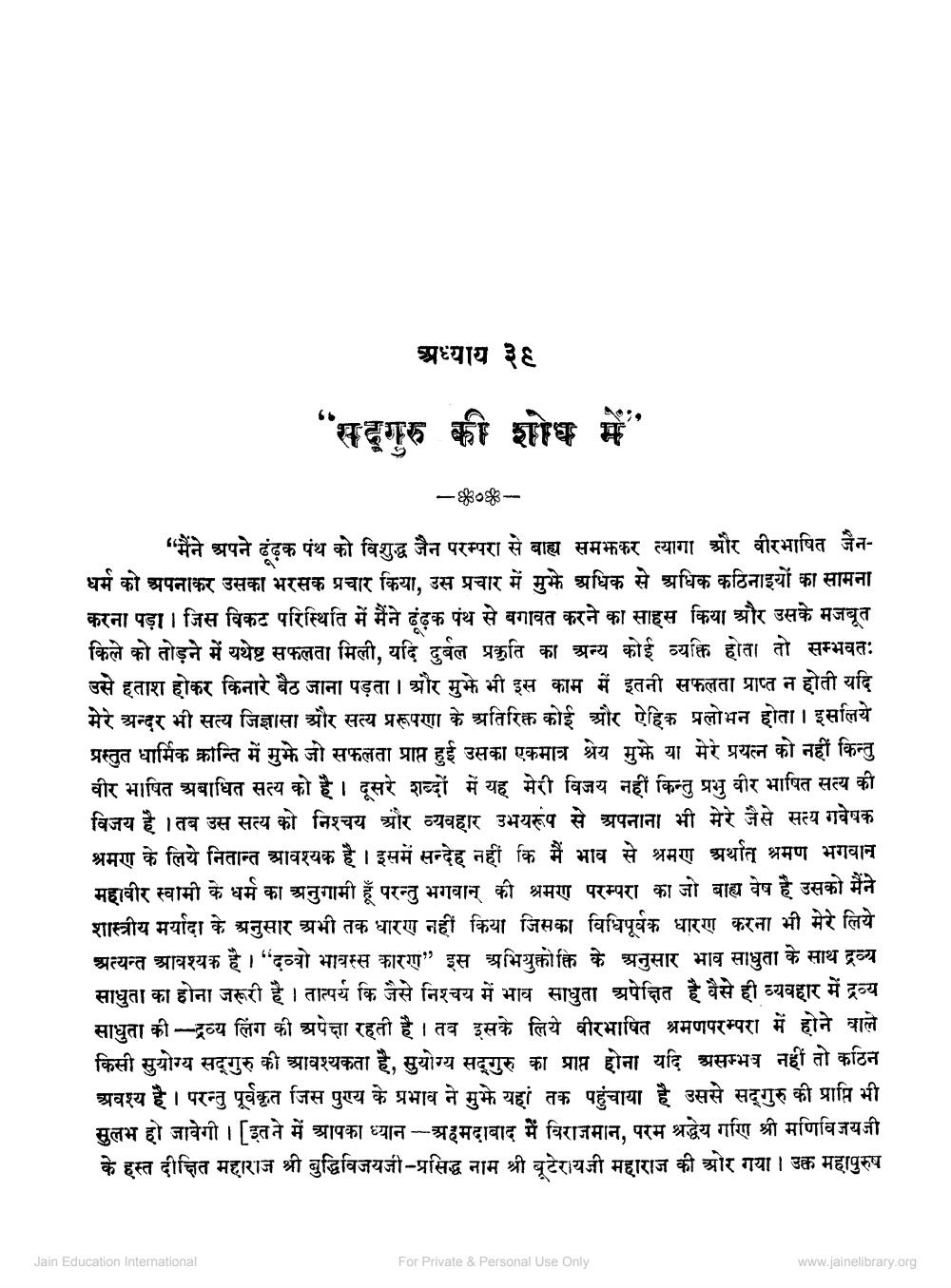________________
अध्याय ३६
"सद्गुरु की शोध में
"मैंने अपने ढूंढ़क पंथ को विशुद्ध जैन परम्परा से बाह्य समझकर त्यागा और वीरभाषित जैनधर्म को अपनाकर उसका भरसक प्रचार किया, उस प्रचार में मुझे अधिक से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जिस विकट परिस्थिति में मैंने ढूंढ़क पंथ से बगावत करने का साहस किया और उसके मजबूत किले को तोड़ने में यथेष्ट सफलता मिली, यदि दुर्बल प्रकृति का अन्य कोई व्यक्ति होता तो सम्भवतः उसे हताश होकर किनारे बैठ जाना पड़ता । और मुझे भी इस काम में इतनी सफलता प्राप्त न होती यदि मेरे अन्दर भी सत्य जिज्ञासा और सत्य प्ररूपणा के अतिरिक्त कोई और ऐहिक प्रलोभन होता । इसलिये प्रस्तुत धार्मिक क्रान्ति में मुझे जो सफलता प्राप्त हुई उसका एकमात्र श्रेय मुझे या मेरे प्रयत्न को नहीं किन्तु वीर भाषित अबाधित सत्य को है। दूसरे शब्दों में यह मेरी विजय नहीं किन्तु प्रभु वीर भाषित सत्य की विजय है । तब उस सत्य को निश्चय और व्यवहार उभयरूप से अपनाना भी मेरे जैसे सत्य गवेषक श्रमण के लिये नितान्त आवश्यक है । इसमें सन्देह नहीं कि मैं भाव से श्रमण अर्थात् श्रमण भगवान महावीर स्वामी के धर्म का अनुगामी हूँ परन्तु भगवान् की श्रमण परम्परा का जो बाह्य वेष है उसको मैंने शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार अभी तक धारण नहीं किया जिसका विधिपूर्वक धारण करना भी मेरे लिये अत्यन्त आवश्यक है । “दव्यो भावस्स कारण" इस अभियुक्तोति के अनुसार भाव साधुता के साथ द्रव्य साधुता का होना जरूरी है । तात्पर्य कि जैसे निश्चय में भाव साधुता अपेक्षित है वैसे ही व्यवहार में द्रव्य साधुता की-द्रव्य लिंग की अपेक्षा रहती है । तव इसके लिये वीरभाषित श्रमणपरम्परा में होने वाले किसी सुयोग्य सद्गुरु की आवश्यकता है, सुयोग्य सद्गुरु का प्राप्त होना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। परन्तु पूर्वकृत जिस पुण्य के प्रभाव ने मुझे यहां तक पहुंचाया है उससे सद्गुरु की प्राप्ति भी सुलभ हो जावेगी। [इतने में आपका ध्यान --अहमदाबाद में विराजमान, परम श्रद्धेय गणि श्री मणिविजयजी के हस्त दीक्षित महाराज श्री बुद्धिविजयजी-प्रसिद्ध नाम श्री बूटेरायजी महाराज की ओर गया। उक्त महापुरुष
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org