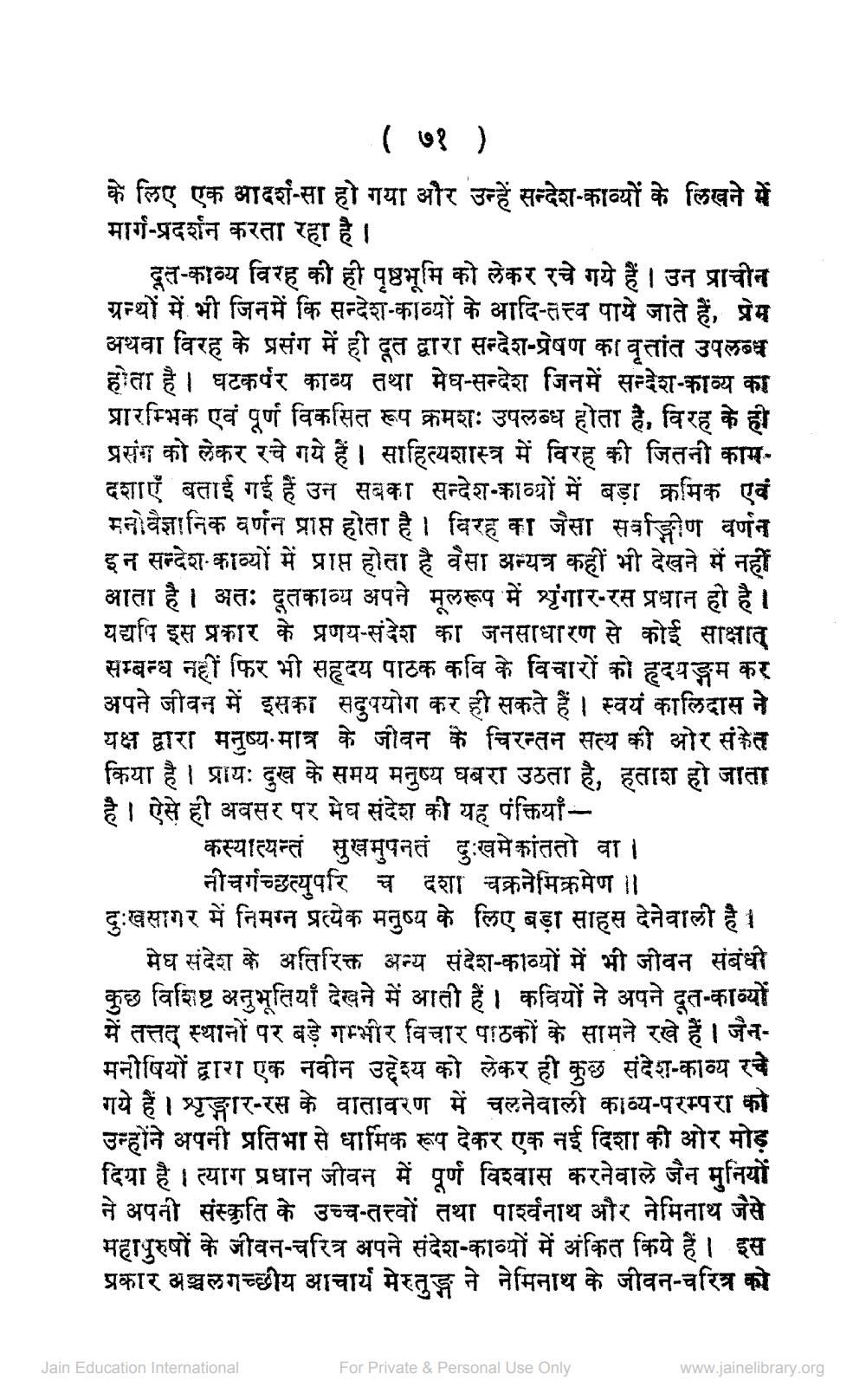________________
( ७१ ) के लिए एक आदर्श-सा हो गया और उन्हें सन्देश-काव्यों के लिखने में मार्ग-प्रदर्शन करता रहा है।
दूत-काव्य विरह की ही पृष्ठभूमि को लेकर रचे गये हैं । उन प्राचीन ग्रन्थों में भी जिनमें कि सन्देश-काव्यों के आदि-तत्त्व पाये जाते हैं, प्रेम अथवा विरह के प्रसंग में ही दूत द्वारा सन्देश-प्रेषण का वृत्तांत उपलब्ध होता है। घटकर्पर काव्य तथा मेघ-सन्देश जिनमें सन्देश-काव्य का प्रारम्भिक एवं पूर्ण विकसित रूप क्रमशः उपलब्ध होता है, विरह के ही प्रसंग को लेकर रचे गये हैं। साहित्यशास्त्र में विरह की जितनी काम. दशाएं बताई गई हैं उन सबका सन्देश-काव्यों में बड़ा क्रमिक एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन प्राप्त होता है। विरह का जैसा सर्वाङ्गीण वर्णन इन सन्देश काव्यों में प्राप्त होता है वैसा अन्यत्र कहीं भी देखने में नहीं आता है। अतः दूतकाव्य अपने मूलरूप में शृंगार-रस प्रधान हो है। यद्यपि इस प्रकार के प्रणय-संदेश का जनसाधारण से कोई साक्षात् सम्बन्ध नहीं फिर भी सहृदय पाठक कवि के विचारों को हृदयङ्गम कर अपने जीवन में इसका सदुपयोग कर ही सकते हैं। स्वयं कालिदास ने यक्ष द्वारा मनुष्य मात्र के जीवन के चिरन्तन सत्य की ओर संकेत किया है । प्रायः दुख के समय मनुष्य घबरा उठता है, हताश हो जाता है। ऐसे ही अवसर पर मेघ संदेश की यह पंक्तियाँ___कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकांततो वा।
नीचर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।। दुःखसागर में निमग्न प्रत्येक मनुष्य के लिए बड़ा साहस देनेवाली है।
मेघ संदेश के अतिरिक्त अन्य संदेश-काव्यों में भी जीवन संबंधी कुछ विशिष्ट अनुभूतियाँ देखने में आती हैं। कवियों ने अपने दूत-काव्यों में तत्तत् स्थानों पर बड़े गम्भीर विचार पाठकों के सामने रखे हैं। जैनमनीषियों द्वारा एक नवीन उद्देश्य को लेकर ही कुछ संदेश-काव्य रचे गये हैं। शृङ्गार-रस के वातावरण में चलनेवाली काव्य-परम्परा को उन्होंने अपनी प्रतिभा से धार्मिक रूप देकर एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया है । त्याग प्रधान जीवन में पूर्ण विश्वास करनेवाले जैन मुनियों ने अपनी संस्कृति के उच्च-तत्त्वों तथा पार्श्वनाथ और नेमिनाथ जैसे महापुरुषों के जीवन-चरित्र अपने संदेश-काव्यों में अंकित किये हैं। इस प्रकार अञ्चल गच्छीय आचार्य मेस्तुङ्ग ने नेमिनाथ के जीवन-चरित्र को
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org