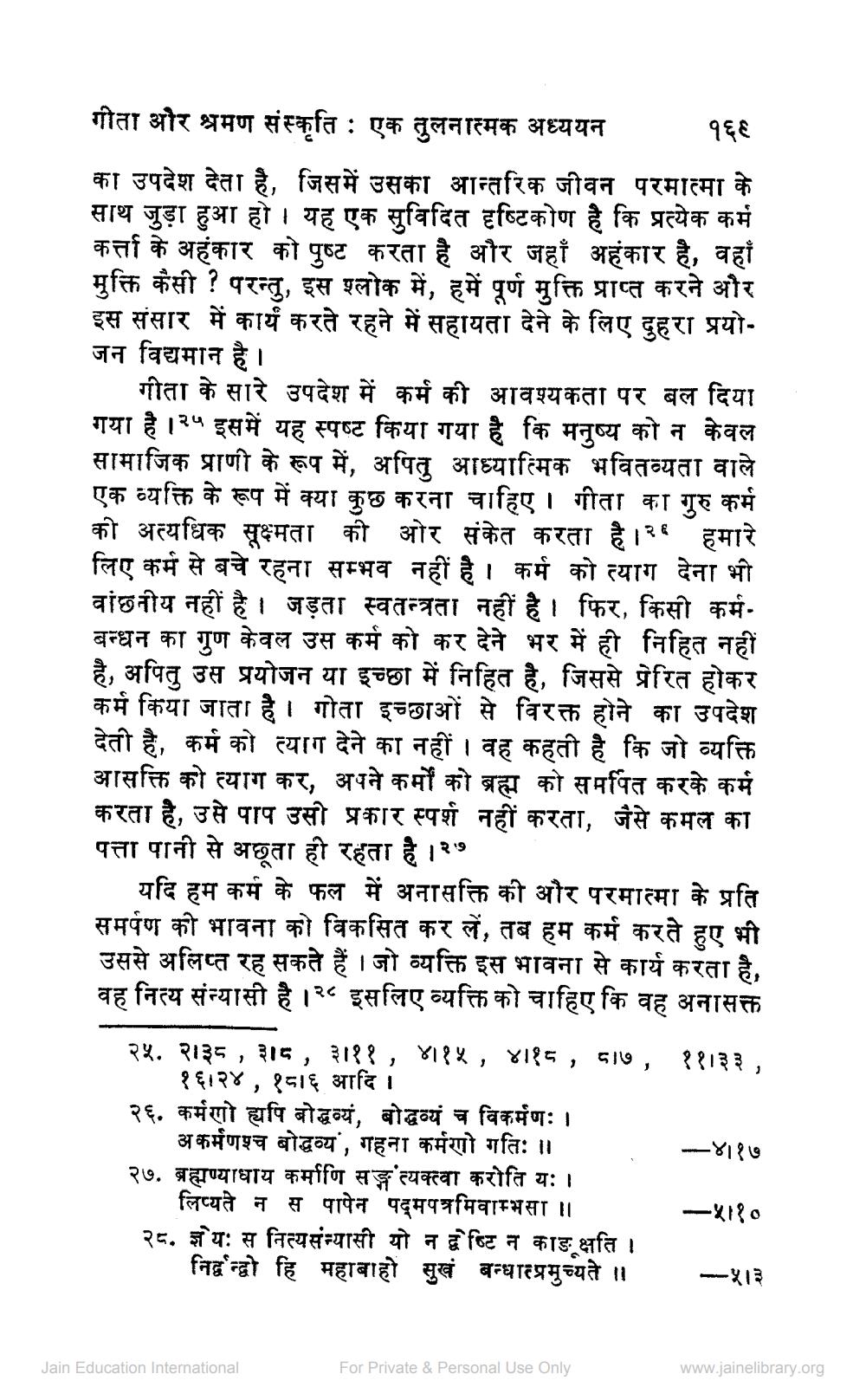________________
गीता और श्रमण संस्कृति : एक तुलनात्मक अध्ययन
१६६
का उपदेश देता है, जिसमें उसका आन्तरिक जीवन परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हो । यह एक सुविदित दृष्टिकोण है कि प्रत्येक कर्म कर्त्ता के अहंकार को पुष्ट करता है और जहाँ अहंकार है, वहाँ मुक्ति कैसी ? परन्तु इस श्लोक में, हमें पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने और इस संसार में कार्यं करते रहने में सहायता देने के लिए दुहरा प्रयोजन विद्यमान है ।
गीता के सारे उपदेश में कर्म की आवश्यकता पर बल दिया गया है । २५ इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य को न केवल सामाजिक प्राणी के रूप में, अपितु आध्यात्मिक भवितव्यता वाले एक व्यक्ति के रूप में क्या कुछ करना चाहिए। गीता का गुरु कर्म की अत्यधिक सूक्ष्मता की ओर संकेत करता है । २६ हमारे लिए कर्म से बचे रहना सम्भव नहीं है । कर्म को त्याग देना भी वांछनीय नहीं है । जड़ता स्वतन्त्रता नहीं है । फिर, किसी कर्मबन्धन का गुण केवल उस कर्म को कर देने भर में ही निहित नहीं है, अपितु उस प्रयोजन या इच्छा में निहित है, जिससे प्रेरित होकर कर्म किया जाता है । गोता इच्छाओं से विरक्त होने का उपदेश देती है, कर्म को त्याग देने का नहीं । वह कहती है कि जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर, अपने कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करके कर्म करता है, उसे पाप उसी प्रकार स्पर्श नहीं करता, जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता ही रहता है । २७
यदि हम कर्म के फल में अनासक्ति की और परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना को विकसित कर लें, तब हम कर्म करते हुए भी उससे अलिप्त रह सकते हैं । जो व्यक्ति इस भावना से कार्य करता है, वह नित्य संन्यासी है । २८ इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अनासक्त
२५. २३८, ३५, ३११, ४१५, ४१८, ८७ ११।३३, १६।२४, १८।६ आदि ।
२६. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं, बोद्धव्यं च विकर्मणः । अकर्मणश्च बोद्धव्यं, गहना कर्मणो गतिः ॥
२७. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः । लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ २८. ज्ञ ेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्व ेष्टि न काङ्क्षति । निर्द्वन्द्वो हि महाबाहों सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
J
-४|१७
- ५1१०
-५/३
www.jainelibrary.org