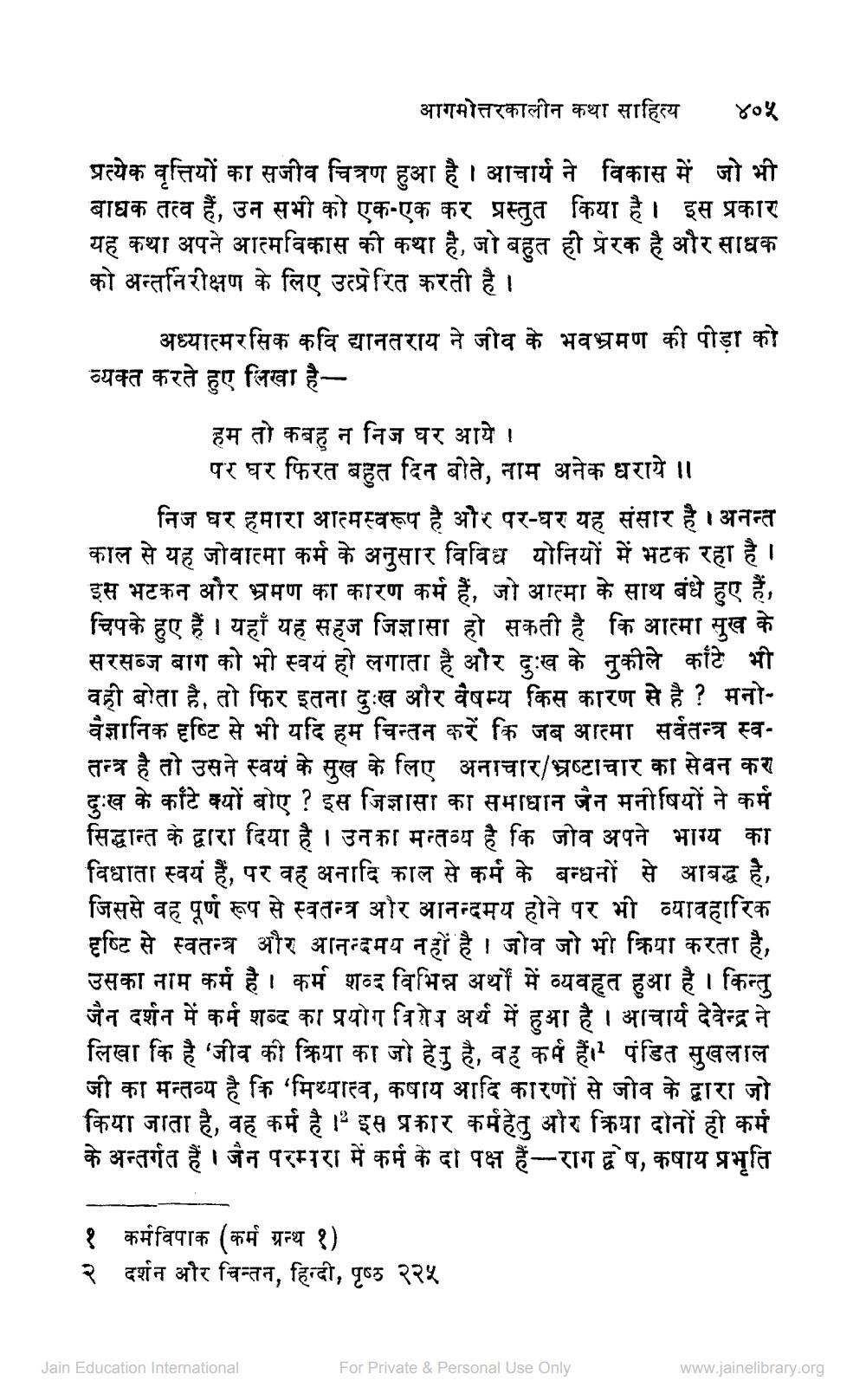________________
आगमोत्तरकालीन कथा साहित्य
४०५
प्रत्येक वृत्तियों का सजीव चित्रण हुआ है । आचार्य ने विकास में जो भी बाधक तत्व हैं, उन सभी को एक-एक कर प्रस्तुत किया है। इस प्रकार यह कथा अपने आत्मविकास की कथा है, जो बहुत ही प्रेरक है और साधक को अन्तनिरीक्षण के लिए उत्प्रेरित करती है।
अध्यात्मरसिक कवि द्यानतराय ने जीव के भवभ्रमण की पीड़ा को व्यक्त करते हुए लिखा है
हम तो कबह न निज घर आये ।
पर घर फिरत बहुत दिन बोते, नाम अनेक धराये ।। निज घर हमारा आत्मस्वरूप है और पर-घर यह संसार है । अनन्त काल से यह जोवात्मा कर्म के अनुसार विविध योनियों में भटक रहा है। इस भटकन और भ्रमण का कारण कर्म हैं, जो आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, चिपके हुए हैं। यहाँ यह सहज जिज्ञासा हो सकती है कि आत्मा सुख के सरसब्ज बाग को भी स्वयं हो लगाता है और दुःख के नुकीले कांटे भी वही बोता है, तो फिर इतना दुःख और वैषम्य किस कारण से है ? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यदि हम चिन्तन करें कि जब आत्मा सर्वतन्त्र स्वतन्त्र है तो उसने स्वयं के सुख के लिए अनाचार/भ्रष्टाचार का सेवन कर दुःख के काँटे क्यों बोए ? इस जिज्ञासा का समाधान जैन मनीषियों ने कर्म सिद्धान्त के द्वारा दिया है । उनका मन्तव्य है कि जोव अपने भाग्य का विधाता स्वयं हैं, पर वह अनादि काल से कर्म के बन्धनों से आबद्ध है, जिससे वह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र और आनन्दमय होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से स्वतन्त्र और आनन्दमय नहीं है। जोव जो भी क्रिया करता है, उसका नाम कर्म है। कर्म शव्द विभिन्न अर्थों में व्यवहृत हुआ है । किन्तु जैन दर्शन में कर्म शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में हुआ है । आचार्य देवेन्द्र ने लिखा कि है ‘जीव की क्रिया का जो हेतु है, वह कर्म हैं। पंडित सुखलाल जी का मन्तव्य है कि 'मिथ्यात्व, कषाय आदि कारणों से जोव के द्वारा जो किया जाता है, वह कर्म है । इस प्रकार कर्म हेतु और क्रिया दोनों ही कर्म के अन्तर्गत हैं । जैन परम्परा में कर्म के दो पक्ष हैं-राग द्वेष, कषाय प्रभृति
१ कर्मविपाक (कर्म ग्रन्थ १) २ दर्शन और चिन्तन, हिन्दी, पृष्ठ २२५
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org