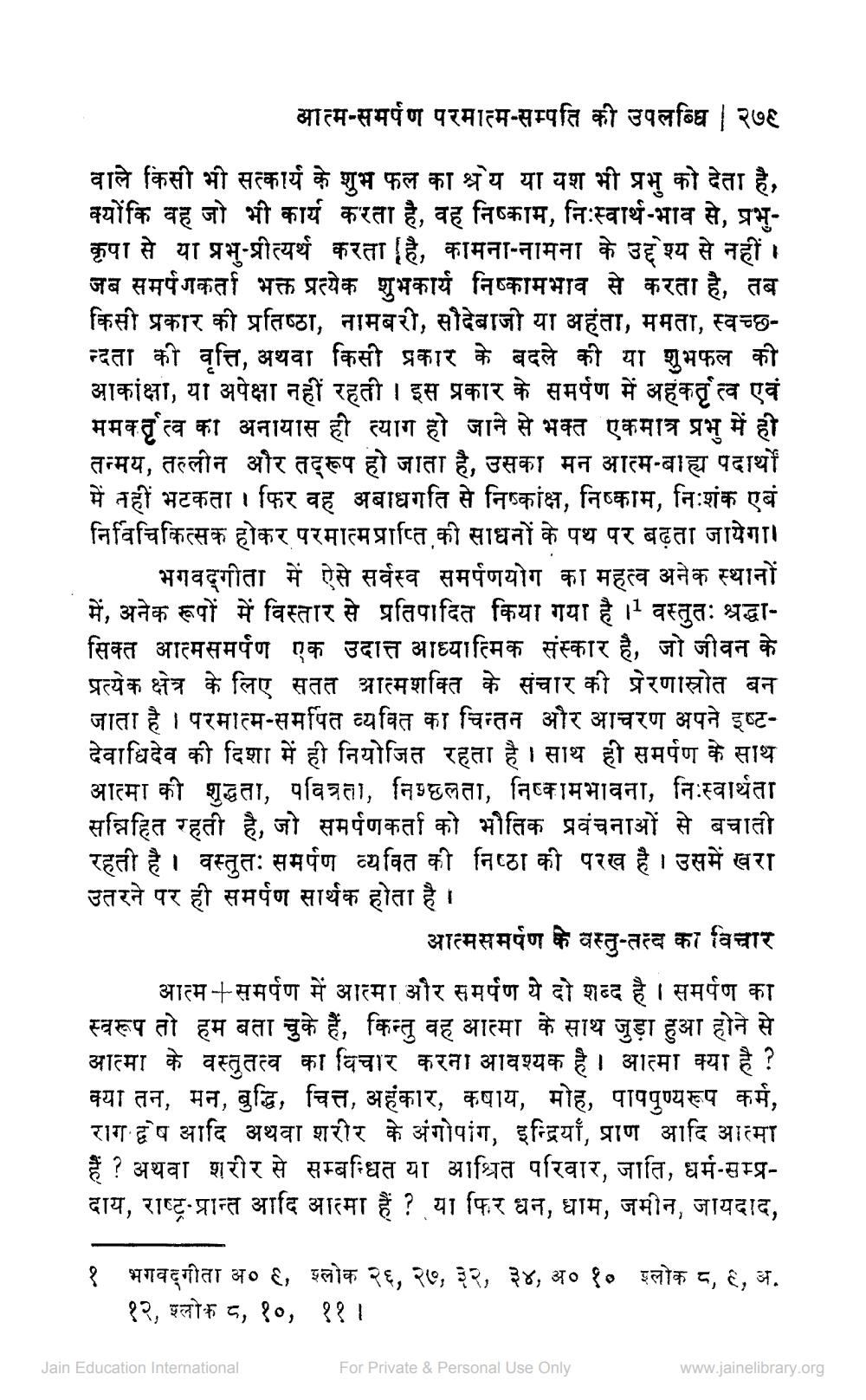________________
आत्म-समर्पण परमात्म-सम्पति की उपलब्धि | २७६
वाले किसी भी सत्कार्य के शुभ फल का श्रेय या यश भी प्रभु को देता है, क्योंकि वह जो भी कार्य करता है, वह निष्काम, निःस्वार्थ-भाव से, प्रभुकृपा से या प्रभु-प्रीत्यर्थ करता है, कामना-नामना के उद्देश्य से नहीं। जब समर्पगकर्ता भक्त प्रत्येक शुभकार्य निष्कामभाव से करता है, तब किसी प्रकार की प्रतिष्ठा, नामबरी, सौदेबाजी या अहंता, ममता, स्वच्छन्दता की वत्ति, अथवा किसी प्रकार के बदले की या शुभफल की आकांक्षा, या अपेक्षा नहीं रहती । इस प्रकार के समर्पण में अहंकर्तृत्व एवं ममकर्तृत्व का अनायास ही त्याग हो जाने से भक्त एकमात्र प्रभु में ही तन्मय, तल्लीन और तद्रूप हो जाता है, उसका मन आत्म-बाह्य पदार्थों में नहीं भटकता। फिर वह अबाधगति से निष्कांक्ष, निष्काम, निःशंक एवं निविचिकित्सक होकर परमात्म प्राप्ति की साधनों के पथ पर बढ़ता जायेगा।
भगवदगीता में ऐसे सर्वस्व समर्पणयोग का महत्व अनेक स्थानों में, अनेक रूपों में विस्तार से प्रतिपादित किया गया है । वस्तुतः श्रद्धासिक्त आत्मसमर्पण एक उदात्त आध्यात्मिक संस्कार है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए सतत आत्मशक्ति के संचार की प्रेरणास्रोत बन जाता है । परमात्म-समर्पित व्यक्ति का चिन्तन और आचरण अपने इष्टदेवाधिदेव की दिशा में ही नियोजित रहता है। साथ ही समर्पण के साथ आत्मा की शुद्धता, पवित्रता, निश्छलता, निष्कामभावना, निःस्वार्थता सन्निहित रहती है, जो समर्पणकर्ता को भौतिक प्रवंचनाओं से बचाती रहती है। वस्तुतः समर्पण व्यक्ति की निष्ठा की परख है । उसमें खरा उतरने पर ही समर्पण सार्थक होता है ।
आत्मसमर्पण के वस्तु-तत्व का विचार आत्म-समर्पण में आत्मा और समर्पण ये दो शब्द है । समर्पण का स्वरूप तो हम बता चुके हैं, किन्तु वह आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होने से आत्मा के वस्तुतत्व का विचार करना आवश्यक है। आत्मा क्या है ? क्या तन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कषाय, मोह, पापपूण्यरूप कर्म, राग द्वेष आदि अथवा शरीर के अंगोपांग, इन्द्रियाँ, प्राण आदि आत्मा हैं ? अथवा शरीर से सम्बन्धित या आश्रित परिवार, जाति, धर्म-सम्प्रदाय, राष्ट्र प्रान्त आदि आत्मा हैं ? या फिर धन, धाम, जमीन, जायदाद,
१ भगवद्गीता अ० ६, श्लोक २६, २७, ३२, ३४, अ० १० श्लोक ८, ६, अ.
१२, श्लोक ८, १०, ११ ।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org