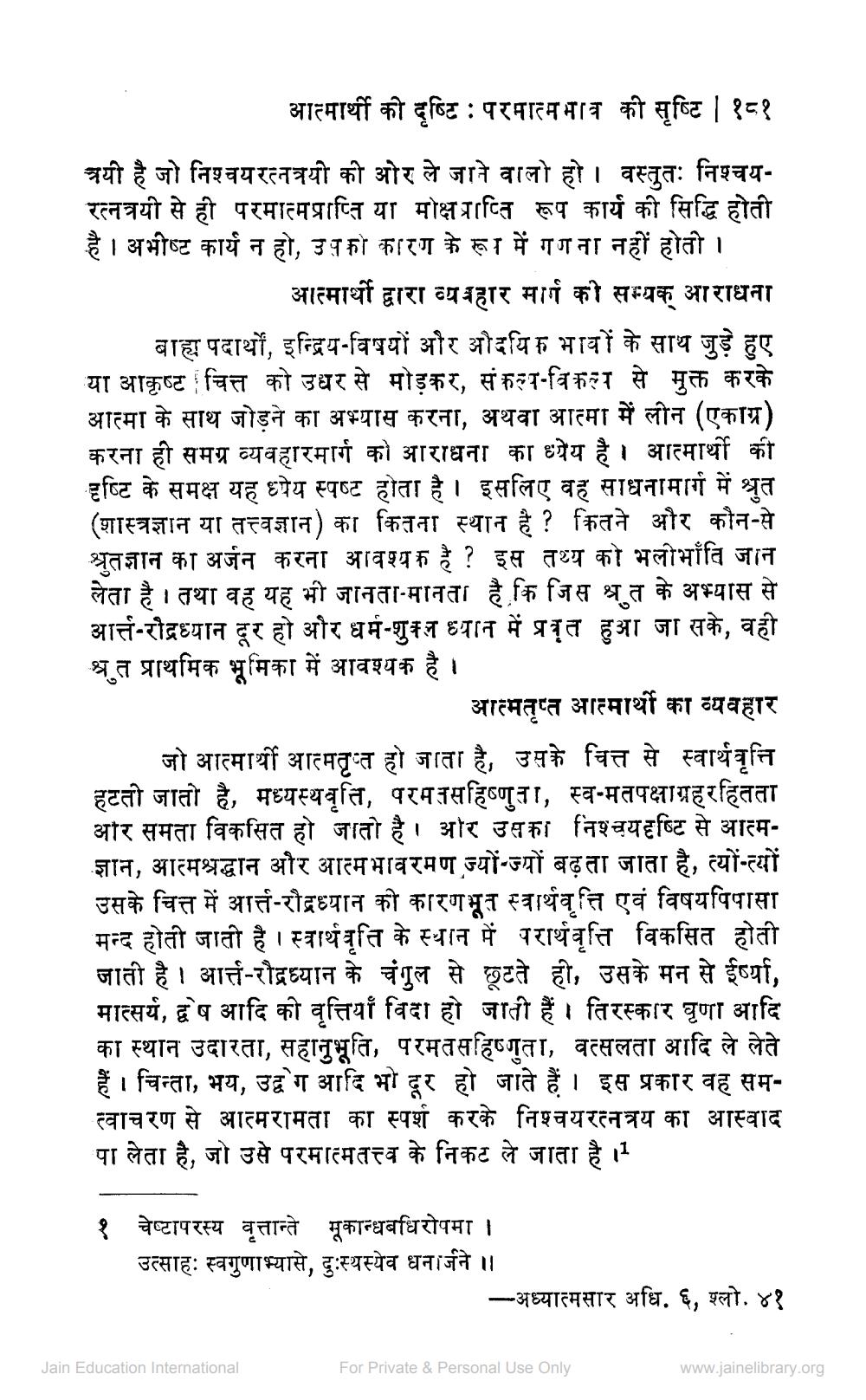________________
आत्मार्थी को दृष्टि : परमात्मभाव की सृष्टि | १८१ त्रयी है जो निश्चयरत्नत्रयो की ओर ले जाने वालो हो । वस्तुतः निश्चयरत्नत्रयी से ही परमात्मप्राप्ति या मोक्षप्राप्ति रूप कार्य की सिद्धि होती है । अभीष्ट कार्य न हो, उसको कारण के रूप में गग ना नहीं होती।
आत्मार्थी द्वारा व्यवहार मार्ग को सम्यक् आराधना बाह्य पदार्थों, इन्द्रिय-विषयों और औदयिक भावों के साथ जुड़े हुए या आकृष्ट चित्त को उधर से मोड़कर, संकल्प-विकल्प से मुक्त करके आत्मा के साथ जोड़ने का अभ्यास करना, अथवा आत्मा में लीन (एकाग्र) करना ही समग्र व्यवहारमार्ग को आराधना का ध्येय है। आत्मार्थो की दृष्टि के समक्ष यह ध्येय स्पष्ट होता है। इसलिए वह साधनामार्ग में श्रुत (शास्त्रज्ञान या तत्त्वज्ञान) का कितना स्थान है ? कितने और कौन-से श्रुतज्ञान का अर्जन करना आवश्यक है ? इस तथ्य को भलीभाँति जान लेता है । तथा वह यह भी जानता-मानता है कि जिस श्रु त के अभ्यास से आत-रौद्रध्यान दूर हो और धर्म-शुक्ल ध्यान में प्रवृत हुआ जा सके, वही श्रु त प्राथमिक भूमिका में आवश्यक है ।
आत्मतृप्त आत्मार्थी का व्यवहार जो आत्मार्थी आत्मतृप्त हो जाता है, उसके चित्त से स्वार्थवृत्ति हटती जाती है, मध्यस्थवृत्ति, परमतसहिष्णुता, स्व-मतपक्षाग्रहरहितता आर समता विकसित हो जाती है। और उसका निश्चयदृष्टि से आत्मज्ञान, आत्मश्रद्धान और आत्मभावरमण ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसके चित्त में आर्त-रौद्रध्यान को कारणभूत स्वार्थवत्ति एवं विषयपिपासा मन्द होती जाती है । स्वार्थवृति के स्थान में परार्थवृत्ति विकसित होती जाती है। आर्त्त-रौद्रध्यान के चंगुल से छूटते ही, उसके मन से ईर्ष्या, मात्सर्य, द्वष आदि को वृत्तियाँ विदा हो जाती हैं। तिरस्कार घृणा आदि का स्थान उदारता, सहानुभूति, परमतसहिष्णुता, वत्सलता आदि ले लेते हैं । चिन्ता, भय, उग आदि भो दूर हो जाते हैं। इस प्रकार वह समत्वाचरण से आत्मरामता का स्पर्श करके निश्चयरत्नत्रय का आस्वाद पा लेता है, जो उसे परमात्मतत्त्व के निकट ले जाता है।1
१ चेष्टापरस्य वृत्तान्ते मूकान्धबधिरोपमा । उत्साहः स्वगुणाभ्यासे, दुःस्थस्येव धनार्जने ॥
-अध्यात्मसार अधि. ६, श्लो. ४१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org