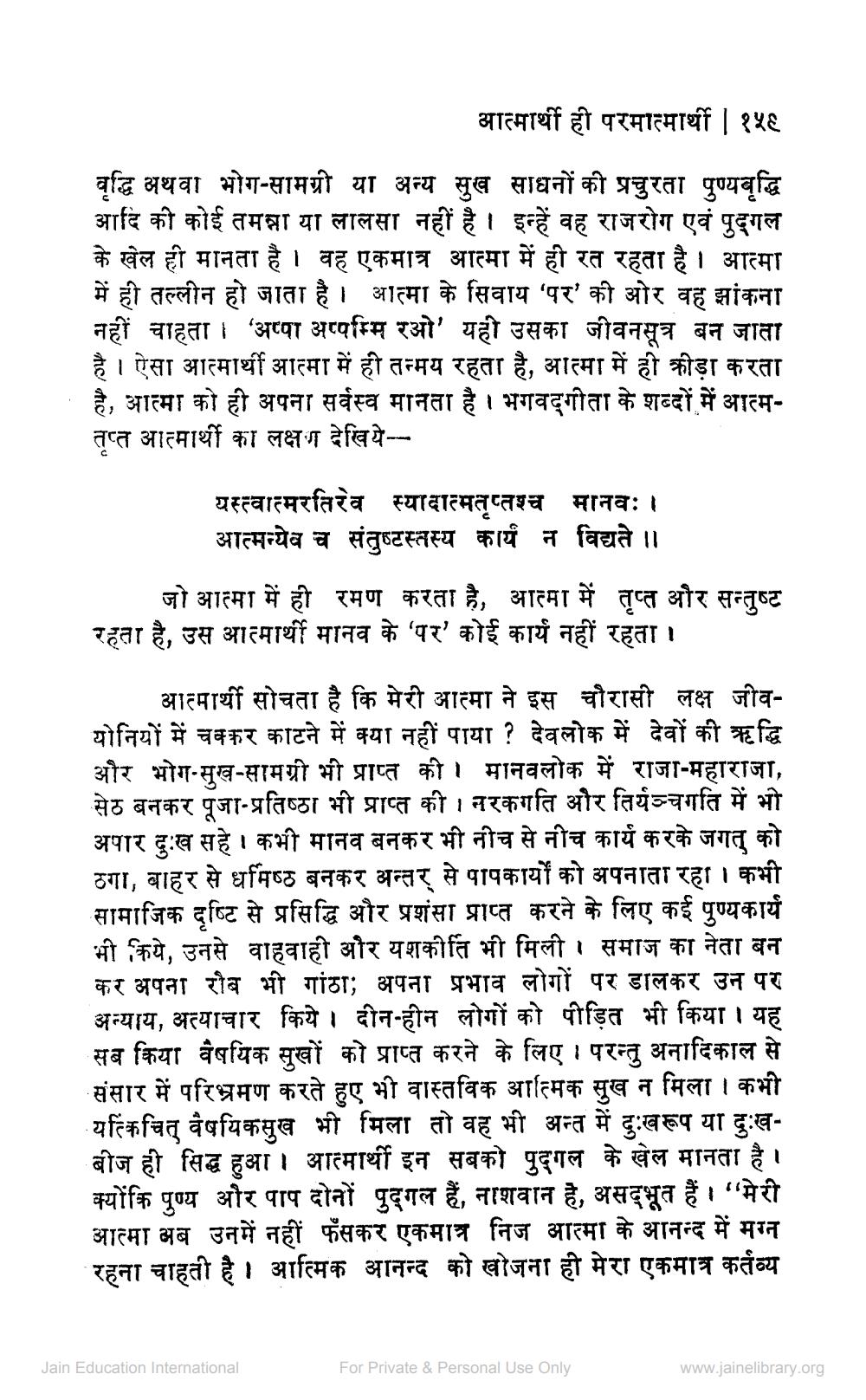________________
आत्मार्थी ही परमात्मार्थी | १५६
वृद्धि अथवा भोग-सामग्री या अन्य सुख साधनों की प्रचुरता पुण्यबृद्धि आदि की कोई तमन्ना या लालसा नहीं है। इन्हें वह राजरोग एवं पुद्गल के खेल ही मानता है । वह एकमात्र आत्मा में ही रत रहता है। आत्मा में ही तल्लीन हो जाता है। आत्मा के सिवाय 'पर' की ओर वह झांकना नहीं चाहता। 'अप्पा अप्पम्मि रओ' यही उसका जीवनसूत्र बन जाता है। ऐसा आत्मार्थी आत्मा में ही तन्मय रहता है, आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, आत्मा को ही अपना सर्वस्व मानता है। भगवद्गीता के शब्दों में आत्मतप्त आत्मार्थी का लक्षण देखिये--
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ।।
जो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में तृप्त और सन्तुष्ट रहता है, उस आत्मार्थी मानव के 'पर' कोई कार्य नहीं रहता।
आत्मार्थी सोचता है कि मेरी आत्मा ने इस चौरासी लक्ष जीवयोनियों में चक्कर काटने में क्या नहीं पाया ? देवलोक में देवों की ऋद्धि और भोग-सुख-सामग्री भी प्राप्त की। मानवलोक में राजा-महाराजा, सेठ बनकर पूजा-प्रतिष्ठा भी प्राप्त की। नरकगति और तिर्यञ्चगति में भी अपार दुःख सहे । कभी मानव बनकर भी नीच से नीच कार्य करके जगत् को ठगा, बाहर से मिष्ठ बनकर अन्तर् से पापकार्यों को अपनाता रहा । कभी सामाजिक दृष्टि से प्रसिद्धि और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कई पुण्यकार्य भी किये, उनसे वाहवाही और यशकीर्ति भी मिली। समाज का नेता बन कर अपना रोब भी गांठा; अपना प्रभाव लोगों पर डालकर उन पर अन्याय, अत्याचार किये। दीन-हीन लोगों को पीड़ित भी किया। यह सब किया वैषयिक सुखों को प्राप्त करने के लिए। परन्तु अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए भी वास्तविक आत्मिक सुख न मिला। कभी यत्किचित् वैषयिकसुख भी मिला तो वह भी अन्त में दुःखरूप या दुःखबीज ही सिद्ध हुआ। आत्मार्थी इन सबको पुद्गल के खेल मानता है। क्योंकि पुण्य और पाप दोनों पुद्गल हैं, नाशवान है, असद्भूत हैं। "मेरी आत्मा अब उनमें नहीं फँसकर एकमात्र निज आत्मा के आनन्द में मग्न रहना चाहती है। आत्मिक आनन्द को खोजना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org