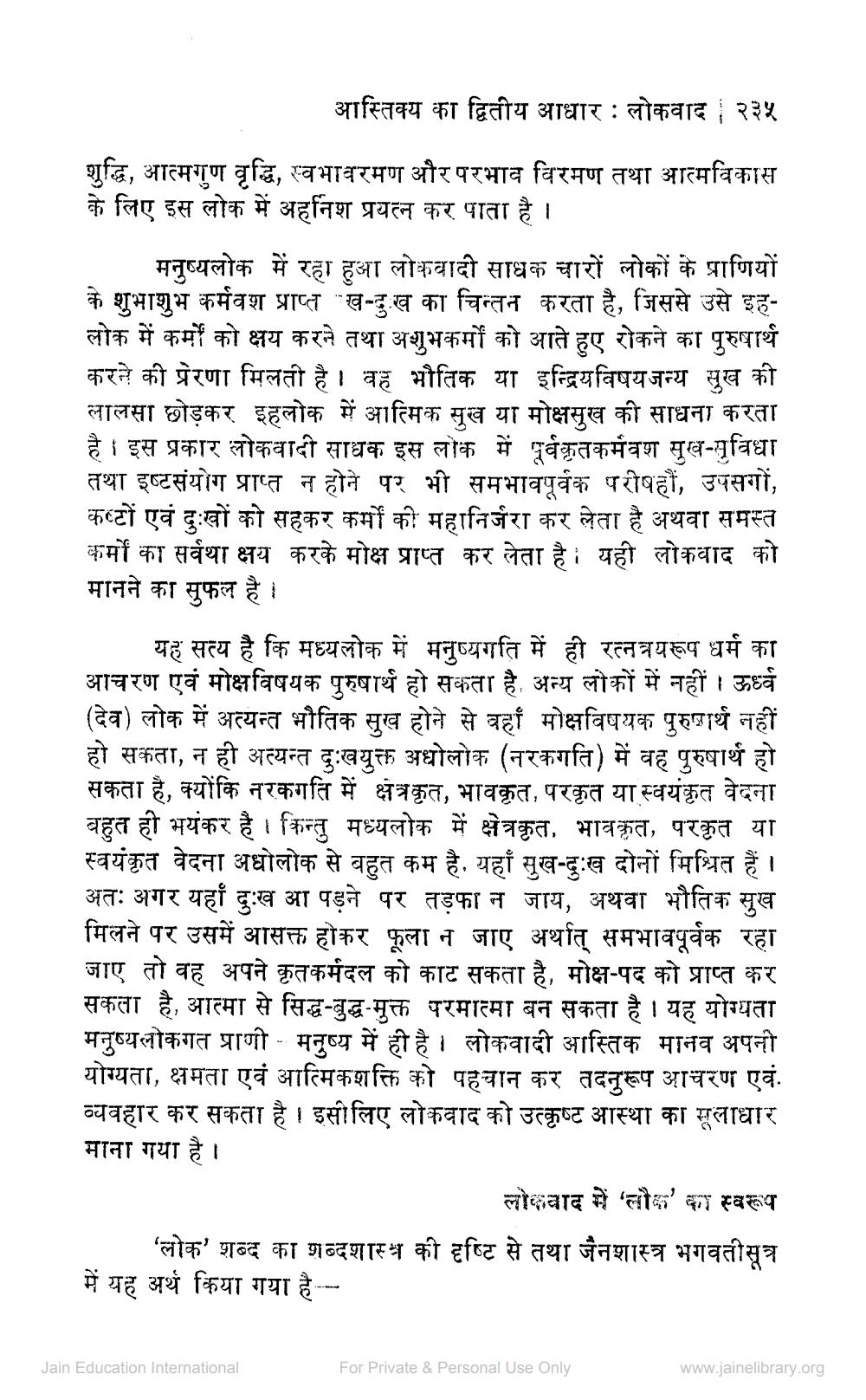________________
आस्तिक्य का द्वितीय आधार : लोकवाद २३५
शुद्धि, आत्मगण वृद्धि, स्वभावरमण और परभाव विरमण तथा आत्मविकास के लिए इस लोक में अहर्निश प्रयत्न कर पाता है ।
मनुष्यलोक में रहा हआ लोकवादी साधक चारों लोकों के प्राणियों के शुभाशुभ कर्मवश प्राप्त “ख-दुःख का चिन्तन करता है, जिससे उसे इहलोक में कर्मों को क्षय करने तथा अशुभकर्मों को आते हुए रोकने का पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती है। वह भौतिक या इन्द्रियविषयजन्य सुख की लालसा छोड़कर इहलोक में आत्मिक सुख या मोक्षसुख की साधना करता है। इस प्रकार लोकवादी साधक इस लोक में पूर्वकृतकर्मवश सुख-सुविधा तथा इष्टसंयोग प्राप्त न होने पर भी समभावपूर्वक परीषहौं, उपसगी, कष्टों एवं दुःखों को सहकर कर्मों की महानिर्जरा कर लेता है अथवा समस्त कर्मों का सर्वथा क्षय करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यही लोकवाद को मानने का सुफल है।
यह सत्य है कि मध्यलोक में मनुष्यगति में ही रत्नत्रयरूप धर्म का आचरण एवं मोक्षविषयक पुरुषार्थ हो सकता है, अन्य लोकों में नहीं । ऊर्ध्व (देव) लोक में अत्यन्त भौतिक सुख होने से वहाँ मोक्षविषयक पुरुषार्थ नहीं हो सकता, न ही अत्यन्त दुःखयुक्त अधोलोक (नरकगति) में वह पुरुषार्थ हो सकता है, क्योंकि नरकगति में क्षेत्रकृत, भावकृत, परकृत या स्वयंकृत वेदना बहत ही भयंकर है। किन्तु मध्यलोक में क्षेत्रकृत, भावकृत, परकृत या स्वयंकृत वेदना अधोलोक से बहुत कम है. यहाँ सुख-दुःख दोनों मिश्रित हैं। अतः अगर यहाँ दुःख आ पड़ने पर तड़फा न जाय, अथवा भौतिक सुख मिलने पर उसमें आसक्त होकर फूला न जाए अर्थात् समभावपूर्वक रहा जाए तो वह अपने कृतकर्मदल को काट सकता है, मोक्ष-पद को प्राप्त कर सकता है, आत्मा से सिद्ध-बुद्ध-मुक्त परमात्मा बन सकता है । यह योग्यता मनुष्यलोकगत प्राणी - मनुष्य में ही है। लोकवादी आस्तिक मानव अपनी योग्यता, क्षमता एवं आत्मिक शक्ति को पहचान कर तदनुरूप आचरण एवं. व्यवहार कर सकता है । इसी लिए लोकवाद को उत्कृष्ट आस्था का मूलाधार माना गया है।
लोकवाद में 'लोक' का स्वरूप 'लोक' शब्द का शब्दशास्त्र की दृष्टि से तथा जैनशास्त्र भगवतीसूत्र में यह अर्थ किया गया है.---.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org