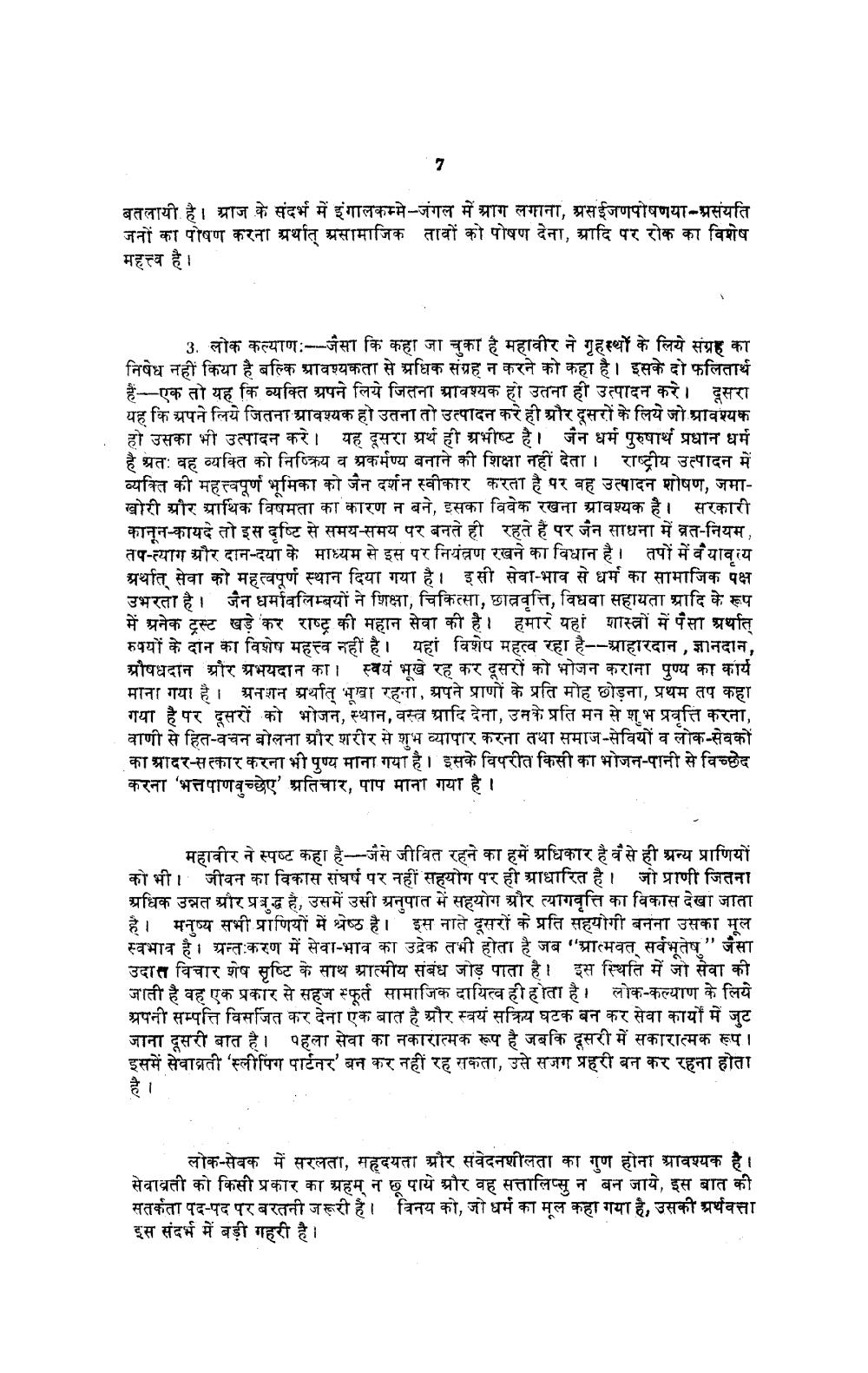________________
बतलायी है। आज के संदर्भ में इंगालकम्मे-जंगल में आग लगाना, असईजणपोषणया-प्रसंयति जनों का पोषण करना अर्थात् असामाजिक तावों को पोषण देना, आदि पर रोक का विशेष महत्त्व है।
3. लोक कल्याण:--जैसा कि कहा जा चुका है महावीर ने गृहस्थों के लिये संग्रह का निषेध नहीं किया है बल्कि आवश्यकता से अधिक संग्रह न करने को कहा है। इसके दो फलितार्थ हैं-एक तो यह कि व्यक्ति अपने लिये जितना आवश्यक हो उतना ही उत्पादन करे। दूसरा यह कि अपने लिये जितना आवश्यक हो उतना तो उत्पादन करे ही और दूसरों के लिये जो अावश्यक हो उसका भी उत्पादन करे। यह दूसरा अर्थ ही अभीष्ट है। जैन धर्म पुरुषार्थ प्रधान धर्म है अतः वह व्यक्ति को निष्क्रिय व अकर्मण्य बनाने की शिक्षा नहीं देता। राष्ट्रीय उत्पादन में व्यक्ति की महत्त्वपूर्ण भूमिका को जैन दर्शन स्वीकार करता है पर वह उत्पादन शोषण, जमाखोरी और आर्थिक विषमता का कारण न बने, इसका विवेक रखना आवश्यक है। सरकारी कानून-कायदे तो इस दृष्टि से समय-समय पर बनते ही रहते हैं पर जैन साधना में व्रत-नियम, तप-त्याग और दान-दया के माध्यम से इस पर नियंत्रण रखने का विधान है। तपों में वैयावृत्य अर्थात सेवा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी सेवा-भाव से धर्म का सामाजिक पक्ष उभरता है। जैन धर्मावलिम्बयों ने शिक्षा, चिकित्सा, छात्रवृत्ति, विधवा सहायता प्रादि के रूप में अनेक ट्रस्ट खड़े कर राष्ट्र की महान सेवा की है। हमारे यहां शास्त्रों में पैसा अर्थात् रुपयों के दान का विशेष महत्त्व नहीं है। यहां विशेष महत्व रहा है--आहारदान , ज्ञानदान, औषधदान और अभयदान का। स्वयं भूखे रह कर दूसरों को भोजन कराना पुण्य का कार्य माना गया है। अनशन अर्थात भूखा रहना, अपने प्राणों के प्रति मोह छोड़ना, प्रथम तप कहा गया है पर दूसरों को भोजन, स्थान, वस्त्र प्रादि देना, उनके प्रति मन से शभ प्रवत्ति करना, वाणी से हित-वचन बोलना और शरीर से शुभ व्यापार करना तथा समाज-सेवियों व लोक-सेवकों का आदर-सत्कार करना भी पुण्य माना गया है। इसके विपरीत किसी का भोजन-पानी से विच्छेद करना 'भत्तपाणवुच्छेए' अतिचार, पाप माना गया है।
महावीर ने स्पष्ट कहा है-जैसे जीवित रहने का हमें अधिकार है वैसे ही अन्य प्राणियों को भी। जीवन का विकास संघर्ष पर नहीं सहयोग पर ही आधारित है। जो प्राणी जितना अधिक उन्नत और प्रबुद्ध है, उसमें उसी अनुपात में सहयोग और त्यागवृत्ति का विकास देखा जाता है। मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। इस नाते दूसरों के प्रति सहयोगी बनना उसका मूल स्वभाव है। अन्तःकरण में सेवा-भाव का उद्रेक तभी होता है जब "प्रात्मवत सर्वभूतेष" जैसा उदात्त विचार शेष सृष्टि के साथ आत्मीय संबंध जोड़ पाता है। इस स्थिति में जो सेवा की जाती है वह एक प्रकार से सहज स्फूर्त सामाजिक दायित्व ही होता है। लोक-कल्याण के लिये अपनी सम्पत्ति विसजित कर देना एक बात है और स्वयं सक्रिय घटक बन कर सेवा कार्यों में जट जाना दूसरी बात है। पहला सेवा का नकारात्मक रूप है जबकि दूसरी में सकारात्मक रूप । इसमें सेवाव्रती 'स्लीपिंग पार्टनर' बन कर नहीं रह सकता, उसे सजग प्रहरी बन कर रहना होता
लोक-सेवक में सरलता, महृदयता और संवेदनशीलता का गुण होना आवश्यक है। सेवाव्रती को किसी प्रकार का अहम् न छ पाये और वह सत्तालिप्सु न बन जाये, इस बात की सतर्कता पद-पद पर बरतनी जरूरी है। विनय को, जो धर्म का मूल कहा गया है, उसकी अर्थवत्ता इस संदर्भ में बड़ी गहरी है।