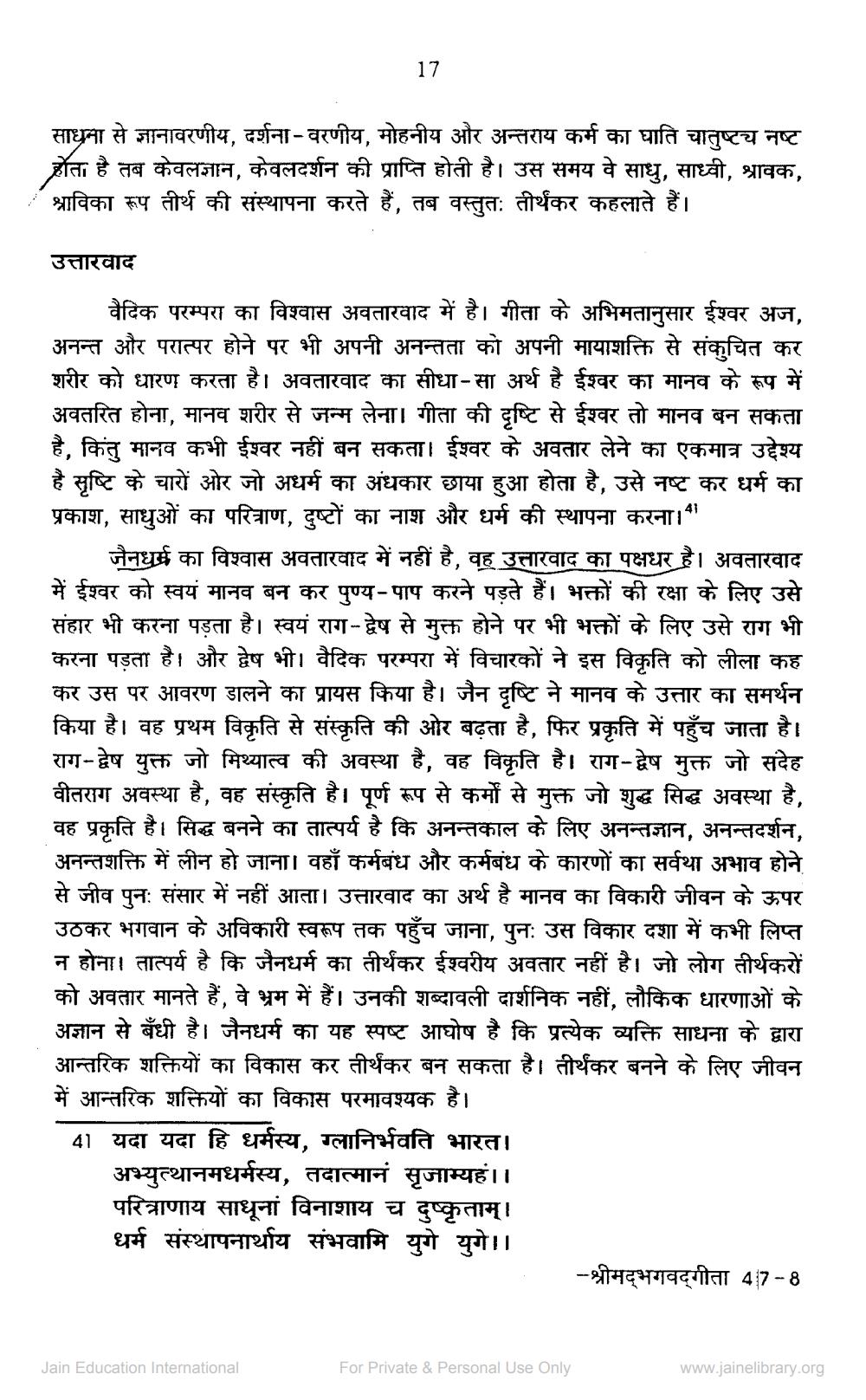________________
साधना से ज्ञानावरणीय, दर्शना - वरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्म का घाति चातुष्टय नष्ट होता है तब केवलज्ञान, केवलदर्शन की प्राप्ति होती है। उस समय वे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप तीर्थ की संस्थापना करते हैं, तब वस्तुतः तीर्थंकर कहलाते हैं।
उत्तारवाद
17
वैदिक परम्परा का विश्वास अवतारवाद में है। गीता के अभिमतानुसार ईश्वर अज, अनन्त और परात्पर होने पर भी अपनी अनन्तता को अपनी मायाशक्ति से संकुचित कर शरीर को धारण करता है। अवतारवाद का सीधा सा अर्थ है ईश्वर का मानव के रूप में अवतरित होना, मानव शरीर से जन्म लेना। गीता की दृष्टि से ईश्वर तो मानव बन सकता है, किंतु मानव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर के अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य है सृष्टि के चारों ओर जो अधर्म का अंधकार छाया हुआ होता है, उसे नष्ट कर धर्म का प्रकाश, साधुओं का परित्राण, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करना । '
41
जैनधर्म का विश्वास अवतारवाद में नहीं है, वह उत्तारवाद का पक्षधर है। अवतारवाद में ईश्वर को स्वयं मानव बन कर पुण्य पाप करने पड़ते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए उसे संहार भी करना पड़ता है। स्वयं राग- - द्वेष से मुक्त होने पर भी भक्तों के लिए उसे राग भी करना पड़ता है। और द्वेष भी । वैदिक परम्परा में विचारकों ने इस विकृति को लीला कह कर उस पर आवरण डालने का प्रायस किया है। जैन दृष्टि ने मानव के उत्तार का समर्थन किया है। वह प्रथम विकृति से संस्कृति की ओर बढ़ता है, फिर प्रकृति में पहुँच जाता है। राग-द्वेष युक्त जो मिथ्यात्व की अवस्था है, वह विकृति है। राग-द्वेष मुक्त जो संदेह वीतराग अवस्था है, वह संस्कृति है । पूर्ण रूप से कर्मों से मुक्त जो शुद्ध सिद्ध अवस्था है, वह प्रकृति है। सिद्ध बनने का तात्पर्य है कि अनन्तकाल के लिए अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति में लीन हो जाना। वहाँ कर्मबंध और कर्मबंध के कारणों का सर्वथा अभाव होने से जीव पुनः संसार में नहीं आता । उत्तारवाद का अर्थ है मानव का विकारी जीवन के ऊपर उठकर भगवान के अविकारी स्वरूप तक पहुँच जाना, पुनः उस विकार दशा में कभी लिप्त न होना । तात्पर्य है कि जैनधर्म का तीर्थंकर ईश्वरीय अवतार नहीं है। जो लोग तीर्थकरों को अवतार मानते हैं, वे भ्रम में हैं। उनकी शब्दावली दार्शनिक नहीं, लौकिक धारणाओं के अज्ञान से बँधी है। जैनधर्म का यह स्पष्ट आघोष है कि प्रत्येक व्यक्ति साधना के द्वारा आन्तरिक शक्तियों का विकास कर तीर्थंकर बन सकता है। तीर्थंकर बनने के लिए जीवन में आन्तरिक शक्तियों का विकास परमावश्यक है। 41 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं । । परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे । ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
- श्रीमद्भगवद्गीता 478
www.jainelibrary.org