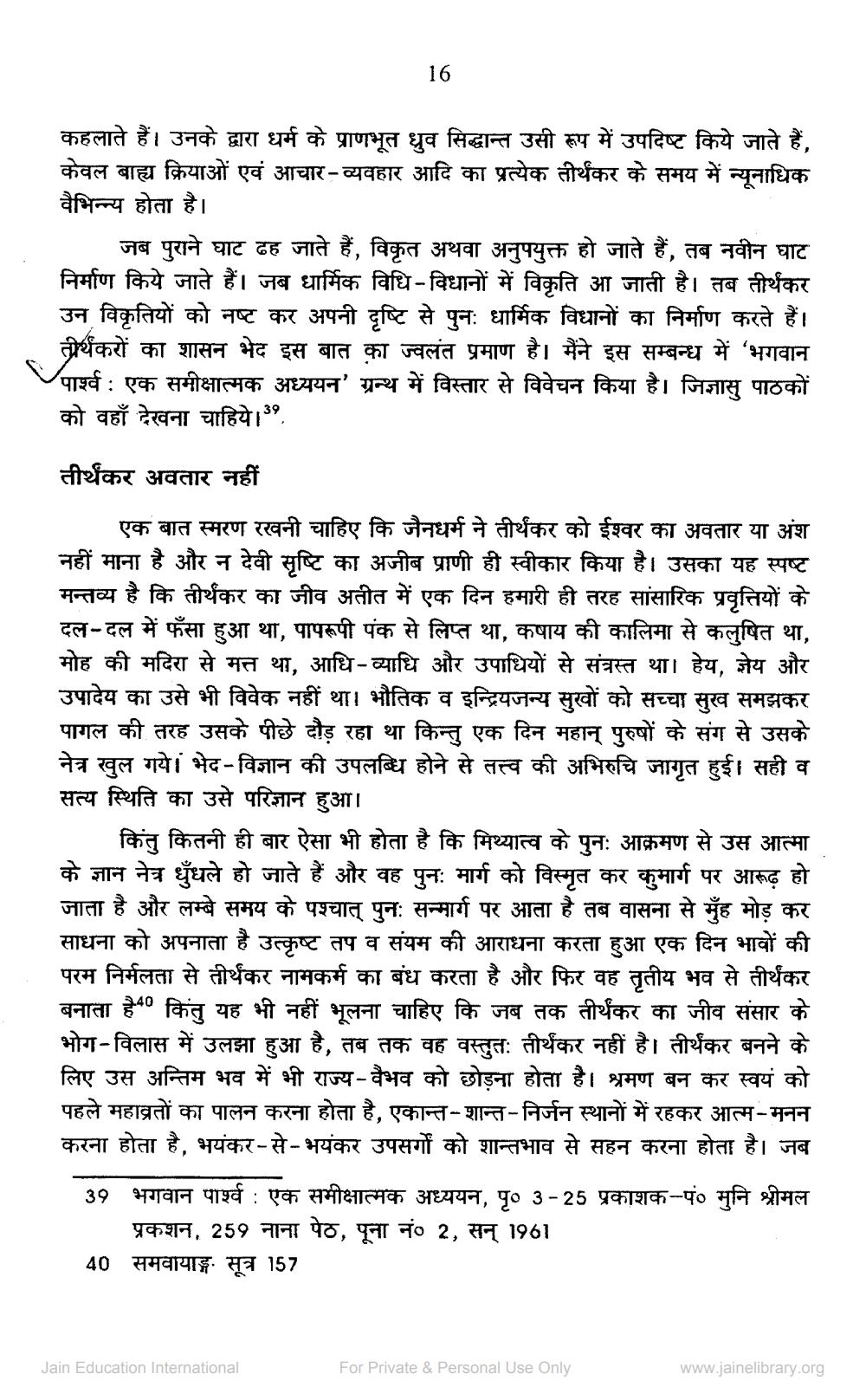________________
16
कहलाते हैं। उनके द्वारा धर्म के प्राणभूत धुव सिद्धान्त उसी रूप में उपदिष्ट किये जाते हैं, केवल बाह्य क्रियाओं एवं आचार-व्यवहार आदि का प्रत्येक तीर्थंकर के समय में न्यूनाधिक वैभिन्न्य होता है।
जब पुराने घाट ढह जाते हैं, विकृत अथवा अनुपयुक्त हो जाते हैं, तब नवीन घाट निर्माण किये जाते हैं। जब धार्मिक विधि-विधानों में विकृति आ जाती है। तब तीर्थंकर उन विकृतियों को नष्ट कर अपनी दृष्टि से पुन: धार्मिक विधानों का निर्माण करते हैं। तीर्थंकरों का शासन भेद इस बात का ज्वलंत प्रमाण है। मैंने इस सम्बन्ध में 'भगवान पार्श्व : एक समीक्षात्मक अध्ययन' ग्रन्थ में विस्तार से विवेचन किया है। जिज्ञासु पाठकों को वहाँ देखना चाहिये।".
तीर्थंकर अवतार नहीं
एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि जैनधर्म ने तीर्थंकर को ईश्वर का अवतार या अंश नहीं माना है और न देवी सृष्टि का अजीब प्राणी ही स्वीकार किया है। उसका यह स्पष्ट मन्तव्य है कि तीर्थंकर का जीव अतीत में एक दिन हमारी ही तरह सांसारिक प्रवृत्तियों के दल-दल में फंसा हुआ था, पापरूपी पंक से लिप्त था, कषाय की कालिमा से कलुषित था, मोह की मदिरा से मत्त था, आधि-व्याधि और उपाधियों से संत्रस्त था। हेय, ज्ञेय और उपादेय का उसे भी विवेक नहीं था। भौतिक व इन्द्रियजन्य सुखों को सच्चा सुख समझकर पागल की तरह उसके पीछे दौड़ रहा था किन्तु एक दिन महान् पुरुषों के संग से उसके नेत्र खुल गये। भेद - विज्ञान की उपलब्धि होने से तत्त्व की अभिरुचि जागृत हुई। सही व सत्य स्थिति का उसे परिज्ञान हुआ।
किंतु कितनी ही बार ऐसा भी होता है कि मिथ्यात्व के पुन: आक्रमण से उस आत्मा के ज्ञान नेत्र धुंधले हो जाते हैं और वह पुन: मार्ग को विस्मृत कर कुमार्ग पर आरूढ़ हो जाता है और लम्बे समय के पश्चात् पुन: सन्मार्ग पर आता है तब वासना से मुँह मोड़ कर साधना को अपनाता है उत्कृष्ट तप व संयम की आराधना करता हुआ एक दिन भावों की परम निर्मलता से तीर्थंकर नामकर्म का बंध करता है और फिर वह तृतीय भव से तीर्थंकर बनाता है। किंतु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब तक तीर्थंकर का जीव संसार के भोग-विलास में उलझा हुआ है, तब तक वह वस्तुत: तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर बनने के लिए उस अन्तिम भव में भी राज्य-वैभव को छोड़ना होता है। श्रमण बन कर स्वयं को पहले महाव्रतों का पालन करना होता है, एकान्त-शान्त-निर्जन स्थानों में रहकर आत्म-मनन करना होता है, भयंकर-से- भयंकर उपसर्गों को शान्तभाव से सहन करना होता है। जब 39 भगवान पार्श्व : एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृ० 3 - 25 प्रकाशक-पं० मुनि श्रीमल
प्रकशन, 259 नाना पेठ, पूना नं० 2, सन् 1961 40 समवायाङ्ग. सूत्र 157
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org