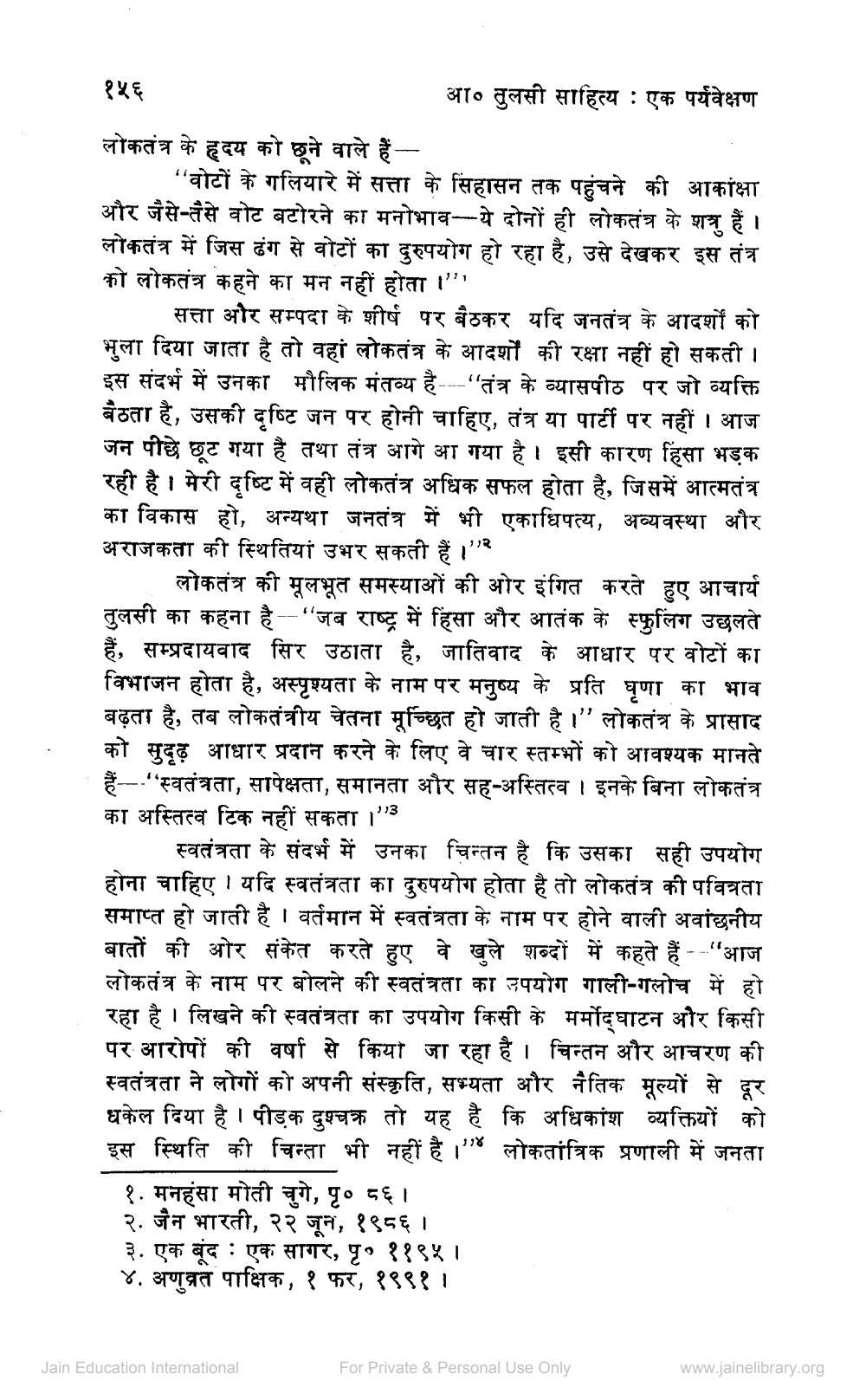________________
१५६
आ० तुलसी साहित्य : एक पर्यवेक्षण लोकतंत्र के हृदय को छूने वाले हैं
"वोटों के गलियारे में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की आकांक्षा और जैसे-तैसे वोट बटोरने का मनोभाव-ये दोनों ही लोकतंत्र के शत्रु हैं । लोकतंत्र में जिस ढंग से वोटों का दुरुपयोग हो रहा है, उसे देखकर इस तंत्र को लोकतंत्र कहने का मन नहीं होता ।''
सत्ता और सम्पदा के शीर्ष पर बैठकर यदि जनतंत्र के आदर्शों को भुला दिया जाता है तो वहां लोकतंत्र के आदर्शों की रक्षा नहीं हो सकती। इस संदर्भ में उनका मौलिक मंतव्य है--- "तंत्र के व्यासपीठ पर जो व्यक्ति बैठता है, उसकी दृष्टि जन पर होनी चाहिए, तंत्र या पार्टी पर नहीं । आज जन पीछे छूट गया है तथा तंत्र आगे आ गया है। इसी कारण हिंसा भड़क रही है। मेरी दृष्टि में वही लोकतंत्र अधिक सफल होता है, जिसमें आत्मतंत्र का विकास हो, अन्यथा जनतंत्र में भी एकाधिपत्य, अव्यवस्था और अराजकता की स्थितियां उभर सकती हैं।।
लोकतंत्र की मूलभूत समस्याओं की ओर इंगित करते हुए आचार्य तुलसी का कहना है -- "जब राष्ट्र में हिंसा और आतंक के स्फुलिंग उछलते हैं, सम्प्रदायवाद सिर उठाता है, जातिवाद के आधार पर वोटों का विभाजन होता है, अस्पृश्यता के नाम पर मनुष्य के प्रति घृणा का भाव बढ़ता है, तब लोकतंत्रीय चेतना मूच्छित हो जाती है।" लोकतंत्र के प्रासाद को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए वे चार स्तम्भों को आवश्यक मानते हैं.-."स्वतंत्रता, सापेक्षता, समानता और सह-अस्तित्व । इनके बिना लोकतंत्र का अस्तित्व टिक नहीं सकता।"3
स्वतंत्रता के संदर्भ में उनका चिन्तन है कि उसका सही उपयोग होना चाहिए। यदि स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है तो लोकतंत्र की पवित्रता समाप्त हो जाती है । वर्तमान में स्वतंत्रता के नाम पर होने वाली अवांछनीय बातों की ओर संकेत करते हुए वे खुले शब्दों में कहते हैं ..."आज लोकतंत्र के नाम पर बोलने की स्वतंत्रता का उपयोग गाली-गलोच में हो रहा है । लिखने की स्वतंत्रता का उपयोग किसी के मर्मोद्घाटन और किसी पर आरोपों की वर्षा से किया जा रहा है। चिन्तन और आचरण की स्वतंत्रता ने लोगों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और नैतिक मूल्यों से दूर धकेल दिया है । पीड़क दुश्चक्र तो यह है कि अधिकांश व्यक्तियों को इस स्थिति की चिन्ता भी नहीं है ।४ लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता १. मनहंसा मोती चुगे, पृ० ८६ । २. जैन भारती, २२ जून, १९८६ । ३. एक बूंद : एक सागर, पृ० ११९५ । ४. अणुव्रत पाक्षिक, १ फर, १९९१ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org