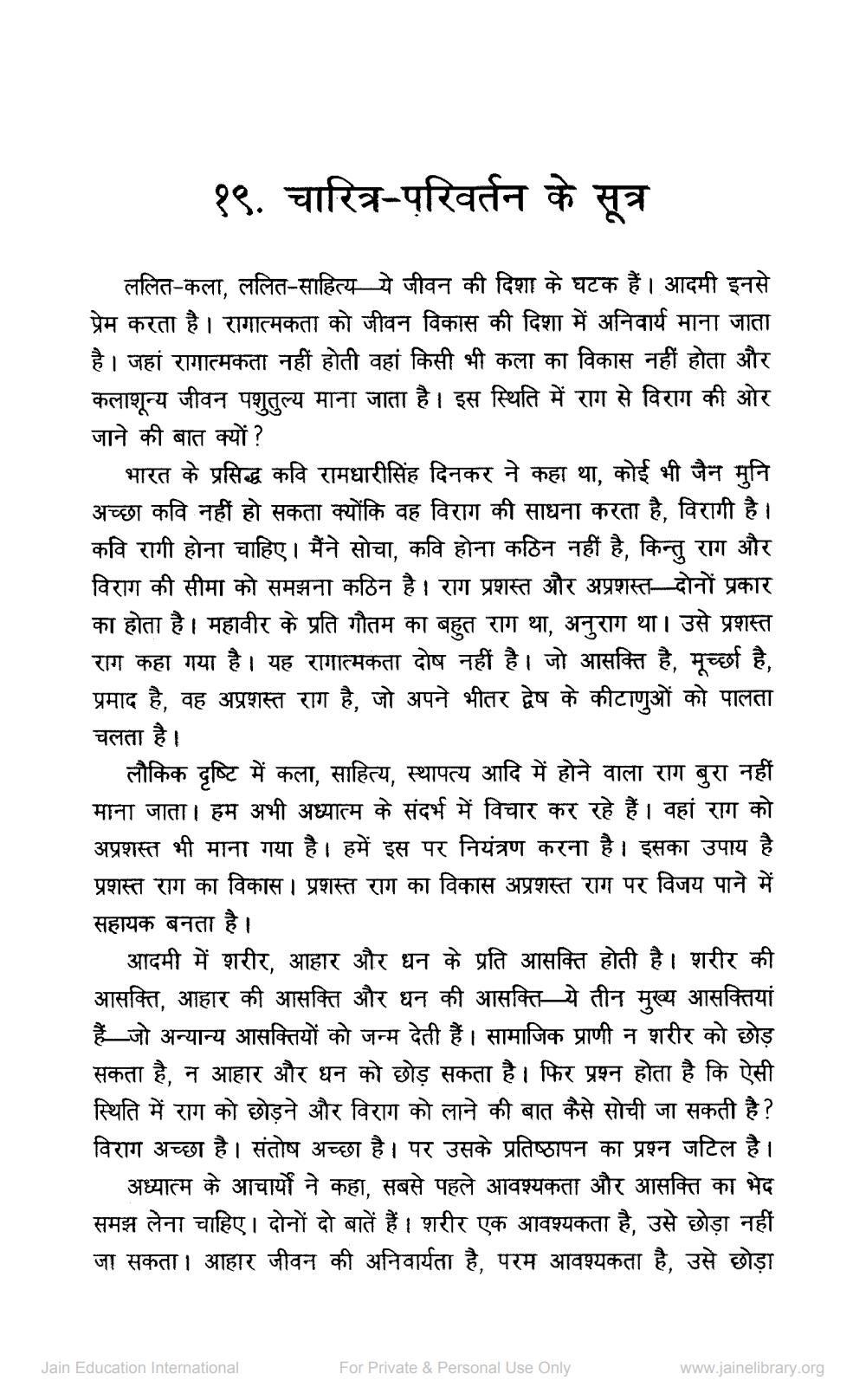________________
१९. चारित्र-परिवर्तन के सूत्र
ललित-कला, ललित-साहित्य ये जीवन की दिशा के घटक हैं। आदमी इनसे प्रेम करता है। रागात्मकता को जीवन विकास की दिशा में अनिवार्य माना जाता है। जहां रागात्मकता नहीं होती वहां किसी भी कला का विकास नहीं होता और कलाशून्य जीवन पशुतुल्य माना जाता है। इस स्थिति में राग से विराग की ओर जाने की बात क्यों? __ भारत के प्रसिद्ध कवि रामधारीसिंह दिनकर ने कहा था, कोई भी जैन मुनि अच्छा कवि नहीं हो सकता क्योंकि वह विराग की साधना करता है, विरागी है। कवि रागी होना चाहिए। मैंने सोचा, कवि होना कठिन नहीं है, किन्तु राग और विराग की सीमा को समझना कठिन है। राग प्रशस्त और अप्रशस्त—दोनों प्रकार का होता है। महावीर के प्रति गौतम का बहुत राग था, अनुराग था। उसे प्रशस्त राग कहा गया है। यह रागात्मकता दोष नहीं है। जो आसक्ति है, मूर्छा है, प्रमाद है, वह अप्रशस्त राग है, जो अपने भीतर द्वेष के कीटाणुओं को पालता चलता है।
लौकिक दृष्टि में कला, साहित्य, स्थापत्य आदि में होने वाला राग बुरा नहीं माना जाता। हम अभी अध्यात्म के संदर्भ में विचार कर रहे हैं। वहां राग को अप्रशस्त भी माना गया है। हमें इस पर नियंत्रण करना है। इसका उपाय है प्रशस्त राग का विकास। प्रशस्त राग का विकास अप्रशस्त राग पर विजय पाने में सहायक बनता है।
आदमी में शरीर, आहार और धन के प्रति आसक्ति होती है। शरीर की आसक्ति, आहार की आसक्ति और धन की आसक्ति ये तीन मुख्य आसक्तियां हैं जो अन्यान्य आसक्तियों को जन्म देती हैं। सामाजिक प्राणी न शरीर को छोड़ सकता है, न आहार और धन को छोड़ सकता है। फिर प्रश्न होता है कि ऐसी स्थिति में राग को छोड़ने और विराग को लाने की बात कैसे सोची जा सकती है? विराग अच्छा है। संतोष अच्छा है। पर उसके प्रतिष्ठापन का प्रश्न जटिल है।
अध्यात्म के आचार्यों ने कहा, सबसे पहले आवश्यकता और आसक्ति का भेद समझ लेना चाहिए। दोनों दो बातें हैं। शरीर एक आवश्यकता है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। आहार जीवन की अनिवार्यता है, परम आवश्यकता है, उसे छोड़ा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org