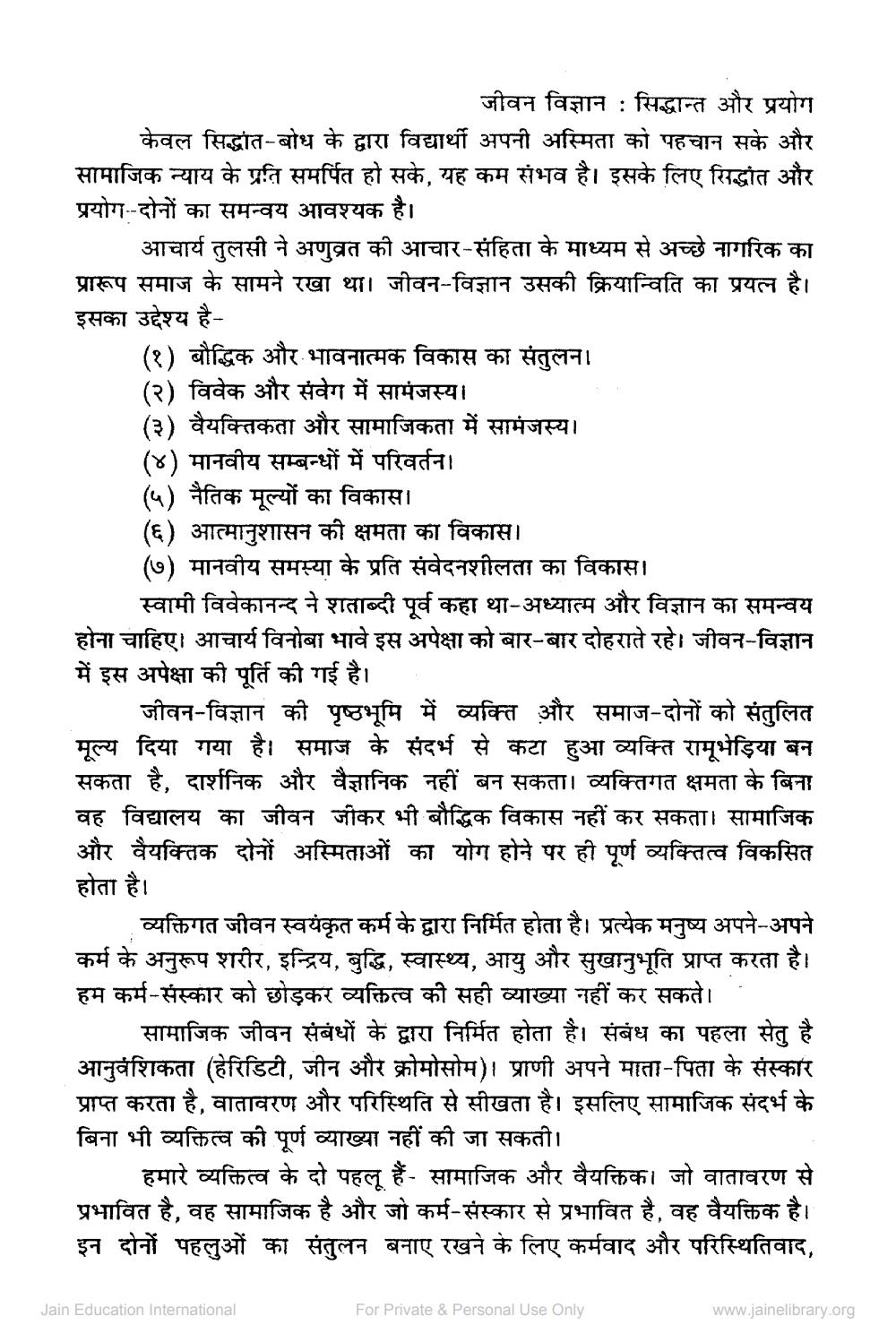________________
जीवन विज्ञान : सिद्धान्त और प्रयोग केवल सिद्धात-बोध के द्वारा विद्यार्थी अपनी अस्मिता को पहचान सके और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित हो सके, यह कम संभव है। इसके लिए सिद्धांत और प्रयोग-दोनों का समन्वय आवश्यक है।
आचार्य तुलसी ने अणुव्रत की आचार-संहिता के माध्यम से अच्छे नागरिक का प्रारूप समाज के सामने रखा था। जीवन-विज्ञान उसकी क्रियान्विति का प्रयत्न है। इसका उद्देश्य है
(१) बौद्धिक और भावनात्मक विकास का संतुलन। (२) विवेक और संवेग में सामंजस्य। (३) वैयक्तिकता और सामाजिकता में सामंजस्य। (४) मानवीय सम्बन्धों में परिवर्तन। (५) नैतिक मूल्यों का विकास। (६) आत्मानुशासन की क्षमता का विकास। (७) मानवीय समस्या के प्रति संवेदनशीलता का विकास।
स्वामी विवेकानन्द ने शताब्दी पूर्व कहा था-अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय होना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे इस अपेक्षा को बार-बार दोहराते रहे। जीवन-विज्ञान में इस अपेक्षा की पूर्ति की गई है।
जीवन-विज्ञान की पृष्ठभूमि में व्यक्ति और समाज-दोनों को संतुलित मूल्य दिया गया है। समाज के संदर्भ से कटा हुआ व्यक्ति रामूभेड़िया बन सकता है, दार्शनिक और वैज्ञानिक नहीं बन सकता। व्यक्तिगत क्षमता के बिना वह विद्यालय का जीवन जीकर भी बौद्धिक विकास नहीं कर सकता। सामाजिक
और वैयक्तिक दोनों अस्मिताओं का योग होने पर ही पूर्ण व्यक्तित्व विकसित होता है।
व्यक्तिगत जीवन स्वयंकृत कर्म के द्वारा निर्मित होता है। प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने कर्म के अनुरूप शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु और सुखानुभूति प्राप्त करता है। हम कर्म-संस्कार को छोड़कर व्यक्तित्व की सही व्याख्या नहीं कर सकते।
सामाजिक जीवन संबंधों के द्वारा निर्मित होता है। संबंध का पहला सेतु है आनुवंशिकता (हेरिडिटी, जीन और क्रोमोसोम)। प्राणी अपने माता-पिता के संस्कार प्राप्त करता है, वातावरण और परिस्थिति से सीखता है। इसलिए सामाजिक संदर्भ के बिना भी व्यक्तित्व की पूर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती।
हमारे व्यक्तित्व के दो पहलू हैं- सामाजिक और वैयक्तिक। जो वातावरण से प्रभावित है, वह सामाजिक है और जो कर्म-संस्कार से प्रभावित है, वह वैयक्तिक है। इन दोनों पहलुओं का संतुलन बनाए रखने के लिए कर्मवाद और परिस्थितिवाद,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org