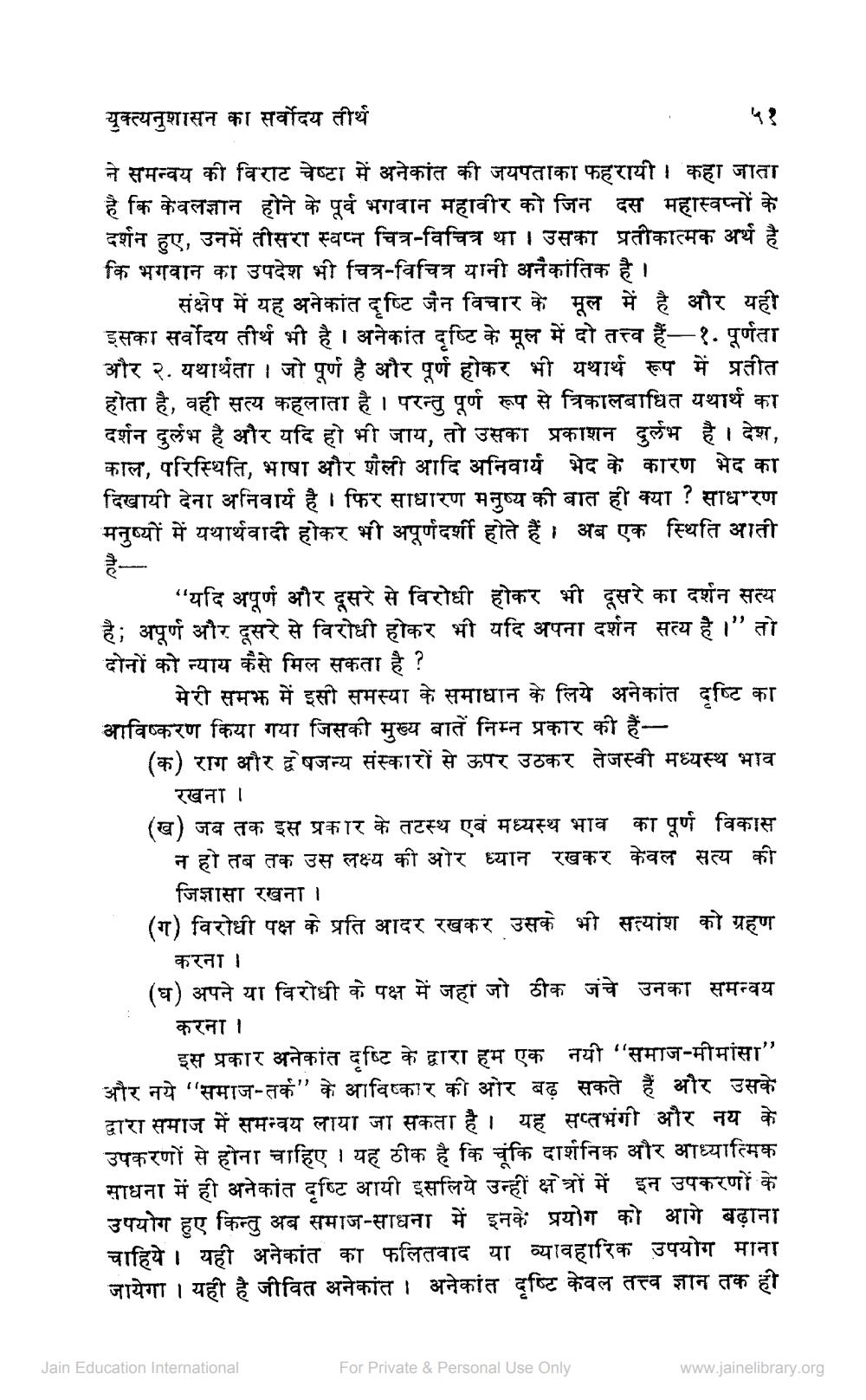________________
युक्त्यनुशासन का सर्वोदय तीर्थ
ने समन्वय की विराट चेष्टा में अनेकांत की जयपताका फहरायी। कहा जाता है कि केवलज्ञान होने के पूर्व भगवान महावीर को जिन दस महास्वप्नों के दर्शन हुए, उनमें तीसरा स्वप्न चित्र-विचित्र था । उसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि भगवान का उपदेश भी चित्र-विचित्र यानी अनैकांतिक है।
संक्षेप में यह अनेकांत दृष्टि जैन विचार के मूल में है और यही इसका सर्वोदय तीर्थ भी है । अनेकांत दृष्टि के मूल में दो तत्त्व हैं- १. पूर्णता
और २. यथार्थता । जो पूर्ण है और पूर्ण होकर भी यथार्थ रूप में प्रतीत होता है, वही सत्य कहलाता है । परन्तु पूर्ण रूप से त्रिकालबाधित यथार्थ का दर्शन दुर्लभ है और यदि हो भी जाय, तो उसका प्रकाशन दुर्लभ है। देश, काल, परिस्थिति, भाषा और शैली आदि अनिवार्य भेद के कारण भेद का दिखायी देना अनिवार्य है । फिर साधारण मनुष्य की बात ही क्या ? साधारण मनुष्यों में यथार्थवादी होकर भी अपूर्णदर्शी होते हैं। अब एक स्थिति आती
"यदि अपूर्ण और दूसरे से विरोधी होकर भी दूसरे का दर्शन सत्य है; अपूर्ण और दूसरे से विरोधी होकर भी यदि अपना दर्शन सत्य है।" तो दोनों को न्याय कैसे मिल सकता है ?
मेरी समझ में इसी समस्या के समाधान के लिये अनेकांत दृष्टि का आविष्करण किया गया जिसकी मुख्य बातें निम्न प्रकार की हैं(क) राग और द्वषजन्य संस्कारों से ऊपर उठकर तेजस्वी मध्यस्थ भाव
रखना। (ख) जब तक इस प्रकार के तटस्थ एवं मध्यस्थ भाव का पूर्ण विकास
न हो तब तक उस लक्ष्य की ओर ध्यान रखकर केवल सत्य की
जिज्ञासा रखना। (ग) विरोधी पक्ष के प्रति आदर रखकर उसके भी सत्यांश को ग्रहण
करना। (घ) अपने या विरोधी के पक्ष में जहां जो ठीक जंचे उनका समन्वय करना।
इस प्रकार अनेकांत दृष्टि के द्वारा हम एक नयी "समाज-मीमांसा" और नये "समाज-तर्क' के आविष्कार की ओर बढ़ सकते हैं और उसके द्वारा समाज में समन्वय लाया जा सकता है। यह सप्तभंगी और नय के उपकरणों से होना चाहिए । यह ठीक है कि चूंकि दार्शनिक और आध्यात्मिक साधना में ही अनेकांत दृष्टि आयी इसलिये उन्हीं क्षेत्रों में इन उपकरणों के उपयोग हुए किन्तु अब समाज-साधना में इनके प्रयोग को आगे बढ़ाना चाहिये। यही अनेकांत का फलितवाद या व्यावहारिक उपयोग माना जायेगा । यही है जीवित अनेकांत । अनेकांत दृष्टि केवल तत्त्व ज्ञान तक ही
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org