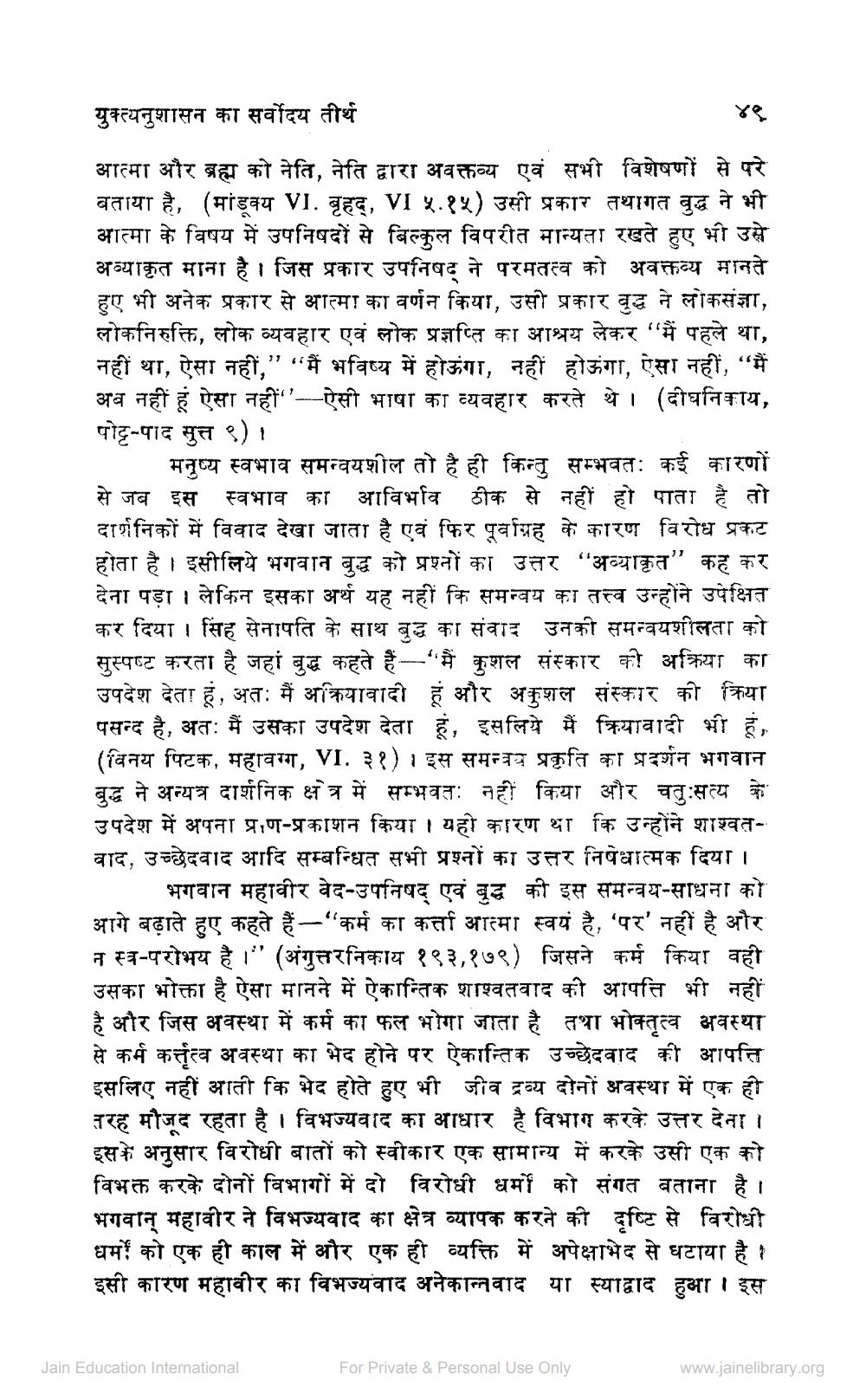________________
युक्त्यनुशासन का सर्वोदय तीर्थ
४९
आत्मा और ब्रह्म को नेति, नेति द्वारा अवक्तव्य एवं सभी विशेषणों से परे बताया है, (मांडूक्य VI. बृहद्, VI ५.१५) उसी प्रकार तथागत बुद्ध ने भी आत्मा के विषय में उपनिषदों से बिल्कुल विपरीत मान्यता रखते हुए भी उसे अव्याकृत माना है। जिस प्रकार उपनिषद ने परमतत्व को अवक्तव्य मानते हुए भी अनेक प्रकार से आत्मा का वर्णन किया, उसी प्रकार बुद्ध ने लोकसंज्ञा, लोकनिरुक्ति, लोक व्यवहार एवं लोक प्रज्ञप्ति का आश्रय लेकर "मैं पहले था, नहीं था, ऐसा नहीं," "मैं भविष्य में होऊंगा, नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं, “मैं अब नहीं हूं ऐसा नहीं''-ऐसी भाषा का व्यवहार करते थे। (दीघनिकाय, पोट्ट-पाद सुत्त ९)।
मनुष्य स्वभाव समन्वयशील तो है ही किन्तु सम्भवतः कई कारणों से जब इस स्वभाव का आविर्भाव ठीक से नहीं हो पाता है तो दार्शनिकों में विवाद देखा जाता है एवं फिर पूर्वाग्रह के कारण विरोध प्रकट होता है। इसीलिये भगवान बुद्ध को प्रश्नों का उत्तर "अव्याकृत" कह कर देना पड़ा । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि समन्वय का तत्त्व उन्होंने उपेक्षित कर दिया। सिंह सेनापति के साथ बुद्ध का संवाद उनकी समन्वयशीलता को सुस्पष्ट करता है जहां बुद्ध कहते हैं- "मैं कुशल संस्कार को अक्रिया का उपदेश देता हूं, अत: मैं अक्रियावादी हूं और अकुशल संस्कार की क्रिया पसन्द है, अतः मैं उसका उपदेश देता हूं, इसलिये मैं क्रियावादी भी हूं, (विनय पिटक, महावग्ग, VI. ३१) । इस समन्वय प्रकृति का प्रदर्शन भगवान बुद्ध ने अन्यत्र दार्शनिक क्षेत्र में सम्भवतः नहीं किया और चतुःसत्य के उपदेश में अपना प्राण-प्रकाशन किया। यही कारण था कि उन्होंने शाश्वतवाद, उच्छेदवाद आदि सम्बन्धित सभी प्रश्नों का उत्तर निषेधात्मक दिया ।
भगवान महावीर वेद-उपनिषद् एवं बुद्ध की इस समन्वय-साधना को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं-"कर्म का कर्ता आत्मा स्वयं है, 'पर' नहीं है और न स्व-परोभय है।" (अंगुत्तरनिकाय १९३,१७९) जिसने कर्म किया वही उसका भोक्ता है ऐसा मानने में ऐकान्तिक शाश्वतवाद की आपत्ति भी नहीं है और जिस अवस्था में कर्म का फल भोगा जाता है तथा भोक्तृत्व अवस्था से कर्म कर्तृत्व अवस्था का भेद होने पर ऐकान्तिक उच्छेदवाद की आपत्ति इसलिए नहीं आती कि भेद होते हुए भी जीव द्रव्य दोनों अवस्था में एक ही तरह मौजूद रहता है । विभज्यवाद का आधार है विभाग करके उत्तर देना। इसके अनुसार विरोधी बातों को स्वीकार एक सामान्य में करके उसी एक को विभक्त करके दोनों विभागों में दो विरोधी धर्मों को संगत बताना है। भगवान् महावीर ने विभज्यवाद का क्षेत्र व्यापक करने की दृष्टि से विरोधी धर्मों को एक ही काल में और एक ही व्यक्ति में अपेक्षाभेद से घटाया है। इसी कारण महावीर का विभज्यवाद अनेकान्तवाद या स्याद्वाद हुआ। इस
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org