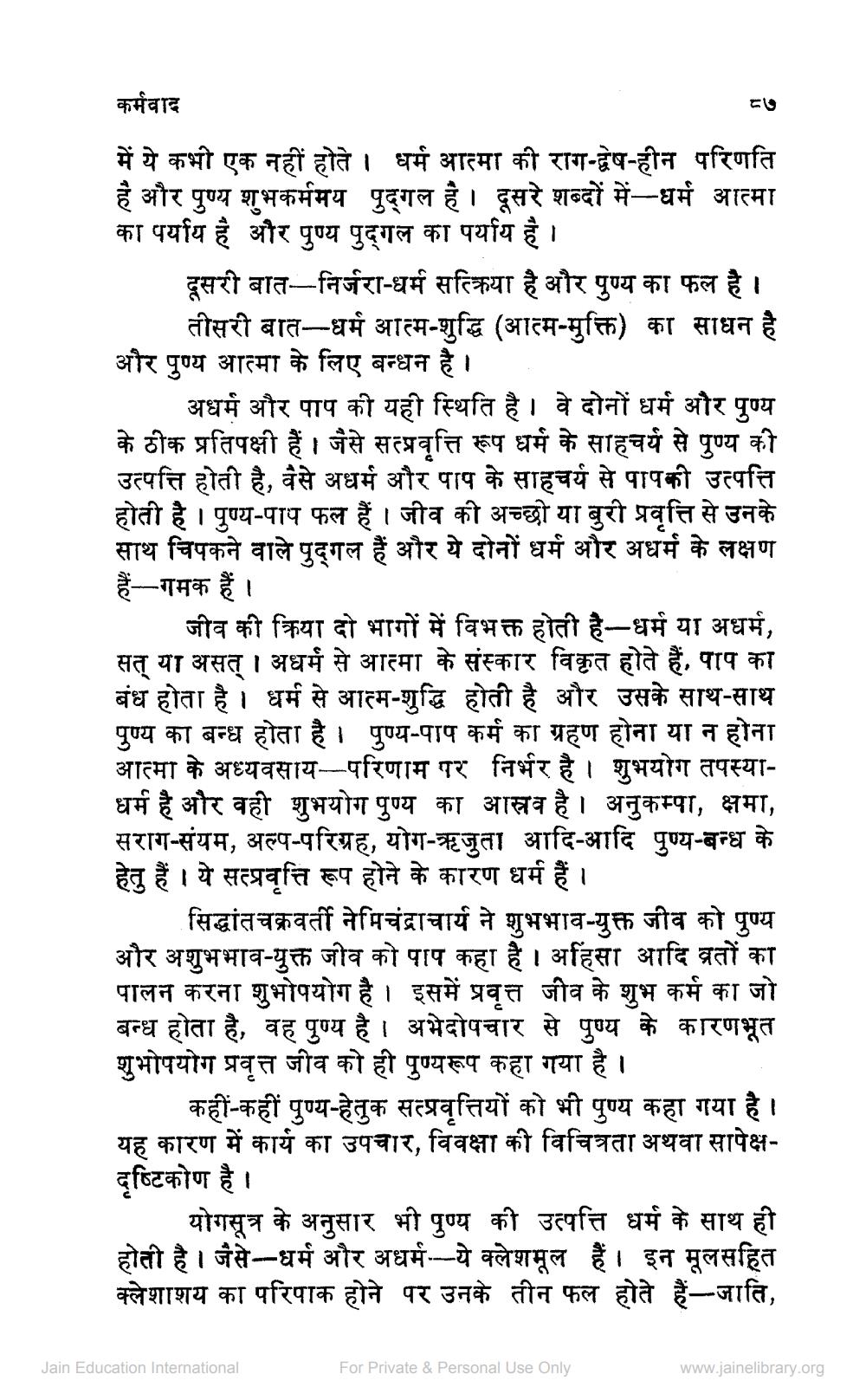________________
कर्मवाद
८७
में ये कभी एक नहीं होते। धर्म आत्मा की राग-द्वेष-हीन परिणति है और पुण्य शुभकर्ममय पुद्गल है। दूसरे शब्दों में-धर्म आत्मा का पर्याय है और पुण्य पुद्गल का पर्याय है।
दूसरी बात-निर्जरा-धर्म सक्रिया है और पुण्य का फल है।
तीसरी बात-धर्म आत्म-शुद्धि (आत्म-मुक्ति) का साधन है और पुण्य आत्मा के लिए बन्धन है।
अधर्म और पाप की यही स्थिति है। वे दोनों धर्म और पुण्य के ठीक प्रतिपक्षी हैं । जैसे सत्प्रवृत्ति रूप धर्म के साहचर्य से पुण्य की उत्पत्ति होती है, वैसे अधर्म और पाप के साहचर्य से पापकी उत्पत्ति होती है । पुण्य-पाप फल हैं । जीव की अच्छी या बुरी प्रवृत्ति से उनके साथ चिपकने वाले पुद्गल हैं और ये दोनों धर्म और अधर्म के लक्षण हैं—गमक हैं।
जीव की क्रिया दो भागों में विभक्त होती है-धर्म या अधर्म, सत् या असत् । अधर्म से आत्मा के संस्कार विकृत होते हैं, पाप का बंध होता है। धर्म से आत्म-शुद्धि होती है और उसके साथ-साथ पुण्य का बन्ध होता है। पुण्य-पाप कर्म का ग्रहण होना या न होना आत्मा के अध्यवसाय-परिणाम पर निर्भर है। शुभयोग तपस्याधर्म है और वही शुभयोग पुण्य का आस्रव है। अनुकम्पा, क्षमा, सराग-संयम, अल्प-परिग्रह, योग-ऋजुता आदि-आदि पुण्य-बन्ध के हेतु हैं । ये सत्प्रवृत्ति रूप होने के कारण धर्म हैं।
सिद्धांतचक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य ने शुभभाव-युक्त जीव को पुण्य और अशुभभाव-युक्त जीव को पाप कहा है। अहिंसा आदि व्रतों का पालन करना शुभोपयोग है। इसमें प्रवृत्त जीव के शुभ कर्म का जो बन्ध होता है, वह पुण्य है। अभेदोपचार से पुण्य के कारणभूत शुभोपयोग प्रवृत्त जीव को ही पुण्यरूप कहा गया है।
कहीं-कहीं पुण्य-हेतुक सत्प्रवृत्तियों को भी पुण्य कहा गया है। यह कारण में कार्य का उपचार, विवक्षा की विचित्रता अथवा सापेक्षदृष्टिकोण है।
योगसूत्र के अनुसार भी पुण्य की उत्पत्ति धर्म के साथ ही होती है। जैसे-धर्म और अधर्म-ये क्लेशमूल हैं। इन मूलसहित क्लेशाशय का परिपाक होने पर उनके तीन फल होते हैं-जाति,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org