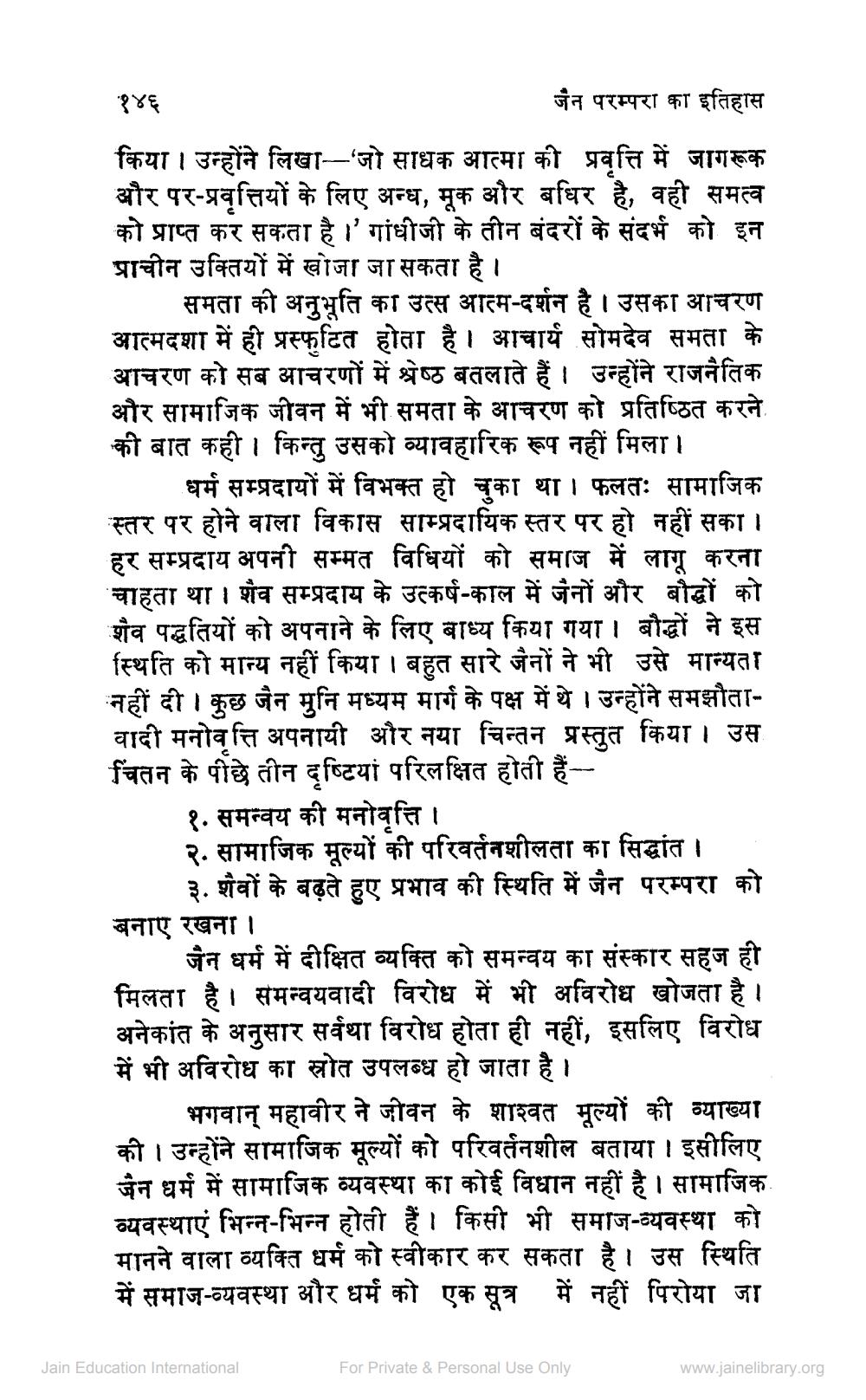________________
१४६
जैन परम्परा का इतिहास किया। उन्होंने लिखा- 'जो साधक आत्मा की प्रवृत्ति में जागरूक
और पर-प्रवृत्तियों के लिए अन्ध, मूक और बधिर है, वही समत्व को प्राप्त कर सकता है।' गांधीजी के तीन बंदरों के संदर्भ को इन प्राचीन उक्तियों में खोजा जा सकता है।
समता की अनुभूति का उत्स आत्म-दर्शन है । उसका आचरण आत्मदशा में ही प्रस्फुटित होता है। आचार्य सोमदेव समता के आचरण को सब आचरणों में श्रेष्ठ बतलाते हैं। उन्होंने राजनैतिक और सामाजिक जीवन में भी समता के आचरण को प्रतिष्ठित करने की बात कही। किन्तु उसको व्यावहारिक रूप नहीं मिला।
धर्म सम्प्रदायों में विभक्त हो चुका था। फलतः सामाजिक स्तर पर होने वाला विकास साम्प्रदायिक स्तर पर हो नहीं सका। हर सम्प्रदाय अपनी सम्मत विधियों को समाज में लागू करना चाहता था। शैव सम्प्रदाय के उत्कर्ष-काल में जैनों और बौद्धों को शैव पद्धतियों को अपनाने के लिए बाध्य किया गया। बौद्धों ने इस स्थिति को मान्य नहीं किया । बहुत सारे जैनों ने भी उसे मान्यता नहीं दी। कुछ जैन मुनि मध्यम मार्ग के पक्ष में थे। उन्होंने समझौतावादी मनोवृत्ति अपनायी और नया चिन्तन प्रस्तुत किया। उस चिंतन के पीछे तीन दृष्टियां परिलक्षित होती हैं
१. समन्वय की मनोवृत्ति । २. सामाजिक मूल्यों की परिवर्तनशीलता का सिद्धांत ।
३. शैवों के बढ़ते हुए प्रभाव की स्थिति में जैन परम्परा को बनाए रखना।
जैन धर्म में दीक्षित व्यक्ति को समन्वय का संस्कार सहज ही मिलता है। समन्वयवादी विरोध में भी अविरोध खोजता है । अनेकांत के अनुसार सर्वथा विरोध होता ही नहीं, इसलिए विरोध में भी अविरोध का स्रोत उपलब्ध हो जाता है।
भगवान् महावीर ने जीवन के शाश्वत मूल्यों की व्याख्या की। उन्होंने सामाजिक मूल्यों को परिवर्तनशील बताया। इसीलिए जैन धर्म में सामाजिक व्यवस्था का कोई विधान नहीं है । सामाजिक व्यवस्थाएं भिन्न-भिन्न होती हैं। किसी भी समाज-व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति धर्म को स्वीकार कर सकता है। उस स्थिति में समाज-व्यवस्था और धर्म को एक सूत्र में नहीं पिरोया जा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org