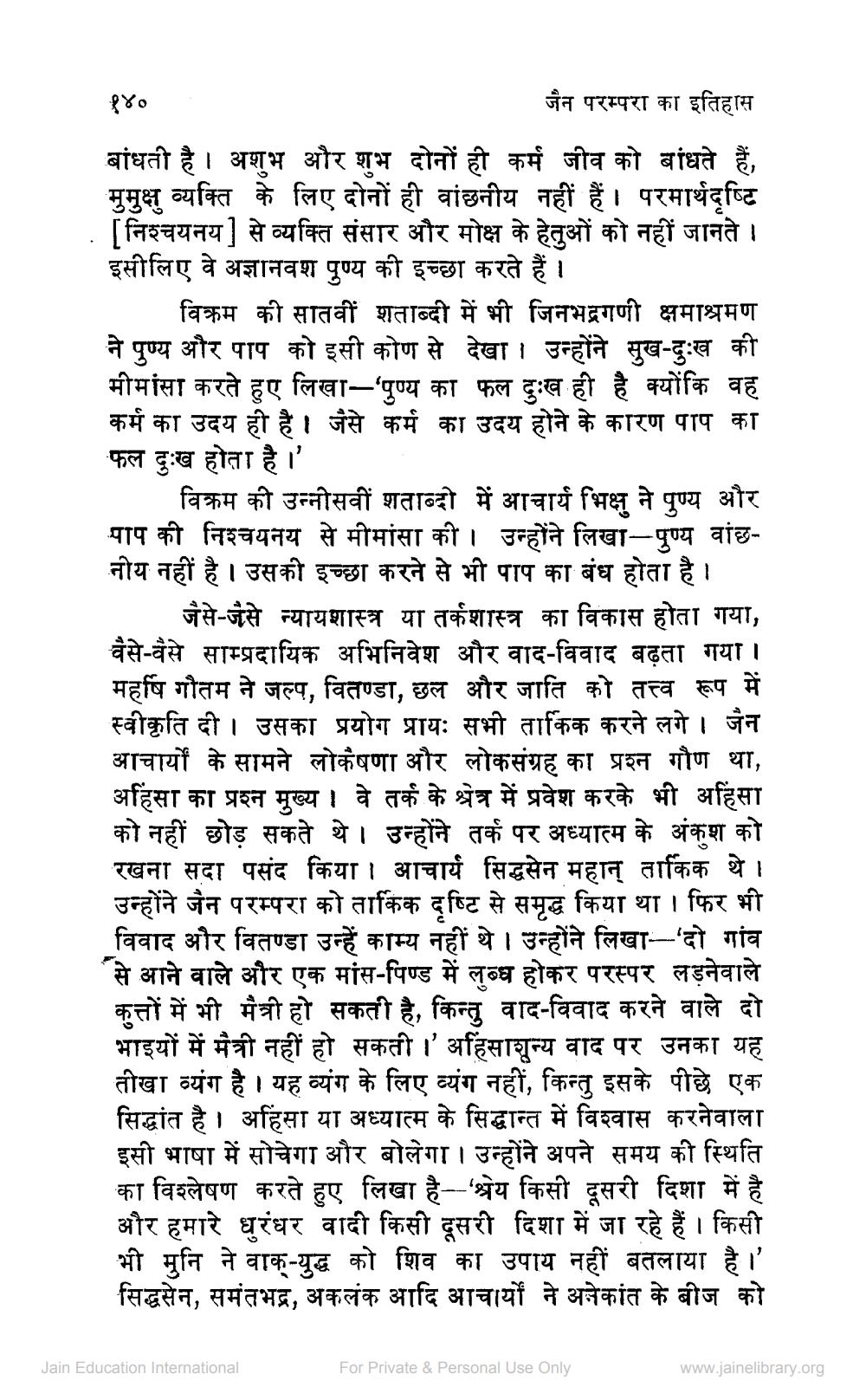________________
१४०
जैन परम्परा का इतिहास
बांधती है। अशुभ और शुभ दोनों ही कर्म जीव को बांधते हैं, मुमुक्षु व्यक्ति के लिए दोनों ही वांछनीय नहीं हैं। परमार्थदृष्टि [निश्चयनय] से व्यक्ति संसार और मोक्ष के हेतुओं को नहीं जानते। इसीलिए वे अज्ञानवश पुण्य की इच्छा करते हैं।
विक्रम की सातवीं शताब्दी में भी जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने पुण्य और पाप को इसी कोण से देखा। उन्होंने सुख-दुःख की मीमांसा करते हुए लिखा-'पुण्य का फल दुःख ही है क्योंकि वह कर्म का उदय ही है। जैसे कर्म का उदय होने के कारण पाप का फल दुःख होता है।'
विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी में आचार्य भिक्षु ने पुण्य और पाप की निश्चयनय से मीमांसा की। उन्होंने लिखा-पुण्य वांछनीय नहीं है । उसकी इच्छा करने से भी पाप का बंध होता है।
जैसे-जैसे न्यायशास्त्र या तर्कशास्त्र का विकास होता गया, वैसे-वैसे साम्प्रदायिक अभिनिवेश और वाद-विवाद बढ़ता गया। महर्षि गौतम ने जल्प, वितण्डा, छल और जाति को तत्त्व रूप में स्वीकृति दी। उसका प्रयोग प्रायः सभी ताकिक करने लगे। जैन आचार्यों के सामने लोकषणा और लोकसंग्रह का प्रश्न गौण था, अहिंसा का प्रश्न मुख्य । वे तर्क के श्रेत्र में प्रवेश करके भी अहिंसा को नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने तर्क पर अध्यात्म के अंकुश को रखना सदा पसंद किया। आचार्य सिद्धसेन महान् तार्किक थे। उन्होंने जैन परम्परा को तार्किक दष्टि से समृद्ध किया था। फिर भी विवाद और वितण्डा उन्हें काम्य नहीं थे। उन्होंने लिखा-'दो गांव से आने वाले और एक मांस-पिण्ड में लुब्ध होकर परस्पर लड़नेवाले कुत्तों में भी मैत्री हो सकती है, किन्तु वाद-विवाद करने वाले दो भाइयों में मैत्री नहीं हो सकती।' अहिंसाशून्य वाद पर उनका यह तीखा व्यंग है। यह व्यंग के लिए व्यंग नहीं, किन्तु इसके पीछे एक सिद्धांत है। अहिंसा या अध्यात्म के सिद्धान्त में विश्वास करनेवाला इसी भाषा में सोचेगा और बोलेगा। उन्होंने अपने समय की स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखा है--'श्रेय किसी दूसरी दिशा में है और हमारे धुरंधर वादी किसी दूसरी दिशा में जा रहे हैं । किसी भी मुनि ने वाक्-युद्ध को शिव का उपाय नहीं बतलाया है।' सिद्धसेन, समंतभद्र, अकलंक आदि आचार्यों ने अनेकांत के बीज को
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org