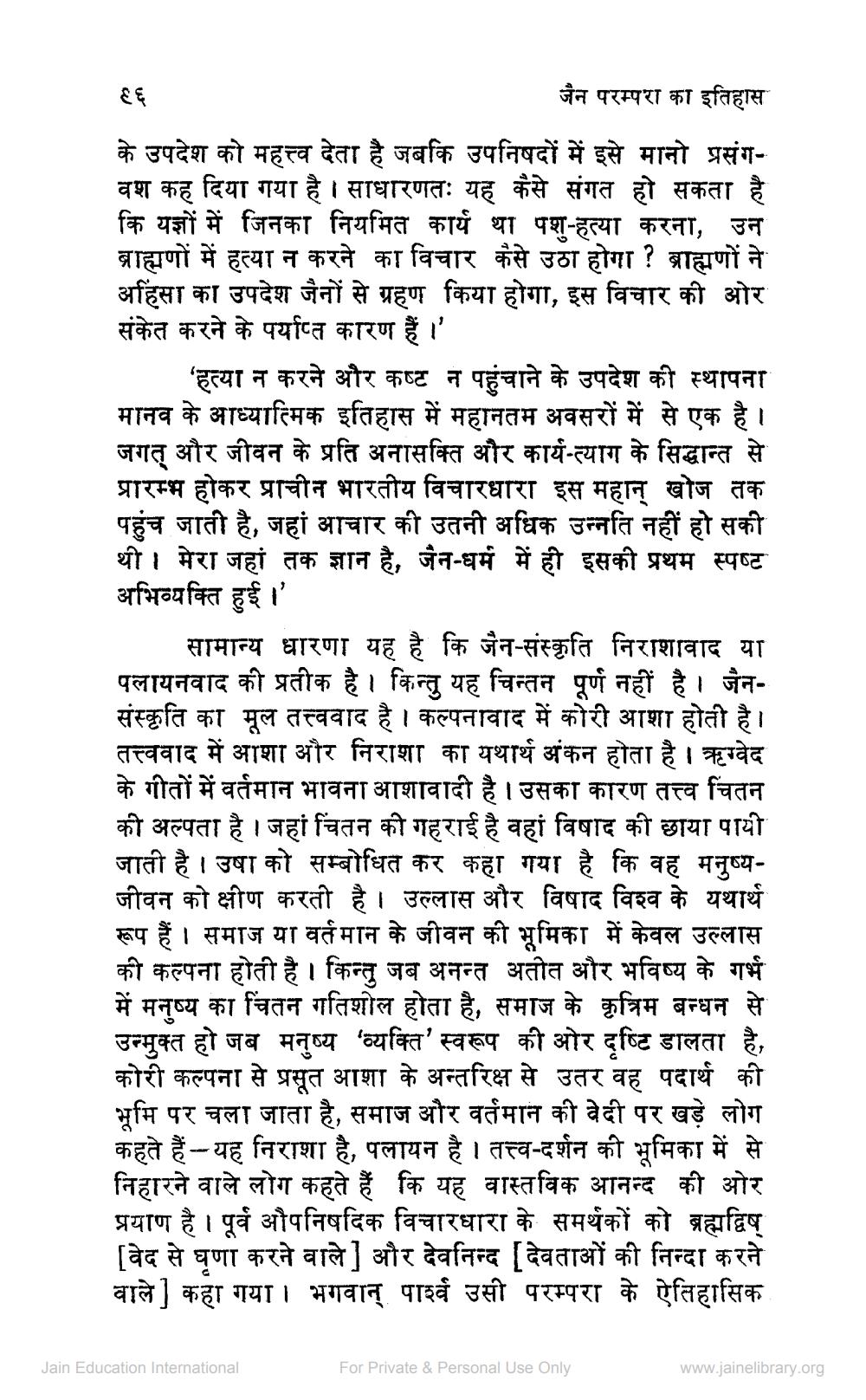________________
जैन परम्परा का इतिहास
के उपदेश को महत्त्व देता है जबकि उपनिषदों में इसे मानो प्रसंगवश कह दिया गया है । साधारणतः यह कैसे संगत हो सकता है कि यज्ञों में जिनका नियमित कार्य था पशु-हत्या करना, उन ब्राह्मणों में हत्या न करने का विचार कैसे उठा होगा? ब्राह्मणों ने अहिंसा का उपदेश जैनों से ग्रहण किया होगा, इस विचार की ओर संकेत करने के पर्याप्त कारण हैं।'
'हत्या न करने और कष्ट न पहुंचाने के उपदेश की स्थापना मानव के आध्यात्मिक इतिहास में महानतम अवसरों में से एक है। जगत् और जीवन के प्रति अनासक्ति और कार्य-त्याग के सिद्धान्त से प्रारम्भ होकर प्राचीन भारतीय विचारधारा इस महान् खोज तक पहुंच जाती है, जहां आचार की उतनी अधिक उन्नति नहीं हो सकी थी। मेरा जहां तक ज्ञान है, जैन-धर्म में ही इसकी प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई।'
सामान्य धारणा यह है कि जैन-संस्कृति निराशावाद या पलायनवाद की प्रतीक है। किन्तु यह चिन्तन पूर्ण नहीं है। जैनसंस्कृति का मूल तत्त्ववाद है। कल्पनावाद में कोरी आशा होती है। तत्त्ववाद में आशा और निराशा का यथार्थ अंकन होता है । ऋग्वेद के गीतों में वर्तमान भावना आशावादी है । उसका कारण तत्त्व चिंतन की अल्पता है । जहां चिंतन की गहराई है वहां विषाद की छाया पायी जाती है। उषा को सम्बोधित कर कहा गया है कि वह मनुष्यजीवन को क्षीण करती है। उल्लास और विषाद विश्व के यथार्थ रूप हैं। समाज या वर्तमान के जीवन की भूमिका में केवल उल्लास की कल्पना होती है। किन्तु जब अनन्त अतीत और भविष्य के गर्भ में मनुष्य का चिंतन गतिशोल होता है, समाज के कृत्रिम बन्धन से उन्मुक्त हो जब मनुष्य 'व्यक्ति' स्वरूप की ओर दृष्टि डालता है, कोरी कल्पना से प्रसूत आशा के अन्तरिक्ष से उतर वह पदार्थ की भूमि पर चला जाता है, समाज और वर्तमान की वेदी पर खड़े लोग कहते हैं- यह निराशा है, पलायन है । तत्त्व-दर्शन की भूमिका में से निहारने वाले लोग कहते हैं कि यह वास्तविक आनन्द की ओर प्रयाण है । पूर्व औपनिषदिक विचारधारा के समर्थकों को ब्रह्मविष् [वेद से घृणा करने वाले और देवनिन्द [देवताओं की निन्दा करने वाले] कहा गया। भगवान् पार्श्व उसी परम्परा के ऐतिहासिक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org