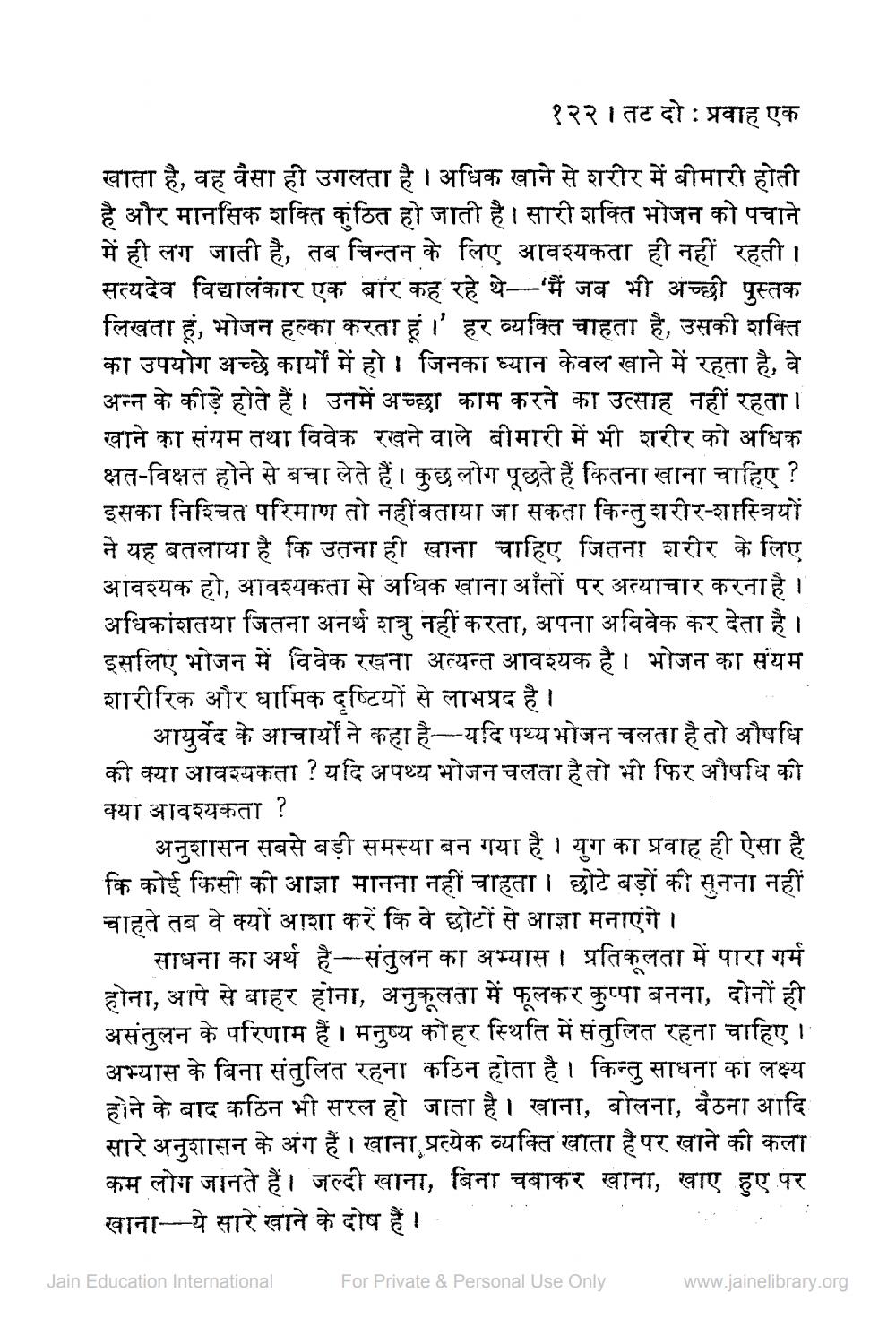________________
१२२ । तट दो : प्रवाह एक
खाता है, वह वैसा ही उगलता है । अधिक खाने से शरीर में बीमारी होती है और मानसिक शक्ति कुंठित हो जाती है । सारी शक्ति भोजन को पचाने में ही लग जाती है, तब चिन्तन के लिए आवश्यकता ही नहीं रहती । सत्यदेव विद्यालंकार एक बार कह रहे थे— ' मैं जब भी अच्छी पुस्तक लिखता हूं, भोजन हल्का करता हूं ।' हर व्यक्ति चाहता है, उसकी शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में हो । जिनका ध्यान केवल खाने में रहता है, वे अन्न के कीड़े होते हैं । उनमें अच्छा काम करने का उत्साह नहीं रहता । खाने का संगम तथा विवेक रखने वाले बीमारी में भी शरीर को अधिक क्षत-विक्षत होने से बचा लेते हैं । कुछ लोग पूछते हैं कितना खाना चाहिए ? इसका निश्चित परिमाण तो नहीं बताया जा सकता किन्तु शरीर-शास्त्रियों ने यह बतलाया है कि उतना ही खाना चाहिए जितना शरीर के लिए आवश्यक हो, आवश्यकता से अधिक खाना आँतों पर अत्याचार करना है । अधिकांशतया जितना अनर्थ शत्रु नहीं करता, अपना अविवेक कर देता है । इसलिए भोजन में विवेक रखना अत्यन्त आवश्यक है। भोजन का संयम शारीरिक और धार्मिक दृष्टियों से लाभप्रद है ।
आयुर्वेद के आचार्यों ने कहा है- यदि पथ्य भोजन चलता है तो औषधि की क्या आवश्यकता ? यदि अपथ्य भोजन चलता है तो भी फिर औषधि की क्या आवश्यकता ?
अनुशासन सबसे बड़ी समस्या बन गया है । युग का प्रवाह ही ऐसा है कि कोई किसी की आज्ञा मानना नहीं चाहता। छोटे बड़ों की सुनना नहीं चाहते तब वे क्यों आशा करें कि वे छोटों से आज्ञा मनाएंगे ।
साधना का अर्थ है-संतुलन का अभ्यास । प्रतिकूलता में पारा गर्म होना, आपे से बाहर होना, अनुकूलता में फूलकर कुप्पा बनना, दोनों ही असंतुलन के परिणाम हैं। मनुष्य को हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए। अभ्यास के बिना संतुलित रहना कठिन होता है । किन्तु साधना का लक्ष्य होने के बाद कठिन भी सरल हो जाता है । खाना, बोलना, बैठना आदि सारे अनुशासन 'के अंग हैं । खाना प्रत्येक व्यक्ति खाता है पर खाने की कला कम लोग जानते हैं। जल्दी खाना, बिना चबाकर खाना खाए हुए पर खाना - ये सारे खाने के दोष हैं ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org