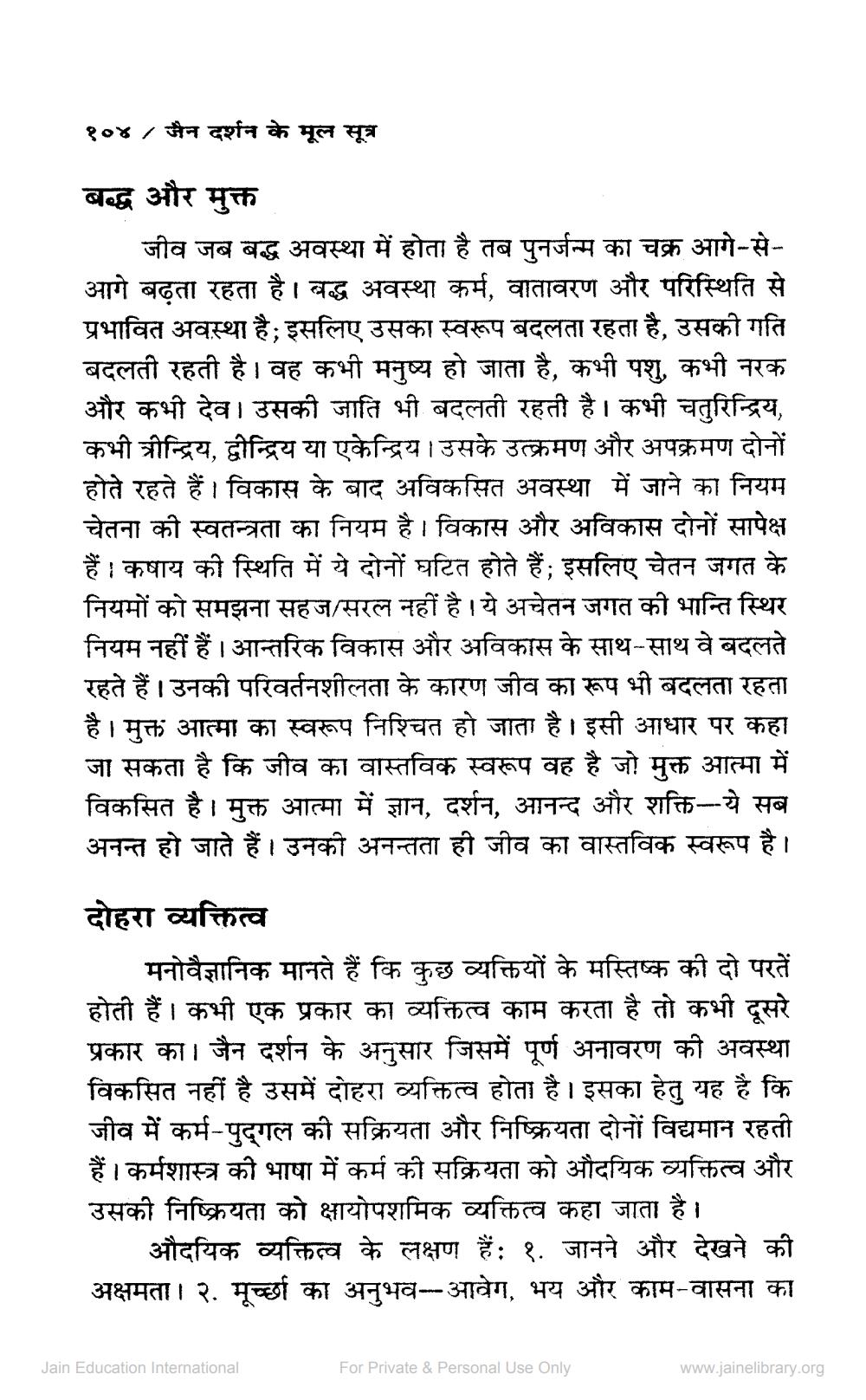________________
१०४ / जैन दर्शन के मूल सूत्र
बद्ध और मुक्त
जीव जब बद्ध अवस्था में होता है तब पुनर्जन्म का चक्र आगे-सेआगे बढ़ता रहता है। बद्ध अवस्था कर्म, वातावरण और परिस्थिति से प्रभावित अवस्था है; इसलिए उसका स्वरूप बदलता रहता है, उसकी गति बदलती रहती है। वह कभी मनुष्य हो जाता है, कभी पशु, कभी नरक और कभी देव। उसकी जाति भी बदलती रहती है। कभी चतुरिन्द्रिय, कभी त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय या एकेन्द्रिय । उसके उत्क्रमण और अपक्रमण दोनों होते रहते हैं। विकास के बाद अविकसित अवस्था में जाने का नियम चेतना की स्वतन्त्रता का नियम है। विकास और अविकास दोनों सापेक्ष हैं। कषाय की स्थिति में ये दोनों घटित होते हैं; इसलिए चेतन जगत के नियमों को समझना सहज/सरल नहीं है। ये अचेतन जगत की भान्ति स्थिर नियम नहीं हैं । आन्तरिक विकास और अविकास के साथ-साथ वे बदलते रहते हैं। उनकी परिवर्तनशीलता के कारण जीव का रूप भी बदलता रहता है। मुक्त आत्मा का स्वरूप निश्चित हो जाता है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि जीव का वास्तविक स्वरूप वह है जो मुक्त आत्मा में विकसित है। मुक्त आत्मा में ज्ञान, दर्शन, आनन्द और शक्ति-ये सब अनन्त हो जाते हैं। उनकी अनन्तता ही जीव का वास्तविक स्वरूप है।
दोहरा व्यक्तित्व
मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क की दो परतें होती हैं। कभी एक प्रकार का व्यक्तित्व काम करता है तो कभी दूसरे प्रकार का। जैन दर्शन के अनुसार जिसमें पूर्ण अनावरण की अवस्था विकसित नहीं है उसमें दोहरा व्यक्तित्व होता है। इसका हेतु यह है कि जीव में कर्म-पुद्गल की सक्रियता और निष्क्रियता दोनों विद्यमान रहती हैं। कर्मशास्त्र की भाषा में कर्म की सक्रियता को औदयिक व्यक्तित्व और उसकी निष्क्रियता को क्षायोपशमिक व्यक्तित्व कहा जाता है।
औदयिक व्यक्तित्व के लक्षण हैं: १. जानने और देखने की अक्षमता। २. मूर्छा का अनुभव-आवेग, भय और काम-वासना का
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org