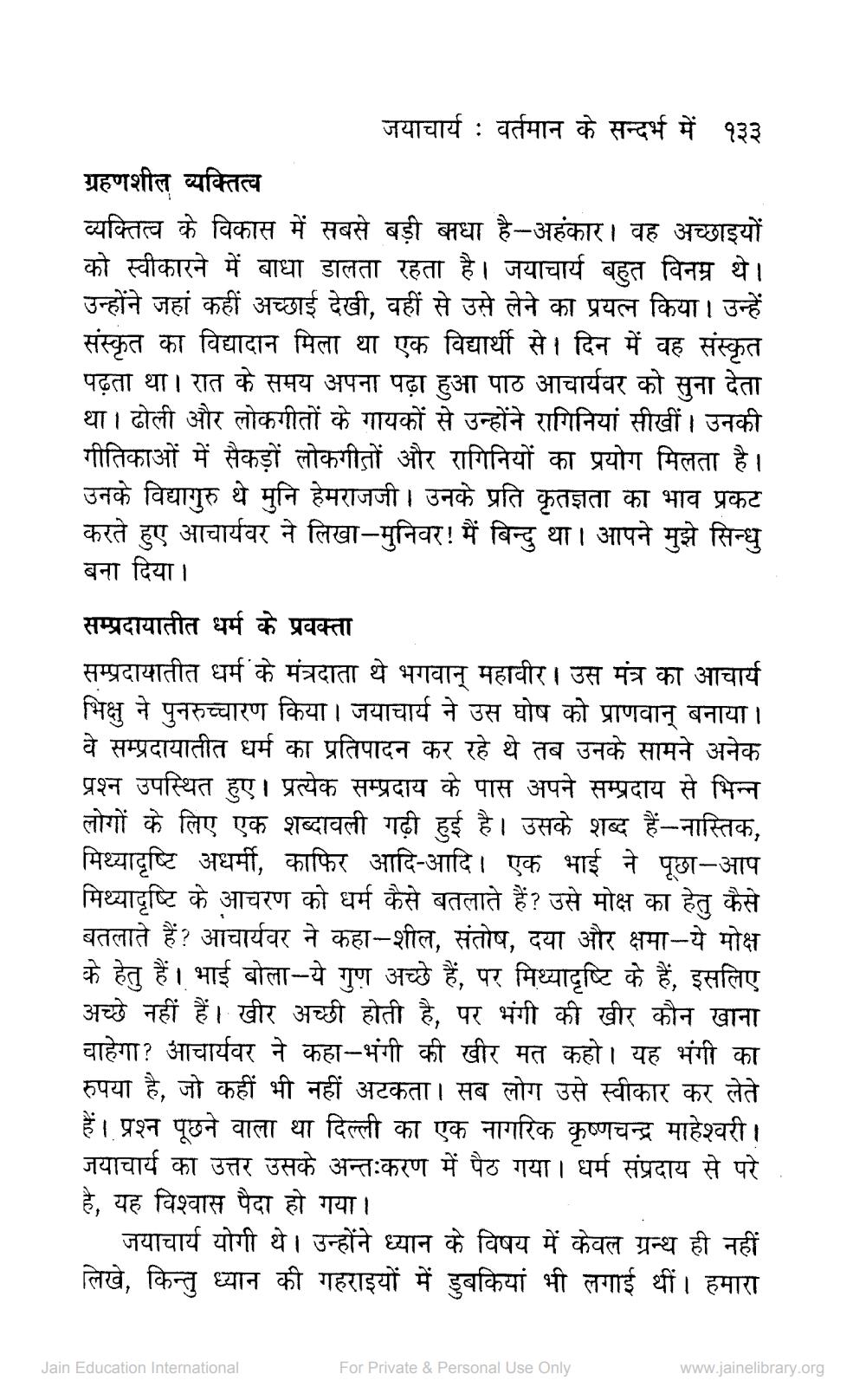________________
जयाचार्य : वर्तमान के सन्दर्भ में १३३ ग्रहणशील व्यक्तित्व व्यक्तित्व के विकास में सबसे बड़ी बधा है-अहंकार। वह अच्छाइयों को स्वीकारने में बाधा डालता रहता है। जयाचार्य बहुत विनम्र थे। उन्होंने जहां कहीं अच्छाई देखी, वहीं से उसे लेने का प्रयत्न किया। उन्हें संस्कृत का विद्यादान मिला था एक विद्यार्थी से। दिन में वह संस्कृत पढ़ता था। रात के समय अपना पढ़ा हुआ पाठ आचार्यवर को सुना देता था। ढोली और लोकगीतों के गायकों से उन्होंने रागिनियां सीखीं। उनकी गीतिकाओं में सैकड़ों लोकगीतों और रागिनियों का प्रयोग मिलता है। उनके विद्यागुरु थे मुनि हेमराजजी। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए आचार्यवर ने लिखा-मुनिवर ! मैं बिन्दु था। आपने मुझे सिन्धु बना दिया। सम्प्रदायातीत धर्म के प्रवक्ता सम्प्रदायातीत धर्म के मंत्रदाता थे भगवान् महावीर । उस मंत्र का आचार्य भिक्षु ने पुनरुच्चारण किया। जयाचार्य ने उस घोष को प्राणवान् बनाया। वे सम्प्रदायातीत धर्म का प्रतिपादन कर रहे थे तब उनके सामने अनेक प्रश्न उपस्थित हुए। प्रत्येक सम्प्रदाय के पास अपने सम्प्रदाय से भिन्न लोगों के लिए एक शब्दावली गढ़ी हुई है। उसके शब्द हैं-नास्तिक, मिथ्यादृष्टि अधर्मी, काफिर आदि-आदि। एक भाई ने पूछा-आप मिथ्यादृष्टि के आचरण को धर्म कैसे बतलाते हैं? उसे मोक्ष का हेतु कैसे बतलाते हैं? आचार्यवर ने कहा-शील, संतोष, दया और क्षमा-ये मोक्ष के हेतु हैं। भाई बोला-ये गुण अच्छे हैं, पर मिथ्यादृष्टि के हैं, इसलिए अच्छे नहीं हैं। खीर अच्छी होती है, पर भंगी की खीर कौन खाना चाहेगा? आचार्यवर ने कहा-भंगी की खीर मत कहो। यह भंगी का रुपया है, जो कहीं भी नहीं अटकता। सब लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। प्रश्न पूछने वाला था दिल्ली का एक नागरिक कृष्णचन्द्र माहेश्वरी। जयाचार्य का उत्तर उसके अन्तःकरण में पैठ गया। धर्म संप्रदाय से परे है, यह विश्वास पैदा हो गया। ___ जयाचार्य योगी थे। उन्होंने ध्यान के विषय में केवल ग्रन्थ ही नहीं लिखे, किन्तु ध्यान की गहराइयों में डुबकियां भी लगाई थीं। हमारा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org