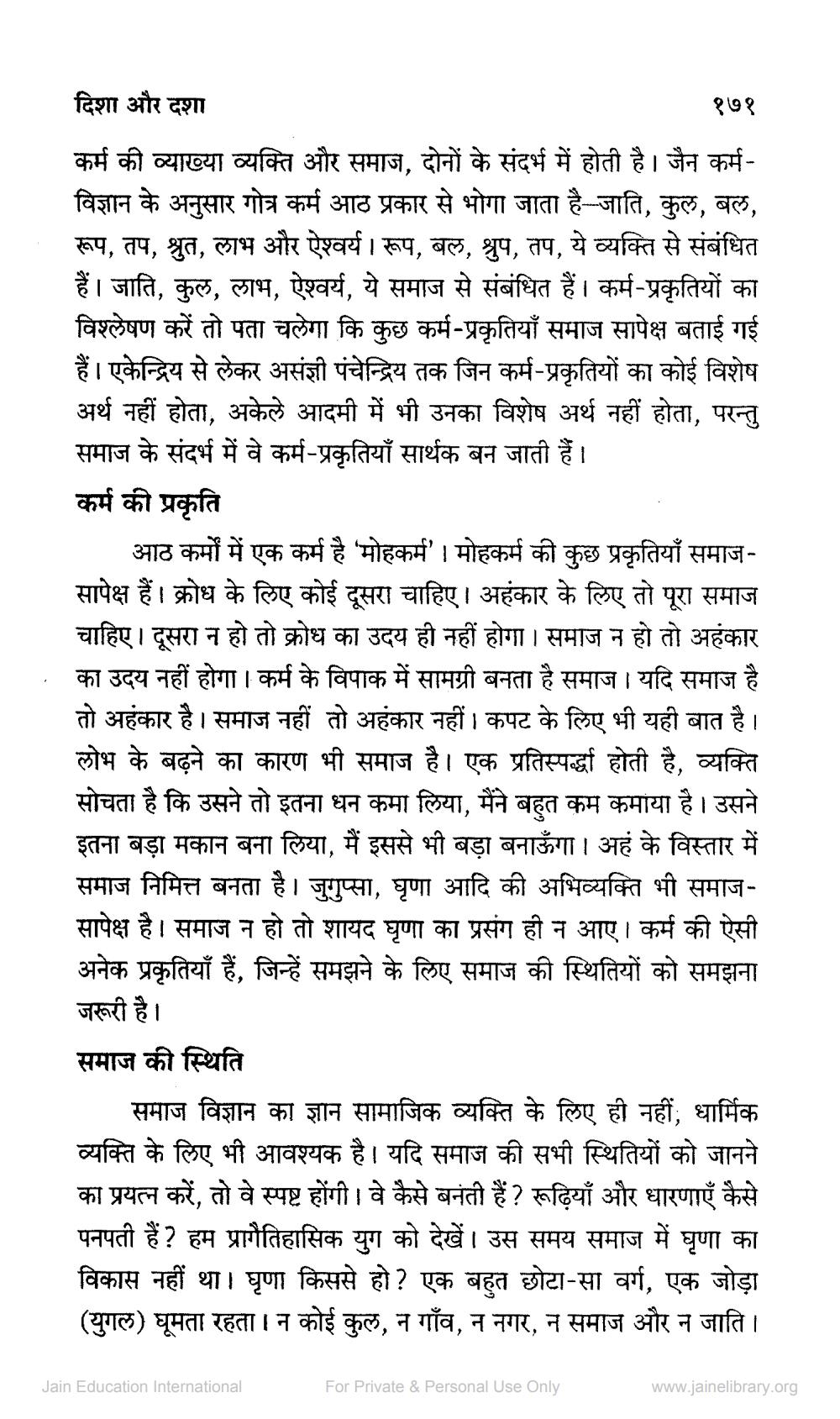________________
दिशा और दशा
१७१ कर्म की व्याख्या व्यक्ति और समाज, दोनों के संदर्भ में होती है। जैन कर्मविज्ञान के अनुसार गोत्र कर्म आठ प्रकार से भोगा जाता है-जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य । रूप, बल, श्रुप, तप, ये व्यक्ति से संबंधित हैं। जाति, कुल, लाभ, ऐश्वर्य, ये समाज से संबंधित हैं। कर्म-प्रकृतियों का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि कुछ कर्म-प्रकृतियाँ समाज सापेक्ष बताई गई हैं। एकेन्द्रिय से लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तक जिन कर्म-प्रकृतियों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, अकेले आदमी में भी उनका विशेष अर्थ नहीं होता, परन्तु समाज के संदर्भ में वे कर्म-प्रकृतियाँ सार्थक बन जाती हैं। कर्म की प्रकृति
आठ कर्मों में एक कर्म है 'मोहकर्म' । मोहकर्म की कुछ प्रकृतियाँ समाजसापेक्ष हैं। क्रोध के लिए कोई दूसरा चाहिए। अहंकार के लिए तो पूरा समाज चाहिए। दूसरा न हो तो क्रोध का उदय ही नहीं होगा। समाज न हो तो अहंकार का उदय नहीं होगा। कर्म के विपाक में सामग्री बनता है समाज । यदि समाज है तो अहंकार है। समाज नहीं तो अहंकार नहीं । कपट के लिए भी यही बात है। लोभ के बढ़ने का कारण भी समाज है। एक प्रतिस्पर्धा होती है, व्यक्ति सोचता है कि उसने तो इतना धन कमा लिया, मैंने बहुत कम कमाया है। उसने इतना बड़ा मकान बना लिया, मैं इससे भी बड़ा बनाऊँगा। अहं के विस्तार में समाज निमित्त बनता है। जुगुप्सा, घृणा आदि की अभिव्यक्ति भी समाजसापेक्ष है। समाज न हो तो शायद घृणा का प्रसंग ही न आए। कर्म की ऐसी अनेक प्रकृतियाँ हैं, जिन्हें समझने के लिए समाज की स्थितियों को समझना जरूरी है। समाज की स्थिति
समाज विज्ञान का ज्ञान सामाजिक व्यक्ति के लिए ही नहीं, धार्मिक व्यक्ति के लिए भी आवश्यक है। यदि समाज की सभी स्थितियों को जानने का प्रयत्न करें, तो वे स्पष्ट होंगी। वे कैसे बनती हैं? रूढ़ियाँ और धारणाएँ कैसे पनपती हैं? हम प्रागैतिहासिक युग को देखें। उस समय समाज में घृणा का विकास नहीं था। घृणा किससे हो? एक बहुत छोटा-सा वर्ग, एक जोड़ा (युगल) घूमता रहता । न कोई कुल, न गाँव, न नगर, न समाज और न जाति ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org