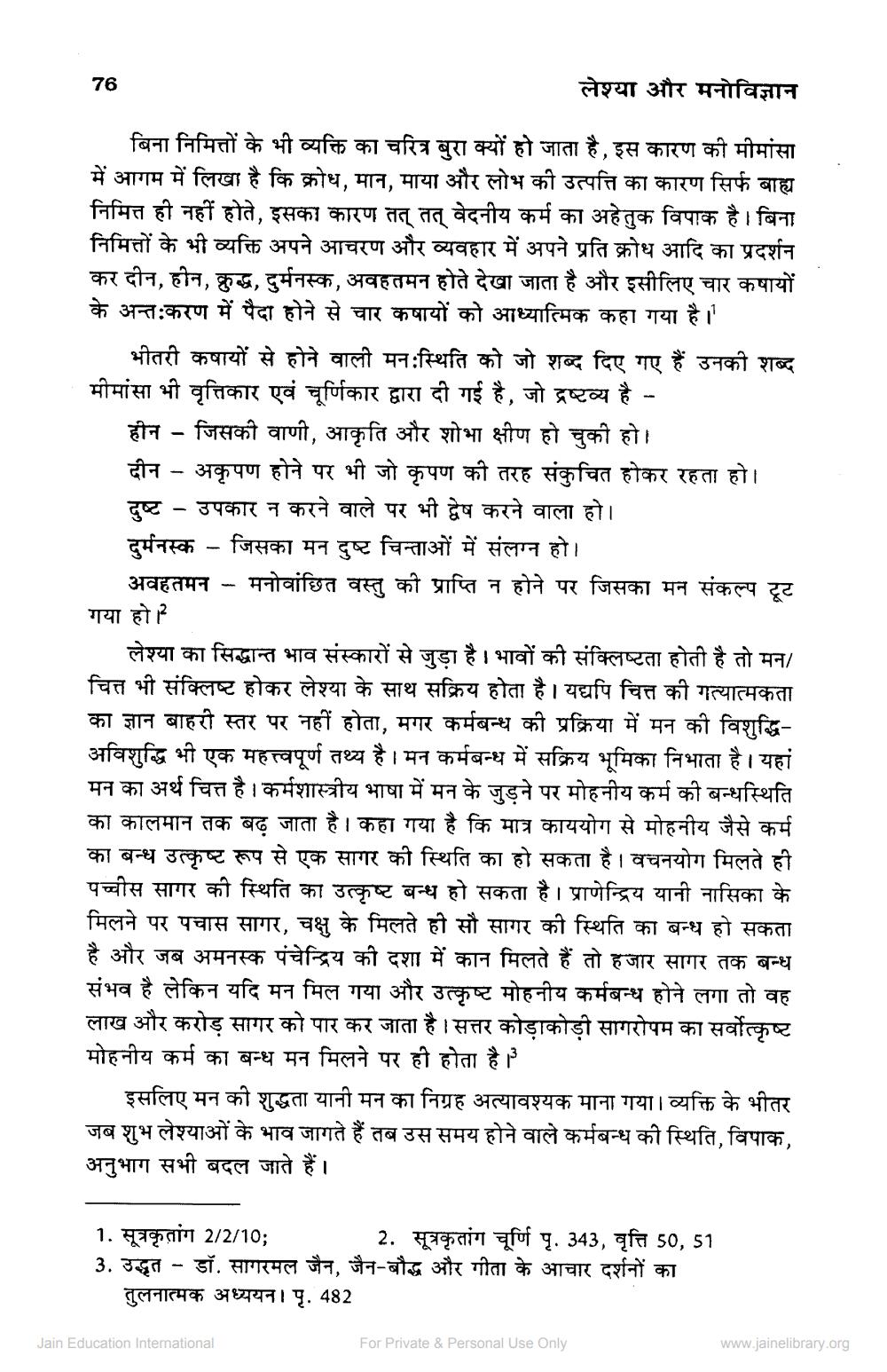________________
76
लेश्या और मनोविज्ञान
बिना निमित्तों के भी व्यक्ति का चरित्र बुरा क्यों हो जाता है, इस कारण की मीमांसा में आगम में लिखा है कि क्रोध, मान, माया और लोभ की उत्पत्ति का कारण सिर्फ बाह्य निमित्त ही नहीं होते, इसका कारण तत् तत् वेदनीय कर्म का अहेतुक विपाक है। बिना निमित्तों के भी व्यक्ति अपने आचरण और व्यवहार में अपने प्रति क्रोध आदि का प्रदर्शन कर दीन, हीन, क्रुद्ध, दुर्मनस्क, अवहतमन होते देखा जाता है और इसीलिए चार कषायों के अन्त:करण में पैदा होने से चार कषायों को आध्यात्मिक कहा गया है।'
भीतरी कषायों से होने वाली मन:स्थिति को जो शब्द दिए गए हैं उनकी शब्द मीमांसा भी वृत्तिकार एवं चूर्णिकार द्वारा दी गई है, जो द्रष्टव्य है -
हीन - जिसकी वाणी, आकृति और शोभा क्षीण हो चुकी हो। दीन - अकृपण होने पर भी जो कृपण की तरह संकुचित होकर रहता हो। दुष्ट - उपकार न करने वाले पर भी द्वेष करने वाला हो। दुर्मनस्क - जिसका मन दुष्ट चिन्ताओं में संलग्न हो।
अवहतमन - मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति न होने पर जिसका मन संकल्प टूट गया हो।
लेश्या का सिद्धान्त भाव संस्कारों से जुड़ा है। भावों की संक्लिष्टता होती है तो मन/ चित्त भी संक्लिष्ट होकर लेश्या के साथ सक्रिय होता है। यद्यपि चित्त की गत्यात्मकता का ज्ञान बाहरी स्तर पर नहीं होता, मगर कर्मबन्ध की प्रक्रिया में मन की विशुद्धिअविशुद्धि भी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है। मन कर्मबन्ध में सक्रिय भूमिका निभाता है। यहां मन का अर्थ चित्त है। कर्मशास्त्रीय भाषा में मन के जुड़ने पर मोहनीय कर्म की बन्धस्थिति का कालमान तक बढ़ जाता है। कहा गया है कि मात्र काययोग से मोहनीय जैसे कर्म का बन्ध उत्कृष्ट रूप से एक सागर की स्थिति का हो सकता है । वचनयोग मिलते ही पच्चीस सागर की स्थिति का उत्कृष्ट बन्ध हो सकता है। प्राणेन्द्रिय यानी नासिका के मिलने पर पचास सागर, चक्षु के मिलते ही सौ सागर की स्थिति का बन्ध हो सकता
है और जब अमनस्क पंचेन्द्रिय की दशा में कान मिलते हैं तो हजार सागर तक बन्ध
संभव है लेकिन यदि मन मिल गया और उत्कृष्ट मोहनीय कर्मबन्ध होने लगा तो वह लाख और करोड़ सागर को पार कर जाता है। सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम का सर्वोत्कृष्ट मोहनीय कर्म का बन्ध मन मिलने पर ही होता है।'
इसलिए मन की शुद्धता यानी मन का निग्रह अत्यावश्यक माना गया। व्यक्ति के भीतर जब शुभ लेश्याओं के भाव जागते हैं तब उस समय होने वाले कर्मबन्ध की स्थिति, विपाक, अनुभाग सभी बदल जाते हैं।
1. सूत्रकृतांग 2/2/10; 2. सूत्रकृतांग चूर्णि पृ. 343, वृत्ति 50, 51 3. उद्धृत - डॉ. सागरमल जैन, जैन-बौद्ध और गीता के आचार दर्शनों का
तुलनात्मक अध्ययन। पृ. 482
Jain Education Interational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org