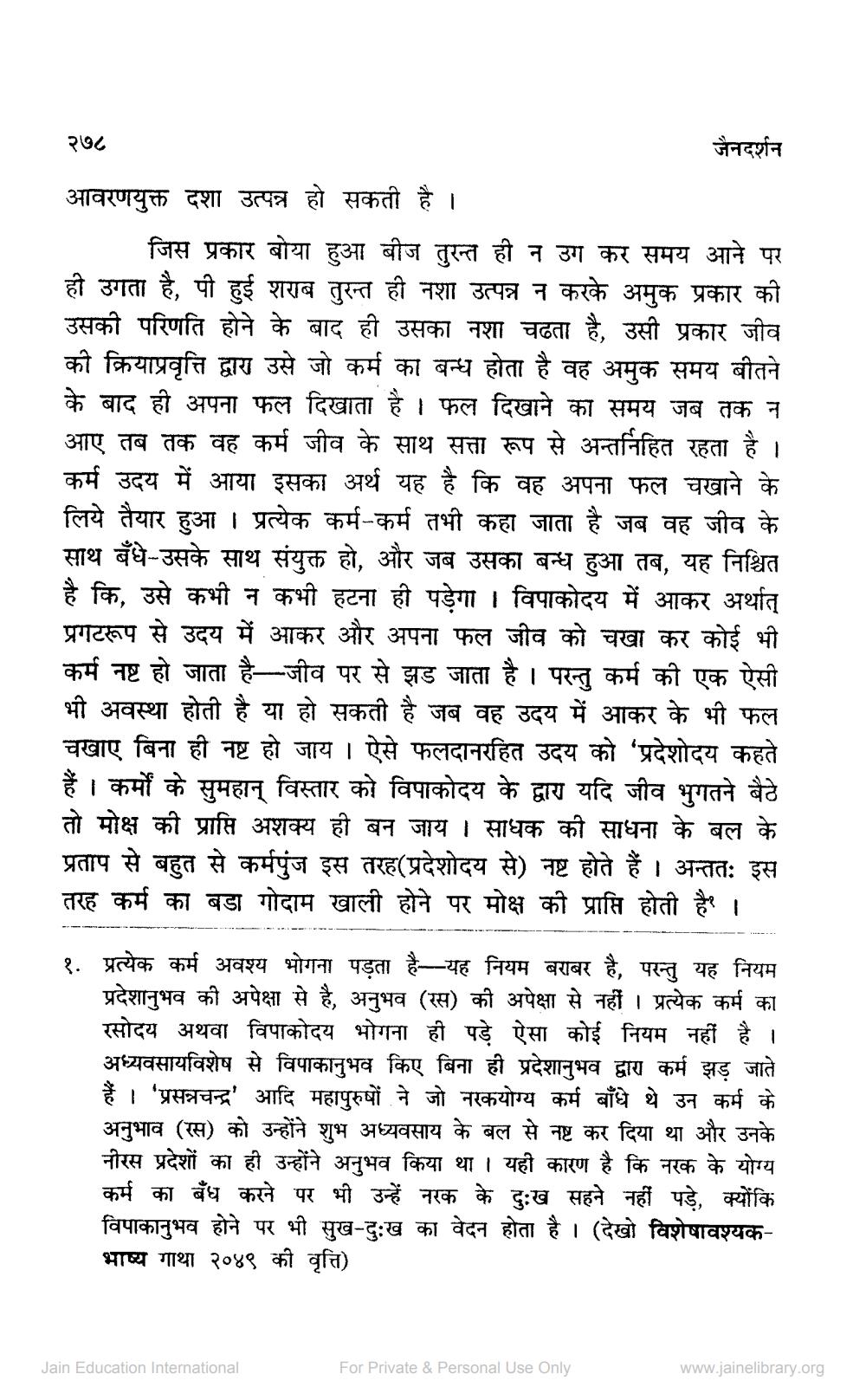________________
२७८
जैनदर्शन
आवरणयुक्त दशा उत्पन्न हो सकती है ।
जिस प्रकार बोया हुआ बीज तुरन्त ही न उग कर समय आने पर ही उगता है, पी हुई शराब तुरन्त ही नशा उत्पन्न न करके अमुक प्रकार की उसकी परिणति होने के बाद ही उसका नशा चढता है, उसी प्रकार जीव की क्रियाप्रवृत्ति द्वारा उसे जो कर्म का बन्ध होता है वह अमुक समय बीतने के बाद ही अपना फल दिखाता है । फल दिखाने का समय जब तक न आए तब तक वह कर्म जीव के साथ सत्ता रूप से अन्तर्निहित रहता है । कर्म उदय में आया इसका अर्थ यह है कि वह अपना फल चखाने के लिये तैयार हुआ । प्रत्येक कर्म-कर्म तभी कहा जाता है जब वह जीव के साथ बँधे-उसके साथ संयुक्त हो, और जब उसका बन्ध हुआ तब, यह निश्चित है कि, उसे कभी न कभी हटना ही पड़ेगा । विपाकोदय में आकर अर्थात् प्रगटरूप से उदय में आकर और अपना फल जीव को चखा कर कोई भी कर्म नष्ट हो जाता है—जीव पर से झड जाता है । परन्तु कर्म की एक ऐसी भी अवस्था होती है या हो सकती है जब वह उदय में आकर के भी फल चखाए बिना ही नष्ट हो जाय । ऐसे फलदानरहित उदय को 'प्रदेशोदय कहते हैं । कर्मों के सुमहान् विस्तार को विपाकोदय के द्वारा यदि जीव भुगतने बैठे तो मोक्ष की प्राप्ति अशक्य ही बन जाय । साधक की साधना के बल के प्रताप से बहुत से कर्मपुंज इस तरह(प्रदेशोदय से) नष्ट होते हैं । अन्ततः इस तरह कर्म का बडा गोदाम खाली होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है ।
१. प्रत्येक कर्म अवश्य भोगना पड़ता है-यह नियम बराबर है, परन्तु यह नियम
प्रदेशानुभव की अपेक्षा से है, अनुभव (रस) की अपेक्षा से नहीं । प्रत्येक कर्म का रसोदय अथवा विपाकोदय भोगना ही पड़े ऐसा कोई नियम नहीं है । अध्यवसायविशेष से विपाकानुभव किए बिना ही प्रदेशानुभव द्वारा कर्म झड़ जाते हैं । 'प्रसन्नचन्द्र' आदि महापुरुषों ने जो नरकयोग्य कर्म बाँधे थे उन कर्म के अनुभाव (रस) को उन्होंने शुभ अध्यवसाय के बल से नष्ट कर दिया था और उनके नीरस प्रदेशों का ही उन्होंने अनुभव किया था । यही कारण है कि नरक के योग्य कर्म का बँध करने पर भी उन्हें नरक के दुःख सहने नहीं पड़े, क्योंकि विपाकानुभव होने पर भी सुख-दुःख का वेदन होता है । (देखो विशेषावश्यकभाष्य गाथा २०४९ की वृत्ति)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org