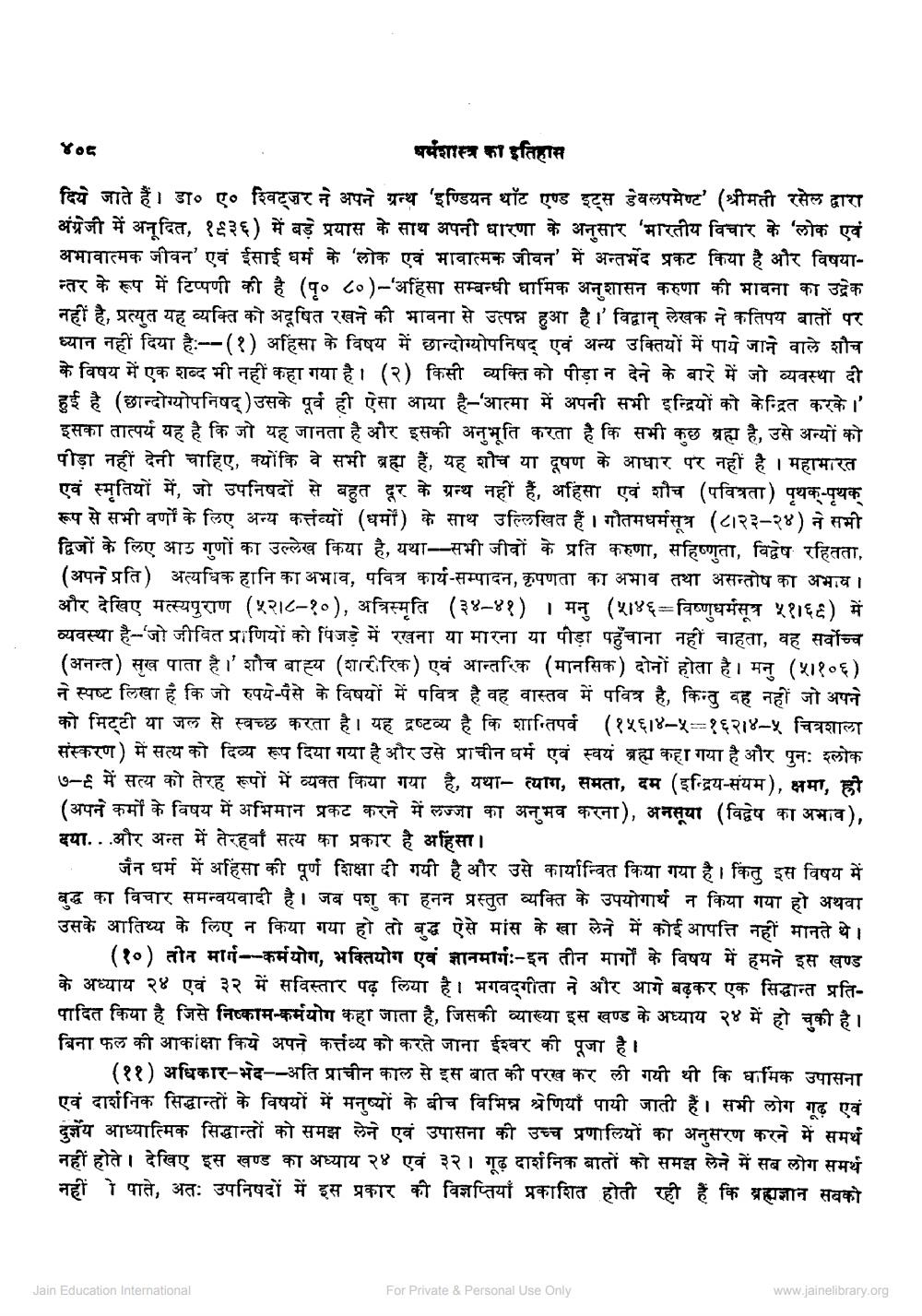________________
४००
धर्मशास्त्र का इतिहास दिये जाते हैं। डा० ए० स्विट्ज़र ने अपने ग्रन्थ 'इण्डियन थॉट एण्ड इट्स डेवलपमेण्ट' (श्रीमती रसेल द्वारा अंग्रेजी में अनदित, १६३६) में बड़े प्रयास के साथ अपनी धारणा के अनसार 'भारतीय विचार के 'लोक एवं अभावात्मक जीवन' एवं ईसाई धर्म के 'लोक एवं भावात्मक जीवन' में अन्तर्भेद प्रकट किया है और विषयान्तर के रूप में टिप्पणी की है (पृ० ८०)-'अहिंसा सम्बन्धी धार्मिक अनुशासन करुणा की भावना का उद्रेक नहीं है, प्रत्युत यह व्यक्ति को अदूषित रखने की भावना से उत्पन्न हुआ है।' विद्वान् लेखक ने कतिपय बातों पर ध्यान नहीं दिया है:--(१) अहिंसा के विषय में छान्दोग्योपनिषद् एवं अन्य उक्तियों में पाये जाने वाले शौच के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। (२) किसी व्यक्ति को पीड़ा न देने के बारे में जो व्यवस्था दी हुई है (छान्दोग्योपनिषद् ) उसके पूर्व ही ऐसा आया है-'आत्मा में अपनी सभी इन्द्रियों को केन्द्रित करके।' इसका तात्पर्य यह है कि जो यह जानता है और इसकी अनुभूति करता है कि सभी कुछ ब्रह्म है, उसे अन्यों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वे सभी ब्रह्म हैं, यह शौच या दूषण के आधार पर नहीं है । महाभारत एवं स्मृतियों में, जो उपनिषदों से बहुत दूर के ग्रन्थ नहीं हैं, अहिंसा एवं शौच (पवित्रता) पृथक्-पृथक रूप से सभी वर्गों के लिए अन्य कर्तव्यों (धर्मों) के साथ उल्लिखित हैं । गौतमधर्मसूत्र (८।२३-२४) ने सभी द्विजों के लिए आठ गुणों का उल्लेख किया है, यथा-सभी जीवों के प्रति करुणा, सहिष्णुता, विद्वेष रहितता, (अपने प्रति) अत्यधिक हानि का अभाव, पवित्र कार्य-सम्पादन, कृपणता का अभाव तथा असन्तोष का अभाव ।
और देखिए मत्स्यपुराण (५२।८-१०), अविस्मृति (३४-४१) । मनु (०४६=विष्णुधर्मसूत्र ५११६६) में व्यवस्था है-'जो जीवित प्राणियों को पिंजड़े में रखना या मारना या पीड़ा पहुँचाना नहीं चाहता, वह सर्वोच्च (अनन्त) सुख पाता है।' शौच बाह्य (शारीरिक) एवं आन्तरिक (मानसिक) दोनों होता है। मनु (५॥१०६) ने स्पष्ट लिखा है कि जो रुपये-पैसे के विषयों में पवित्र है वह वास्तव में पवित्र है, किन्तु वह नहीं जो अपने को मिट्टी या जल से स्वच्छ करता है। यह द्रष्टव्य है कि शान्तिपर्व (१५६।४-५=१६२।४-५ चित्रशाला संस्करण) में सत्य को दिव्य रूप दिया गया है और उसे प्राचीन धर्म एवं स्वयं ब्रह्म कहा गया है और पुन: इलोक ७-६ में सत्य को तेरह रूपों में व्यक्त किया गया है, यथा- त्याग, समता, दम (इन्द्रिय-संयम), क्षमा, हो (अपने कर्मों के विषय में अभिमान प्रकट करने में लज्जा का अनुभव करना), अनसूया (विद्वेष का अभाव), दया...और अन्त में तेरहवां सत्य का प्रकार है अहिंसा। व जैन धर्म में अहिंसा की पूर्ण शिक्षा दी गयी है और उसे कार्यान्वित किया गया है। किंतु इस विषय में बुद्ध का विचार समन्वयवादी है। जब पशु का हनन प्रस्तुत व्यक्ति के उपयोगार्थ न किया गया हो अथवा उसके आतिथ्य के लिए न किया गया हो तो बुद्ध ऐसे मांस के खा लेने में कोई आपत्ति नहीं मानते थे।
(१०) तीन मार्ग--कर्मयोग, भक्तियोग एवं ज्ञानमार्गः-इन तीन मार्गों के विषय में हमने इस खण्ड के अध्याय २४ एवं ३२ में सविस्तार पढ़ लिया है। भगवद्गीता ने और आगे बढ़कर एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जिसे निष्काम कर्मयोग कहा जाता है, जिसकी व्याख्या इस खण्ड के अध्याय २४ में हो चुकी है। बिना फल की आकांक्षा किये अपने कर्त्तव्य को करते जाना ईश्वर की पूजा है।
(११) अधिकार-भेद-अति प्राचीन काल से इस बात की परख कर ली गयी थी कि धर्मिक उपासना एवं दार्शनिक सिद्धान्तों के विषयों में मनुष्यों के बीच विभिन्न श्रेणियाँ पायी जाती हैं। सभी लोग गूढ़ एवं दुज्ञेय आध्यात्मिक सिद्धान्तों को समझ लेने एवं उपासना की उच्च प्रणालियों का अनुसरण करने में समर्थ नहीं होते। देखिए इस खण्ड का अध्याय २४ एवं ३२। गूढ़ दार्शनिक बातों को समझ लेने में सब लोग समर्थ नहीं । पाते, अतः उपनिषदों में इस प्रकार की विज्ञप्तियाँ प्रकाशित होती रही हैं कि ब्रह्मज्ञान सबको
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org