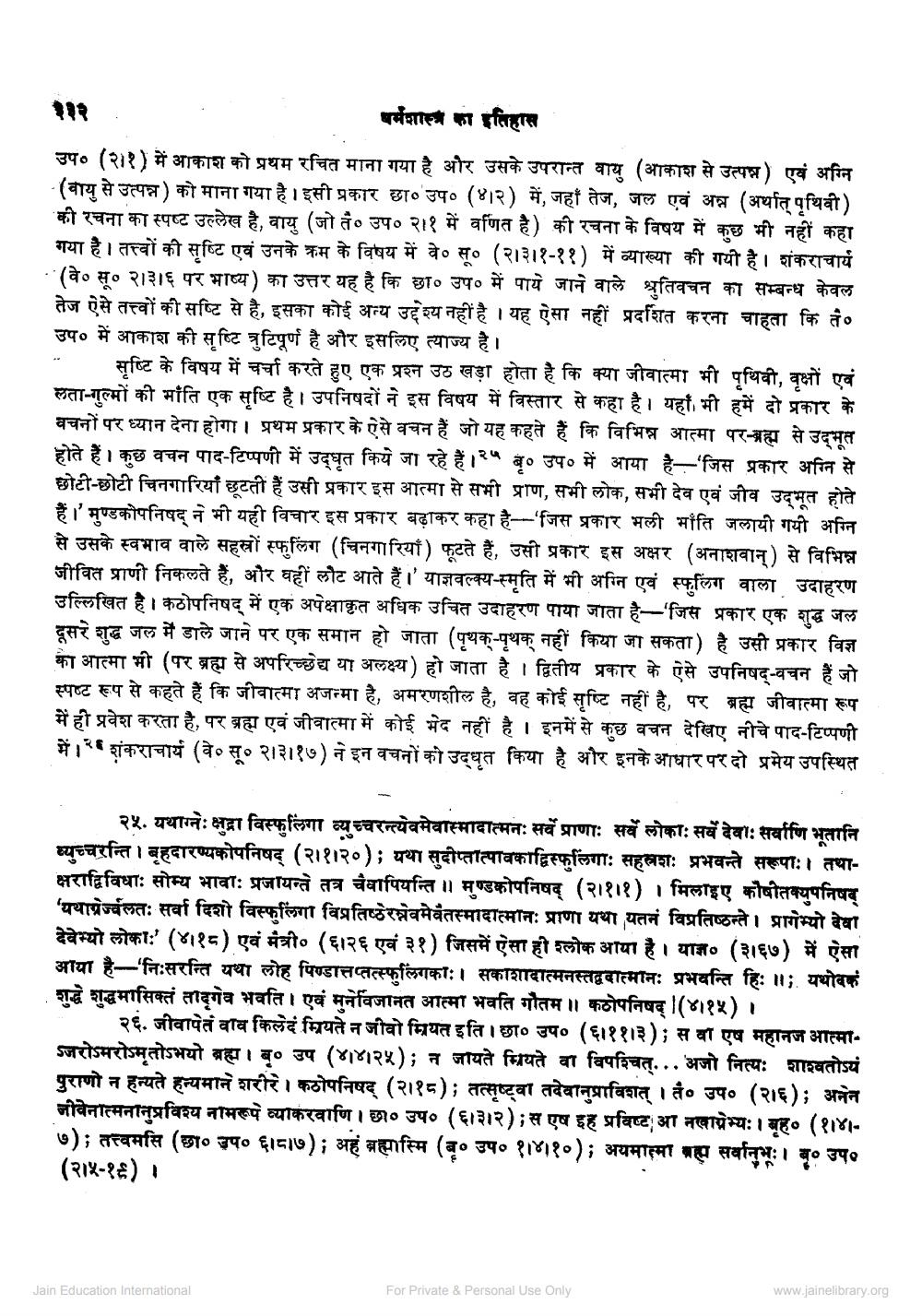________________
धर्मशास्त्र का इतिहास उप० (२११) में आकाश को प्रथम रचित माना गया है और उसके उपरान्त वायु (आकाश से उत्पन्न) एवं अग्नि -(वायु से उत्पन्न) को माना गया है । इसी प्रकार छा० उप० (४।२) में, जहाँ तेज, जल एवं अन्न (अर्थात् पृथिवी) की रचना का स्पष्ट उल्लेख है, वायु (जो तै० उप० २११ में वर्णित है) की रचना के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। तत्त्वों की सृष्टि एवं उनके क्रम के विषय में वे० सू० (२।३।१-११) में व्याख्या की गयी है। शंकराचार्य (वे० सू० २।३।६ पर भाष्य) का उत्तर यह है कि छा० उप० में पाये जाने वाले श्रुतिवचन का सम्बन्ध केवल तेज ऐसे तत्त्वों की सष्टि से है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है । यह ऐसा नहीं प्रदर्शित करना चाहता कि ते. उप० में आकाश की सृष्टि त्रुटिपूर्ण है और इसलिए त्याज्य है। - सृष्टि के विषय में चर्चा करते हुए एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि क्या जीवात्मा भी पृथिवी, वृक्षों एवं लता-गुल्मों की भांति एक सृष्टि है। उपनिषदों ने इस विषय में विस्तार से कहा है। यहाँ भी हमें दो प्रकार के वचनों पर ध्यान देना होगा। प्रथम प्रकार के ऐसे वचन हैं जो यह कहते हैं कि विभिन्न आत्मा पर-ब्रह्म से उद्भूत होते हैं। कुछ वचन पाद-टिप्पणी में उद्धृत किये जा रहे हैं।२५ बृ० उप० में आया है जिस प्रकार अग्नि से छोटी-छोटी चिनगारियां छूटती हैं उसी प्रकार इस आत्मा से सभी प्राण, सभी लोक, सभी देव एवं जीव उद्भूत होते हैं।' मुण्डकोपनिषद् ने भी यही विचार इस प्रकार बढ़ाकर कहा है-'जिस प्रकार भली भाँति जलायी गयी अग्नि से उसके स्वभाव वाले सहस्रों स्फुलिंग (चिनगारियाँ) फूटते हैं, उसी प्रकार इस अक्षर (अनाशवान्) से विभिन्न जीवित प्राणी निकलते हैं, और वहीं लौट आते हैं।' याज्ञवल्क्य-स्मृति में भी अग्नि एवं स्फुलिंग वाला उदाहरण उल्लिखित है। कठोपनिषद् में एक अपेक्षाकृत अधिक उचित उदाहरण पाया जाता है-'जिस प्रकार एक शुद्ध जल दूसरे शुद्ध जल में डाले जाने पर एक समान हो जाता (पृथक्-पृथक् नहीं किया जा सकता) है उसी प्रकार विज्ञ का आत्मा भी (पर ब्रह्म से अपरिच्छेद्य या अलक्ष्य) हो जाता है । द्वितीय प्रकार के ऐसे उपनिषद्-वचन हैं जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीवात्मा अजन्मा है, अमरणशील है, वह कोई सृष्टि नहीं है, पर ब्रह्म जीवात्मा रूप में ही प्रवेश करता है, पर ब्रह्म एवं जीवात्मा में कोई भेद नहीं है । इनमें से कुछ वचन देखिए नीचे पाद-टिप्पणी में। शंकराचार्य (वे० सू० २।३।१७) ने इन वचनों को उद्धृत किया है और इनके आधार पर दो प्रमेय उपस्थित
२५. यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि म्युच्चरन्ति । बृहदारण्यकोपनिषद् (२।१।२०); यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः। तथाक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ मुण्डकोपनिषद् (२।१३१) । मिलाइए कौषोतक्युपनिषद् 'यथाग्ने+लतः सर्वा दिशो विस्फुलिंगा विप्रतिष्ठेरनेवमेवंतस्मादात्मानः प्राणा यथा यतनं विप्रतिष्ठन्ते। प्रागेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका:' (४।१८) एवं मंत्री० (६।२६ एवं ३१) जिसमें ऐसा ही श्लोक आया है। याज्ञ० (३।६७) में ऐसा आया है-'निःसरन्ति यथा लोह पिण्डात्तप्तत्स्फुलिंगकाः । सकाशादात्मनस्तद्वदात्मानः प्रभवन्ति हिः ॥; यथोवर्क शुद्ध शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति । एवं मुविजानत आत्मा भवति गौतम ॥ कठोपनिषद् (४।१५)।
२६. जीवापेतं वाव किलेदं मियते न जीवो मियत इति । छा० उप० (६॥११॥३); स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म। बृ० उप (४।४।२५); न जायते मियते वा विपश्चित्... 'अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद् (२०१८); तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् । त० उप० (२१६); अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि । छा० उप० (६॥३॥२); स एष इह प्रविष्ट आ नखाग्नेभ्यः । बृह० (१।४।७); तत्त्वमसि (छा० उप० ६८७); अहं ब्रह्मास्मि (बृ० उप० १।४।१०); अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः। बृ० उप० (२१५-१६) ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org
Jain Education International