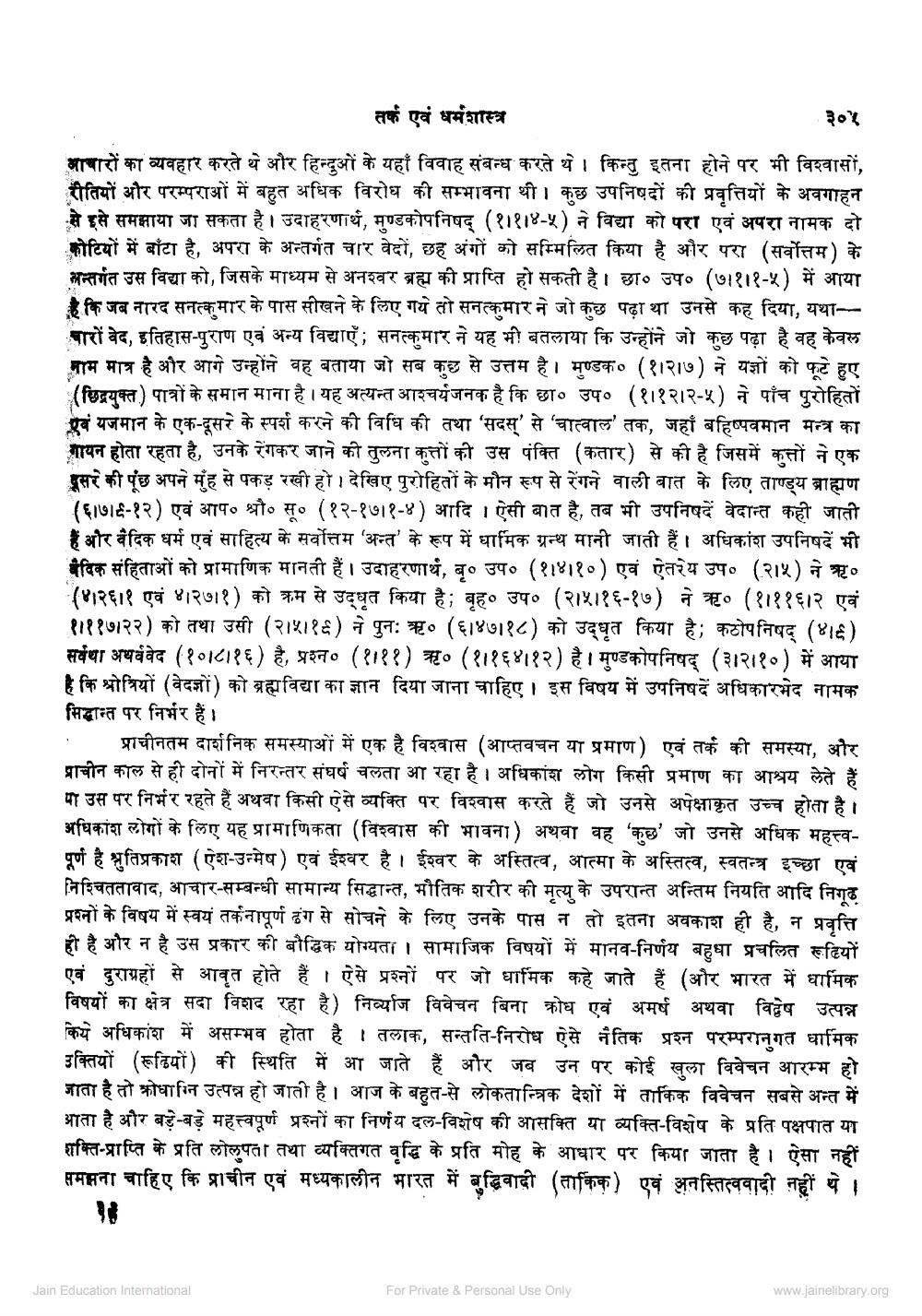________________
तर्क एवं धर्मशास्त्र
३०५ आचारों का व्यवहार करते थे और हिन्दुओं के यहाँ विवाह संबन्ध करते थे। किन्तु इतना होने पर भी विश्वासों, रीतियों और परम्पराओं में बहुत अधिक विरोध की सम्भावना थी। कुछ उपनिषदों की प्रवृत्तियों के अवगाहन से इसे समझाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, मुण्डकोपनिषद् (१।१।४-५) ने विद्या को परा एवं अपरा नामक दो कोटियों में बाँटा है, अपरा के अन्तर्गत चार वेदों, छह अंगों को सम्मिलित किया है और परा (सर्वोत्तम) के अन्तर्गत उस विद्या को, जिसके माध्यम से अनश्वर ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। छा० उप० (७।१।१-५) में आया
कि जब नारद सनत्कुमार के पास सीखने के लिए गये तो सनत्कुमार ने जो कुछ पढ़ा था उनसे कह दिया, यथा-- चारों वेद, इतिहास-पुराण एवं अन्य विद्याएँ; सनत्कुमार ने यह भी बतलाया कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा है वह केवल माम मात्र है और आगे उन्होंने वह बताया जो सब कुछ से उत्तम है। मुण्डक० (१।२।७) ने यज्ञों को फूटे हुए (छिद्रयुक्त) पात्रों के समान माना है । यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि छा० उप० (१।१२।२-५) ने पाँच पुरोहितों एवं यजमान के एक-दूसरे के स्पर्श करने की विधि की तथा सदस्' से 'चात्वाल' तक, जहाँ बहिष्पवमान मन्त्र का गायन होता रहता है, उनके रेंगकर जाने की तुलना कुत्तों की उस पंक्ति (कतार) से की है जिसमें कुत्तों ने एक दूसरे की पूंछ अपने मुंह से पकड़ रखी हो । देखिए पुरोहितों के मौन रूप से रेंगने वाली बात के लिए ताण्ड्य ब्राह्मण (६७१६-१२) एवं आप० श्रौ० सू० (१२-१७।१-४) आदि । ऐसी बात है, तब भी उपनिषदें वेदान्त कही जाती हैं और वैदिक धर्म एवं साहित्य के सर्वोत्तम 'अन्त' के रूप में धार्मिक ग्रन्थ मानी जाती हैं। अधिकांश उपनिष वैदिक संहिताओं को प्रामाणिक मानती हैं। उदाहरणार्थ, ब० उप० (१।४।१०) एवं ऐतरेय उप० (२१५) ने ऋ० (४१२६१ एवं ४।२७।१) को क्रम से उद्धत किया है; बृह० उप० (२।५।१६-१७) ने ऋ०
६.२ एवं १३११७१२२) को तथा उसी (२।५।१६) ने पुन: ऋ० (६।४७।१८) को उद्धृत किया है; कठोपनिषद् (४१६) सर्वथा अथर्ववेद (१०।८।१६) है, प्रश्न० (१।११) ऋ० (१।१६४।१२) है। मुण्डकोपनिषद् (३।२।१०) में आया है कि श्रोत्रियों (वेदज्ञों) को ब्रह्मविद्या का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इस विषय में उपनिषदें अधिकारभेद नामक सिद्धान्त पर निर्भर हैं। . प्राचीनतम दार्शनिक समस्याओं में एक है विश्वास (आप्तवचन या प्रमाण) एवं तर्क की समस्या, और प्राचीन काल से ही दोनों में निरन्तर संघर्ष चलता आ रहा है। अधिकांश लोग किसी प्रमाण का आश्रय लेते हैं या उस पर निर्भर रहते हैं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो उनसे अपेक्षाकृत उच्च होता है। अधिकांश लोगों के लिए यह प्रामाणिकता (विश्वास की भावना) अथवा वह 'कुछ' जो उनसे अधिक महत्त्वपूर्ण है श्रुतिप्रकाश (ऐश-उन्मेष) एवं ईश्वर है। ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा के अस्तित्व, स्वतन्त्र इच्छा एवं निश्चिततावाद, आचार-सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, भौतिक शरीर की मृत्यु के उपरान्त अन्तिम नियति आदि निगूढ प्रश्नों के विषय में स्वयं तर्कनापूर्ण ढंग से सोचने के लिए उनके पास न तो इतना अवकाश ही है, न प्रवृत्ति ही है और न है उस प्रकार की बौद्धिक योग्यता। सामाजिक विषयों में मानव-निर्णय बहधा प्रचलित रूढियों एवं दुराग्रहों से आवृत होते हैं । ऐसे प्रश्नों पर जो धार्मिक कहे जाते हैं (और भारत में धार्मिक विषयों का क्षेत्र सदा विशद रहा है) निर्व्याज विवेचन बिना क्रोध एवं अमर्ष अथवा विद्वेष उत्पन्न कये अधिकांश में असम्भव होता है । तलाक, सन्तति-निरोध ऐसे नैतिक प्रश्न परम्परानुगत धार्मिक उक्तियों (रूढियों) की स्थिति में आ जाते हैं और जब उन पर कोई खुला विवेचन आरम्भ हो जाता है तो क्रोधाग्नि उत्पन्न हो जाती है। आज के बहुत-से लोकतान्त्रिक देशों में तार्किक विवेचन सबसे अन्त में आता है और बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय दल-विशेष की आसक्ति या व्यक्ति-विशेष के प्रति पक्षपात या शक्ति-प्राप्ति के प्रति लोलुपता तथा व्यक्तिगत वृद्धि के प्रति मोह के आधार पर किया जाता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में बुद्धिवादी (तार्किक) एवं अनस्तित्ववादी नहीं थे ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org