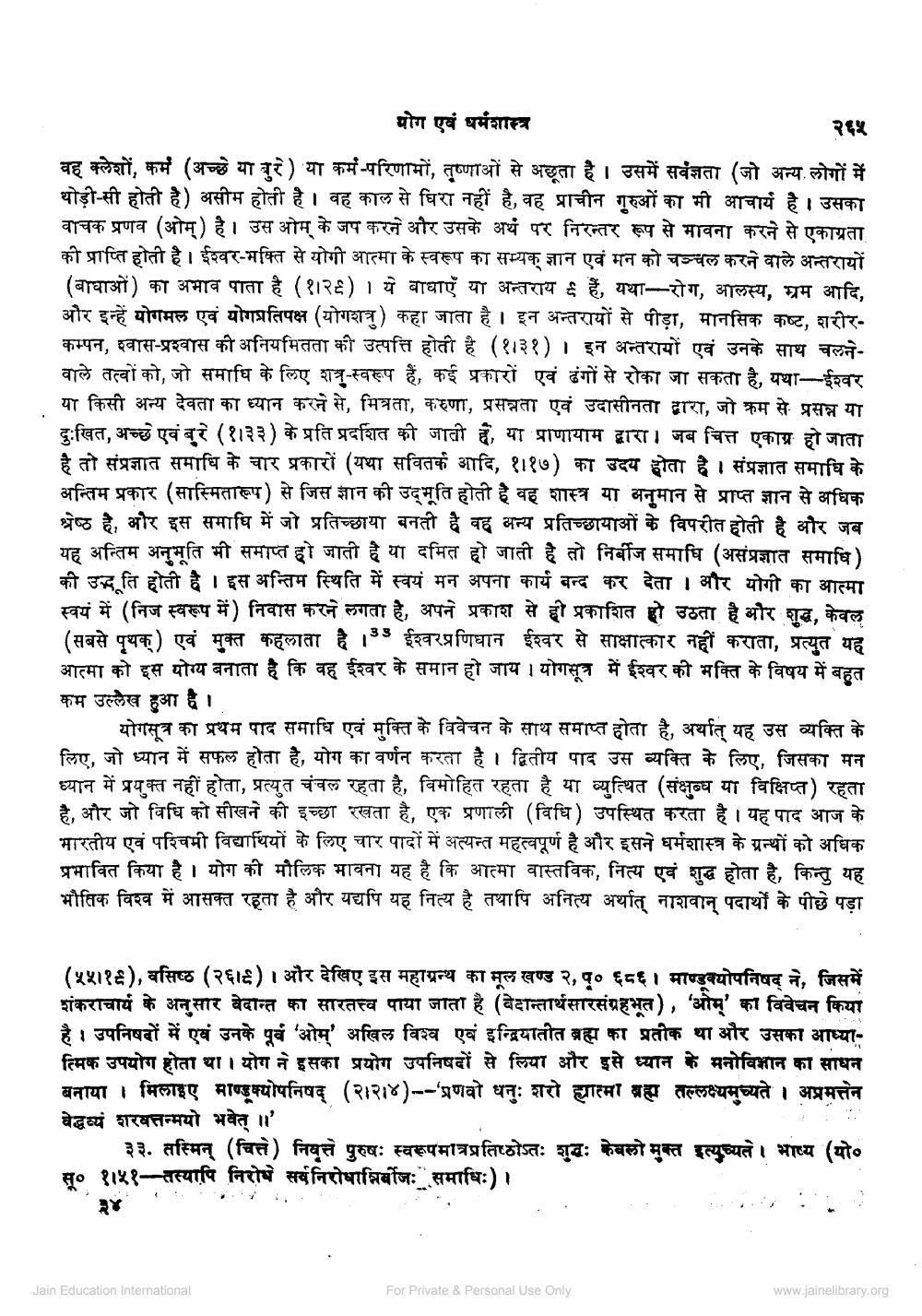________________
योग एवं धर्मशास्त्र
२६५ वह क्लेशों, कर्म (अच्छे या बुरे) या कर्म-परिणामों, तृष्णाओं से अछूता है। उसमें सर्वज्ञता (जो अन्य लोगों में थोड़ी-सी होती है) असीम होती है। वह काल से घिरा नहीं है, वह प्राचीन गुरुओं का भी आचार्य है। उसका वाचक प्रणव (ओम् ) है। उस ओम् के जप करने और उसके अर्थ पर निरन्तर रूप से मावना करने से एकाग्रता की प्राप्ति होती है। ईश्वर-भक्ति से योगी आत्मा के स्वरूप का सम्यक ज्ञान एवं मन को चञ्चल करने वाले अन्तरायों (बाधाओं) का अभाव पाता है (१।२६) । ये बाधाएँ या अन्तराय ६ हैं, यथा-रोग, आलस्य, म्रम आदि, और इन्हें योगमल एवं योगप्रतिपक्ष (योगशत्रु) कहा जाता है। इन अन्तरायों से पीड़ा, मानसिक कष्ट, शरीरकम्पन, श्वास-प्रश्वास की अनियमितता की उत्पत्ति होती है (१९३१)। इन अन्तरायों एवं उनके साथ चलनेवाले तत्वों को, जो समाधि के लिए शत्रु-स्वरूप हैं, कई प्रकारों एवं ढंगों से रोका जा सकता है, यथा-ईश्वर या किसी अन्य देवता का ध्यान करने से, मित्रता, करुणा, प्रसन्नता एवं उदासीनता द्वारा, जो क्रम से प्रसन्न या दुःखित, अच्छे एवं बुरे (१९३३) के प्रति प्रदर्शित की जाती है, या प्राणायाम द्वारा। जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो संप्रज्ञात समाधि के चार प्रकारों (यथा सवितर्क आदि, १।१७) का उदय होता है। संप्रज्ञात समाधि के अन्तिम प्रकार (सास्मितारूप) से जिस ज्ञान की उद्भूति होती है वह शास्त्र या अनुमान से प्राप्त ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है, और इस समाधि में जो प्रतिच्छाया बनती है वह अन्य प्रतिच्छायाओं के विपरीत होती है और जब यह अन्तिम अनुभूति भी समाप्त हो जाती है या दमित हो जाती है तो निर्बीज समाधि (असंप्रज्ञात समाधि) की उदति होती है । इस अन्तिम स्थिति में स्वयं मन अपना कार्य बन्द कर देता । और योगी का आत्मा स्वयं में (निज स्वरूप में) निवास करने लगता है, अपने प्रकाश से ही प्रकाशित हो उठता है और शुद्ध, केवल (सबसे पृथक) एवं मुक्त कहलाता है । ईश्वरप्रणिधान ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कराता, प्रत्युत यह आत्मा को इस योग्य बनाता है कि वह ईश्वर के समान हो जाय । योगसूत्र में ईश्वर की भक्ति के विषय में बहुत कम उल्लेख हुआ है।
योगसूत्र का प्रथम पाद समाधि एवं मुक्ति के विवेचन के साथ समाप्त होता है, अर्थात यह उस व्यक्ति के लिए, जो ध्यान में सफल होता है, योग का वर्णन करता है। द्वितीय पाद उस व्यक्ति के लिए, जिसका मन ध्यान में प्रयुक्त नहीं होता, प्रत्युत चंचल रहता है, विमोहित रहता है या व्युत्थित (संक्षुब्ध या विक्षिप्त) रहता है, और जो विधि को सीखने की इच्छा रखता है, एक प्रणाली (विधि) उपस्थित करता है । यह पाद आज के भारतीय एवं पश्चिमी विद्यार्थियों के लिए चार पादों में अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसने धर्मशास्त्र के ग्रन्थों को अधिक प्रभावित किया है। योग की मौलिक भावना यह है कि आत्मा वास्तविक, नित्य एवं शुद्ध होता है, किन्तु यह भौतिक विश्व में आसक्त रहता है और यद्यपि यह नित्य है तथापि अनित्य अर्थात् नाशवान् पदार्थों के पीछे पड़ा
(५५॥१६), वसिष्ठ (२६६) । और देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पृ० ६८६ । माण्डक्योपनिषद् ने, जिसमें शंकराचार्य के अनुसार बेदान्त का सारतत्त्व पाया जाता है (वेदान्तार्थसारसंग्रहभूत), 'ओम्' का विवेचन किया है। उपनिषदों में एवं उनके पूर्व 'ओम्' अखिल विश्व एवं इन्द्रियातीत ब्रह्म का प्रतीक था और उसका आध्यात्मिक उपयोग होता था। योग ने इसका प्रयोग उपनिषदों से लिया और इसे ध्यान के मनोविज्ञान का साधन बनाया । मिलाइए माण्डूक्योपनिषद् (२।२।४)--'प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरबत्तन्मयो भवेत् ॥'
३३. तस्मिन् (चित्ते) निवृत्ते पुरुषः स्वरूपमात्रप्रतिष्ठोऽतः शुवः केवलो मुक्त इत्युच्यते। भाष्य (यो० सू० ११५१-तस्यापि निरोधे सर्व निरोधाग्निर्योजः समाधिः)।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org