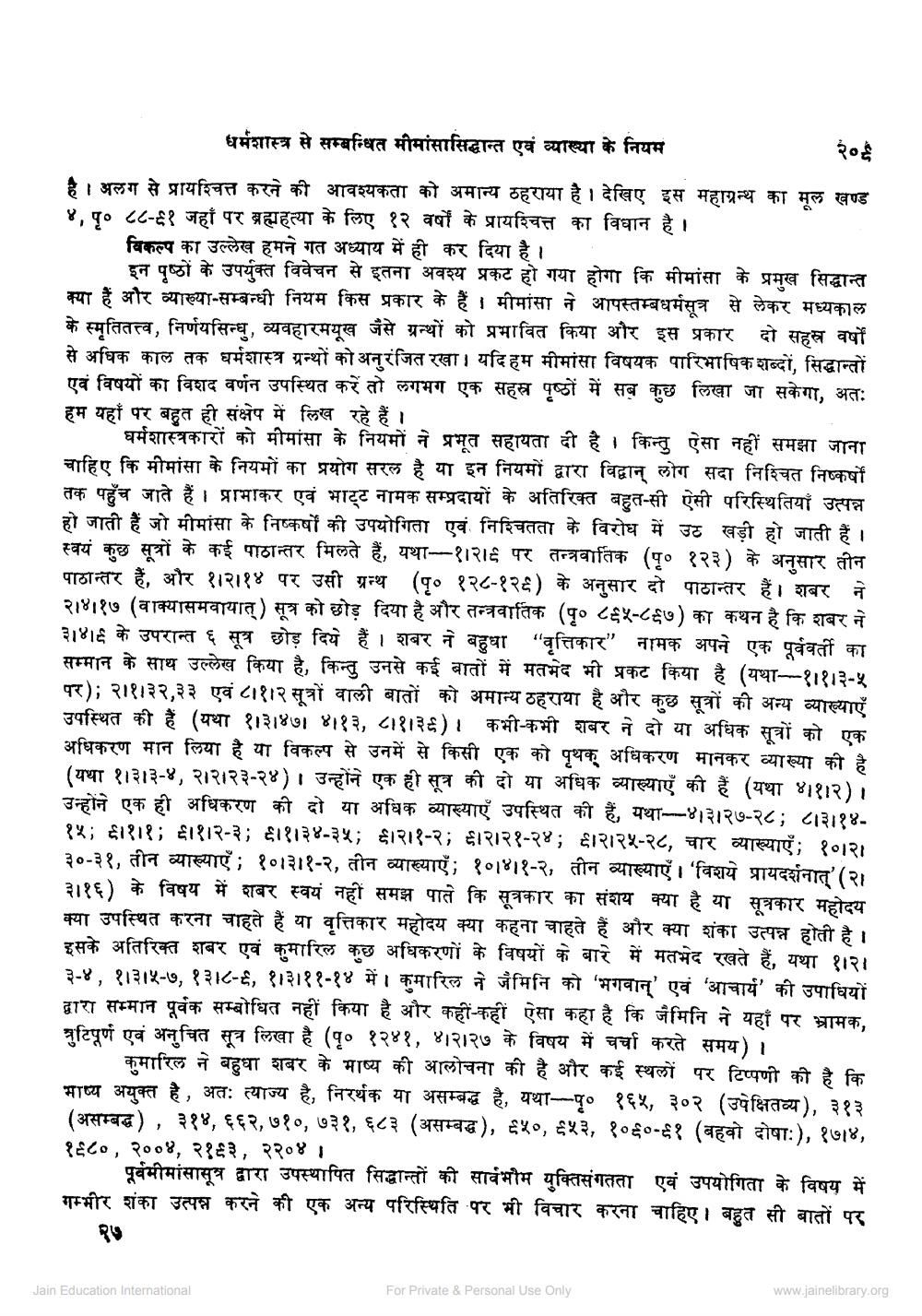________________
धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मीमांसासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम
२०६
है। अलग से प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता को अमान्य ठहराया है। देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड ४, पृ० ८८-६१ जहाँ पर ब्रह्महत्या के लिए १२ वर्षों के प्रायश्चित्त का विधान है।
विकल्प का उल्लेख हमने गत अध्याय में ही कर दिया है।
इन पष्ठों के उपर्यक्त विवेचन से इतना अवश्य प्रकट हो गया होगा कि मीमांसा के प्रमख सिद्धान्त क्या हैं और व्याख्या-सम्बन्धी नियम किस प्रकार के हैं। मीमांसा ने आपस्तम्बधर्मसत्र से लेकर मध्यकाल के स्मृतितत्त्व, निर्णयसिन्धु, व्यवहारमयूख जैसे ग्रन्थों को प्रभावित किया और इस प्रकार दो सहस्र वर्षों से अधिक काल तक धर्मशास्त्र ग्रन्थों को अनरंजित रखा। यदि हम मीमांसा विषयक पारिभाषिक शब्दों, सिद्धान्तों एवं विषयों का विशद वर्णन उपस्थित करें तो लगभग एक सहस्र पृष्ठों में सब कुछ लिखा जा सकेगा, अतः हम यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में लिख रहे हैं।
धर्मशास्त्रकारों को मीमांसा के नियमों ने प्रभूत सहायता दी है। किन्तु ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि मीमांसा के नियमों का प्रयोग सरल है या इन नियमों द्वारा विद्वान् लोग सदा निश्चित निष्कर्षों तक पहुंच जाते हैं। प्राभाकर एवं भाट्ट नामक सम्प्रदायों के अतिरिक्त बहुत-सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो मीमांसा के निष्कर्षों की उपयोगिता एवं निश्चितता के विरोध में उठ खड़ी हो जाती हैं। स्वयं कुछ सूत्रों के कई पाठान्तर मिलते हैं, यथा-१।२।६ पर तन्त्रवातिक (पृ० १२३) के पाठान्तर हैं, और ११२।१४ पर उसी ग्रन्थ (पृ० १२८-१२६) के अनुसार दो पाठान्तर हैं। शबर ने २१४११७ (वाक्यासमवायात) सत्र को छोड़ दिया है और तन्त्रवार्तिक (१० ८६५-८६७) का कथन है कि शबर ने ३१४ के उपरान्त ६ सत्र छोड दिये हैं। शबर ने बहधा "वत्तिकार" नामक अपने एक पूर्ववर्ती का सम्मान के साथ उल्लेख किया है, किन्तु उनसे कई बातों में मतभेद भी प्रकट किया है (यथा-११।३-५ पर); २।१।३२,३३ एवं ८।१।२ सूत्रों वाली बातों को अमान्य ठहराया है और कुछ सूत्रों की अन्य व्याख्याएँ उपस्थित की हैं (यथा ११३१४७। ४।१३, ८११।३६)। कभी-कभी शबर ने दो या अधिक सूत्रों को एक अधिकरण मान लिया है या विकल्प से उनमें से किसी एक को पृथक् अधिकरण मानकर व्याख्या की है (यथा १०३१३-४, २।२।२३-२४)। उन्होंने एक ही सूत्र की दो या अधिक व्याख्याएँ की हैं (यथा ४११०२)। उन्होंने एक ही अधिकरण की दो या अधिक व्याख्याएँ उपस्थित की हैं, यथा-४।३।२७-२८: ८३४१४. १५; ६।११; ६।२-३; ६।१।३४-३५; ६२।१-२, ६।२।२१-२४, ६।२५-२८, चार व्याख्याएँ; १०॥२॥ ३०-३१, तीन व्याख्याएँ; १०३।१-२, तीन व्याख्याएँ; १०।४।१-२, तीन व्याख्याएँ। 'विशये प्रायदर्शनात' (२॥ ३।१६) के विषय में शबर स्वयं नहीं समझ पाते कि सूत्रकार का संशय क्या है या सूत्रकार महोदय क्या उपस्थित करना चाहते हैं या वृत्तिकार महोदय क्या कहना चाहते हैं और क्या शंका उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त शबर एवं कुमारिल कुछ अधिकरणों के विषयों के बारे में मतभद रखते हैं, यथा श२। ३-४, १३१५-७, १३१८-६, १।३।११-१४ में। कुमारिल ने जैमिनि को 'भगवान्' एवं 'आचार्य' की उपाधियों द्वारा सम्मान पूर्वक सम्बोधित नहीं किया है और कहीं-कहीं ऐसा कहा है कि जैमिनि ने यहाँ पर भ्रामक त्रुटिपूर्ण एवं अनुचित सूत्र लिखा है (पृ० १२४१, ४।२।२७ के विषय में चर्चा करते स
कुमारिल ने बहुधा शबर के भाष्य की आलोचना की है और कई स्थलों पर टिप्पणी की है कि भाष्य अयुक्त है , अत: त्याज्य है, निरर्थक या असम्बद्ध है, यथा-पृ० १६५, ३०२ (उपेक्षितव्य), ३१३ (असम्बद्ध), ३१४, ६६२, ७१०, ७३१, ६८३ (असम्बद्ध), ६५०, ६५३, १०६०-६१ (बहवो दोषाः), १७।४, १६८०, २००४, २१६३, २२०४ ।
पूर्वमीमांसासूत्र द्वारा उपस्थापित सिद्धान्तों को सार्वभौम युक्तिसंगतता एवं उपयोगिता के विषय में गम्भीर शंका उत्पन्न करने की एक अन्य परिस्थिति पर भी विचार करना चाहिए। बहुत सी बातों पर
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org