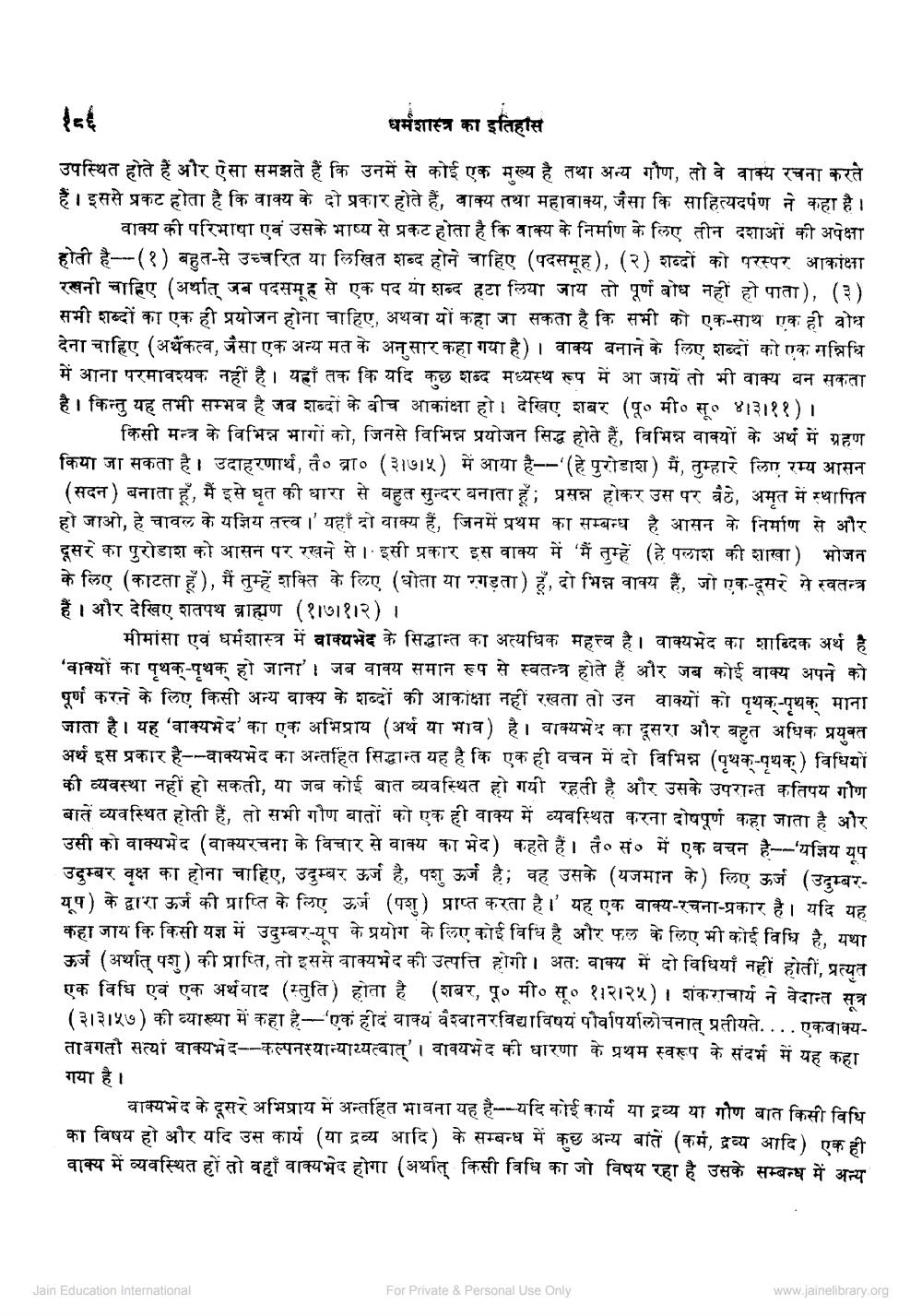________________
धर्मशास्त्र का इतिहास उपस्थित होते हैं और ऐसा समझते हैं कि उनमें से कोई एक मुख्य है तथा अन्य गौण, तो वे वाक्य रचना करते हैं। इससे प्रकट होता है कि वाक्य के दो प्रकार होते हैं, वाक्य तथा महावाक्य, जैसा कि साहित्यदर्पण ने कहा है।
वाक्य की परिभाषा एवं उसके भाष्य से प्रकट होता है कि वाक्य के निर्माण के लिए तीन दशाओं की अपेक्षा होती है---(१) बहुत-से उच्चरित या लिखित शब्द होने चाहिए (पदसमूह), (२) शब्दों को परस्पर आकांक्षा रखनी चाहिए (अर्थात जब पदसमूह से एक पद या शब्द हटा लिया जाय तो पूर्ण बोध नहीं हो पाता), (३) सभी शब्दों का एक ही प्रयोजन होना चाहिए, अथवा यों कहा जा सकता है कि सभी को एक-साथ एक ही बोध देना चाहिए (अर्थंकत्व, जैसा एक अन्य मत के अनुसार कहा गया है)। वाक्य बनाने के लिए शब्दों को एक सन्निधि में आना परमावश्यक नहीं है। यहाँ तक कि यदि कुछ शब्द मध्यस्थ रूप में आ जायें तो भी वाक्य बन सकता है। किन्तु यह तभी सम्भव है जब शब्दों के बीच आकांक्षा हो। देखिए शबर (पू० मी० सू० ४।३।११)।
किसी मन्त्र के विभिन्न भागों को, जिनसे विभिन्न प्रयोजन सिद्ध होते हैं, विभिन्न वाक्यों के अर्थ में ग्रहण किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, तै० ब्रा० (३१७१५) में आया है--(हे पुरोडाश) मैं, तुम्हारे लिए रम्य आसन (सदन) बनाता हूँ, मैं इसे घृत की धारा से बहुत सुन्दर बनाता हूँ; प्रसन्न होकर उस पर बैठे, अमृत में स्थापित हो जाओ, हे चावल के यज्ञिय तत्त्व।' यहाँ दो वाक्य हैं, जिनमें प्रथम का सम्बन्ध है आसन के निर्माण से और दूसरे का पुरोडाश को आसन पर रखने से। इसी प्रकार इस वाक्य में 'मैं तुम्हें (हे पलाश की शाखा) भोजन के लिए (काटता हूँ), मैं तुम्हें शक्ति के लिए (धोता या रगड़ता) हूँ, दो भिन्न वाक्य हैं, जो एक-दूसरे से स्वतन्त्र हैं। और देखिए शतपथ ब्राह्मण (११७।१।२) ।
मीमांसा एवं धर्मशास्त्र में वाक्यभेद के सिद्धान्त का अत्यधिक महत्त्व है। वाक्यभेद का शाब्दिक अर्थ है 'वाक्यों का पृथक्-पृथक् हो जाना'। जब वाक्य समान रूप से स्वतन्त्र होते हैं और जब कोई वाक्य अपने को पूर्ण करने के लिए किसी अन्य वाक्य के शब्दों की आकांक्षा नहीं रखता तो उन वाक्यों को पृथक्-पृथक् माना जाता है। यह 'वाक्यभेद' का एक अभिप्राय (अर्थ या भाव) है। वाक्यभेद का दूसरा और बहुत अधिक प्रयुक्त अर्थ इस प्रकार है--वाक्यभेद का अन्तहित सिद्धान्त यह है कि एक ही वचन में दो विभिन्न (पृथक्-पृथक् ) विधियों की व्यवस्था नहीं हो सकती, या जब कोई बात व्यवस्थित हो गयी रहती है और उसके उपरान्त कतिपय गौण बातें व्यवस्थित होती हैं, तो सभी गौण बातों को एक ही वाक्य में व्यवस्थित करना दोषपूर्ण कहा जाता है और उसी को वाक्यभेद (वाक्यरचना के विचार से वाक्य का भेद) कहते हैं। तै० सं० में एक वचन है--'यज्ञिय यप उदुम्बर वृक्ष का होना चाहिए, उदुम्बर ऊर्ज है, पशु ऊर्ज है; वह उसके (यजमान के लिए ऊर्ज (उदुम्बरयूप) के द्वारा ऊर्ज की प्राप्ति के लिए ऊर्ज (पशु) प्राप्त करता है।' यह एक वाक्य-रचना-प्रकार है। यदि यह कहा जाय कि किसी यज्ञ में उदुम्बर-यूप के प्रयोग के लिए कोई विधि है और फल के लिए भी कोई विधि है, यथा ऊर्ज (अर्थात् पशु) की प्राप्ति, तो इससे वाक्यभेद की उत्पत्ति होगी। अत: वाक्य में दो विधियाँ नहीं होती, प्रत्यत एक विधि एवं एक अर्थवाद (स्तुति) होता है (शबर, पू० मी० सू० ११२।२५)। शंकराचार्य ने वेदान्त सत्र (३१३१५७) की व्याख्या में कहा है-'एक हीदं वाक्यं वैश्वानरविद्याविषयं पौषिर्यालोचनात प्रतीयते....एकवाक्य. तावगतौ सत्यां वाक्यभेद--कल्पनस्यान्याय्यत्वात्। वाक्यभेद की धारणा के प्रथम स्वरूप के संदर्भ में यह कहा गया है।
वाक्यभेद के दूसरे अभिप्राय में अन्तहित भावना यह है---यदि कोई कार्य या द्रव्य या गौण बात किसी विधि का विषय हो और यदि उस कार्य (या द्रव्य आदि) के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें (कर्म, द्रव्य आदि) एक ही वाक्य में व्यवस्थित हों तो वहाँ वाक्यभेद होगा (अर्थात् किसी विधि का जो विषय रहा है उसके सम्बन्ध में अन्य
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org