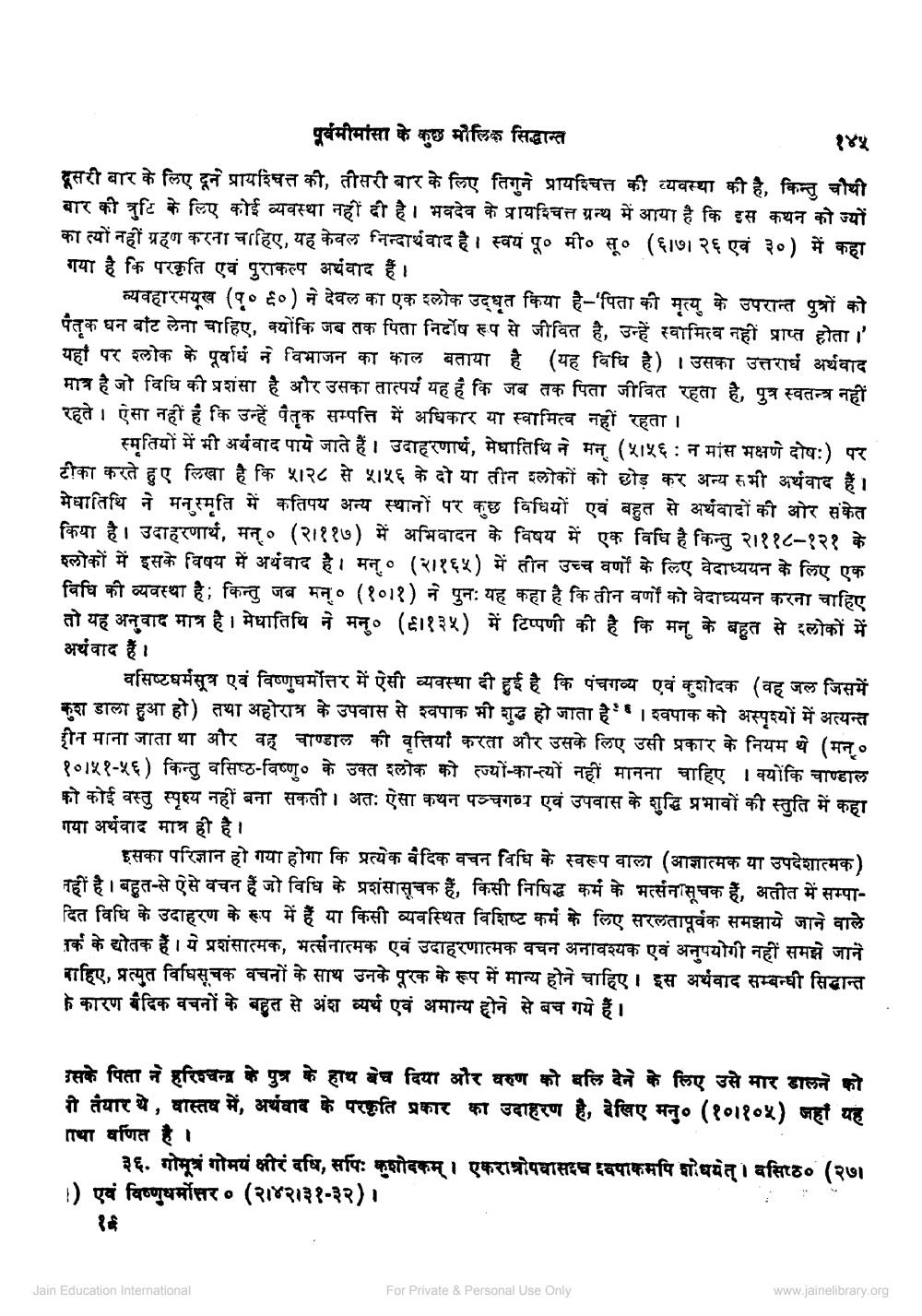________________
पूर्वमीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त
१४५ दूसरी बार के लिए दूने प्रायश्चित्त की, तीसरी बार के लिए तिगुने प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है, किन्तु चौथी बार की त्रुटि के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी है। भवदेव के प्रायश्चित्त ग्रन्थ में आया है कि इस कथन को ज्यों का त्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए, यह केवल निन्दार्थवाद है। स्वयं पू० मी० सू० (६।७। २६ एवं ३०) में कहा गया है कि परकृति एवं पुराकल्प अर्थवाद हैं।
व्यवहारमयूख (१०६०) ने देवल का एक श्लोक उद्धृत किया है-'पिता की मृत्यु के उपरान्त पुत्रों को पैतृक धन बाँट लेना चाहिए, क्योंकि जब तक पिता निर्दोष रूप से जीवित है, उन्हें स्वामित्व नहीं प्राप्त होता।' यहाँ पर श्लोक के पूर्वाधं ने विभाजन का काल बताया है (यह विधि है) । उसका उत्तरार्घ अर्थवाद मात्र है जो विधि की प्रशंसा है और उसका तात्पर्य यह है कि जब तक पिता जीवित रहता है, पुत्र स्वतन्त्र नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि उन्हें पैतृक सम्पत्ति में अधिकार या स्वामित्व नहीं रहता।
स्मृतियों में भी अर्थवाद पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, मेधातिथि ने मन् (५१५६ : न मांस भक्षणे दोषः) पर टीका करते हुए लिखा है कि ५।२८ से १५६ के दो या तीन इलोकों को छोड़ कर अन्य सभी अर्थवाद हैं। मेधातिथि ने मनुस्मृति में कतिपय अन्य स्थानों पर कुछ विधियों एवं बहुत से अर्थवादों की ओर संकेत किया है। उदाहरणार्थ, मन्० (२।११७) में अभिवादन के विषय में एक विधि है किन्तु २०११८-१२१ के श्लोकों में इसके विषय में अर्थवाद है। मन ० (२।१६५) में तीन उच्च वर्गों के लिए वेदाध्ययन के लिए एक विधि की व्यवस्था है; किन्तु जब मन् ० (१०११) ने पुन: यह कहा है कि तीन वर्णों को वेदाध्ययन करना चाहिए तो यह अनुवाद मात्र है। मेधातिथि ने मनु० (६।१३५) में टिप्पणी की है कि मनु के बहुत से दलोकों में अर्थवाद हैं।
वसिष्टधर्मसूत्र एवं विष्णुधर्मोत्तर में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि पंचगव्य एवं कुशोदक (वह जल जिसमें कुश डाला हुआ हो) तथा अहोरात्र के उपवास से श्वपाक भी शुद्ध हो जाता है । श्वपाक को अस्पृश्यों में अत्यन्त हीन माना जाता था और वह चाण्डाल की वृत्तियां करता और उसके लिए उसी प्रकार के नियम थे (मन । १०५१-५६) किन्तु वसिष्ठ-विष्णु० के उक्त श्लोक को ज्यों-का-त्यों नहीं मानना चाहिए । क्योंकि चाण्डाल को कोई वस्तु स्पृश्य नहीं बना सकती। अत: ऐसा कथन पञ्चगव्य एवं उपवास के शुद्धि प्रभावों की स्तुति में कहा गया अर्थवाद मात्र ही है।
इसका परिज्ञान हो गया होगा कि प्रत्येक वैदिक वचन विधि के स्वरूप वाला (आज्ञात्मक या उपदेशात्मक) नहीं है। बहुत-से ऐसे वचन हैं जो विधि के प्रशंसासूचक हैं, किसी निषिद्ध कर्म के भर्त्सनासूचक हैं, अतीत में सम्पादित विधि के उदाहरण के रूप में हैं या किसी व्यवस्थित विशिष्ट कर्म के लिए सरलतापूर्वक समझाये जाने वाले तर्क के द्योतक हैं। ये प्रशंसात्मक, भर्त्सनात्मक एवं उदाहरणात्मक वचन अनावश्यक एवं अनुपयोगी नहीं समझे जाने वाहिए, प्रत्युत विधिसूचक वचनों के साथ उनके पूरक के रूप में मान्य होने चाहिए। इस अर्थवाद सम्बन्धी सिद्धान्त के कारण बैदिक वचनों के बहुत से अंश व्यर्थ एवं अमान्य होने से बच गये हैं।
उसके पिता ने हरिश्चन्द्र के पुत्र के हाथ बेच दिया और वरुण को बलि देने के लिए उसे मार डालने को गो तैयार थे , वास्तव में, अर्थवाद के परकृति प्रकार का उदाहरण है, देखिए मनु० (१०।१०५) जहाँ यह था वणित है।
३६. गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दषि, सपिः कुशोदकम् । एकरात्रोपवासच वपाकमपि शोधयेत् । वसिष्ठ० (२७॥ 1) एवं विष्णुधर्मोत्तर ० (२२४२२३१-३२)।
For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org