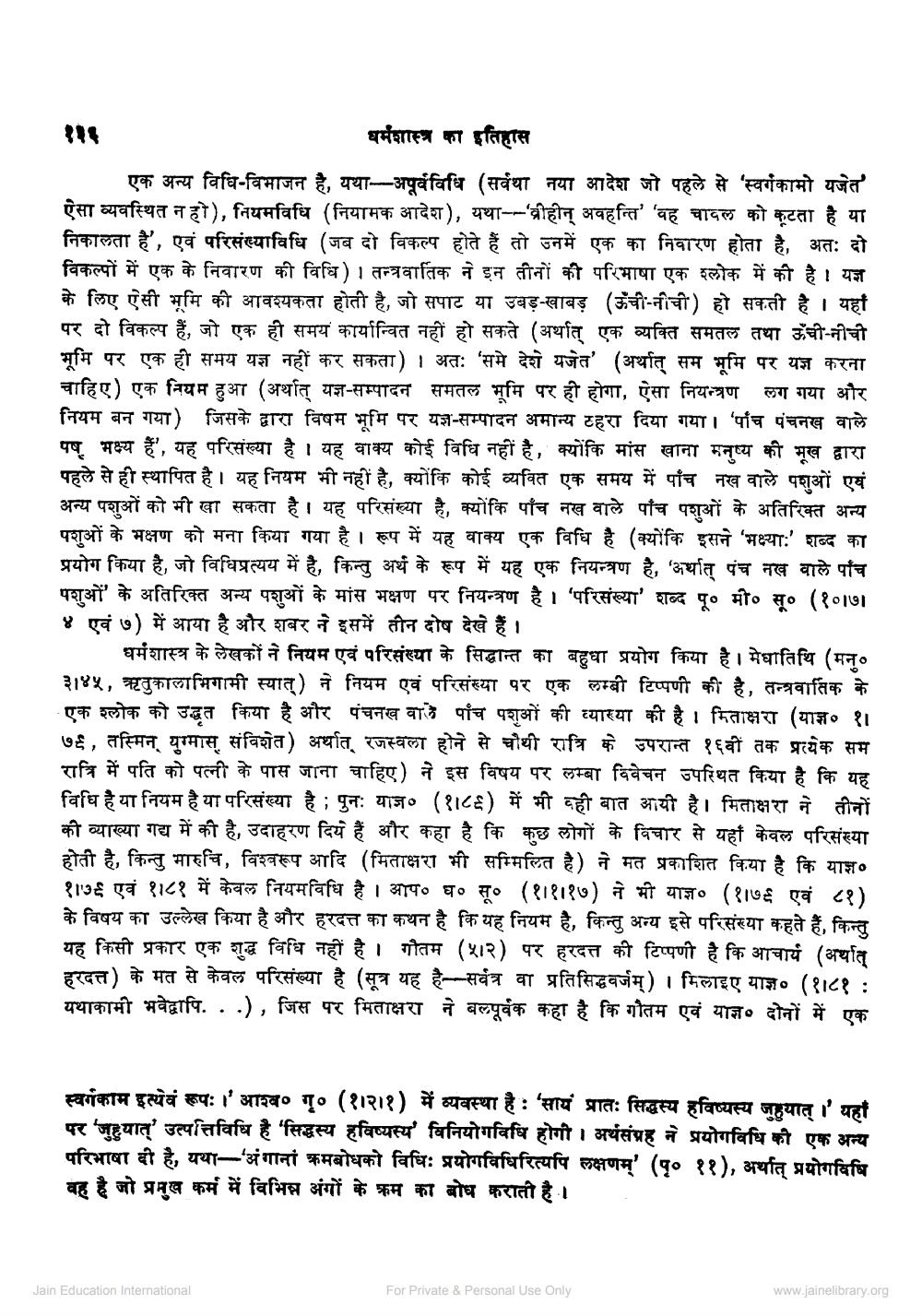________________
धर्मशास्त्र का इतिहास
एक अन्य विधि-विभाजन है, यथा-- अपूर्वविधि ( सर्वथा नया आदेश जो पहले से 'स्वर्गकामो यजेत ऐसा व्यवस्थित न हो), नियमविधि ( नियामक आदेश ), यथा-- ' व्रीहीन् अवहन्ति' 'वह चावल को कूटता है या निकालता है, एवं परिसंख्याविधि ( जब दो विकल्प होते हैं तो उनमें एक का निवारण होता है, अतः दो विकल्पों में एक के निवारण की विधि ) । तन्त्रवार्तिक ने इन तीनों की परिभाषा एक श्लोक में की है । यज्ञ के लिए ऐसी भूमि की आवश्यकता होती है, जो सपाट या उबड़-खाबड़ ( ऊँची-नीची ) हो सकती है । यहाँ पर दो विकल्प हैं, जो एक ही समय कार्यान्वित नहीं हो सकते ( अर्थात् एक व्यक्ति समतल तथा ऊँची-नीची भूमि पर एक ही समय यज्ञ नहीं कर सकता ) । अतः 'समे देशे यजेत' (अर्थात् सम भूमि पर यज्ञ करना चाहिए ) एक नियम हुआ (अर्थात् यज्ञ - सम्पादन समतल भूमि पर ही होगा, ऐसा नियन्त्रण लग गया और नियम बन गया ) जिसके द्वारा विषम भूमि पर यज्ञ-सम्पादन अमान्य ठहरा दिया गया। 'पाँच पंचनख वाले पष् मक्ष्य हैं, यह परिसंख्या है । यह वाक्य कोई विधि नहीं है, क्योंकि मांस खाना मनुष्य की भूख द्वारा पहले से ही स्थापित है । यह नियम भी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक समय में पाँच नख वाले पशुओं एवं अन्य पशुओं को भी खा सकता है। यह परिसंख्या है, क्योंकि पाँच नख वाले पाँच पशुओं के अतिरिक्त अन्य पशुओं के भक्षण को मना किया गया है । रूप में यह वाक्य एक विधि है ( क्योंकि इसने 'भक्ष्याः' शब्द का प्रयोग किया है, जो विधिप्रत्यय में है, किन्तु अर्थ के रूप में यह एक नियन्त्रण है, 'अर्थात् पंच नख वाले पाँच पशुओं के अतिरिक्त अन्य पशुओं के मांस भक्षण पर नियन्त्रण है । 'परिसंख्या' शब्द पू० मी० सू० (१०|७| ४ एवं ७ ) में आया है और शबर ने इसमें तीन दोष देखे हैं ।
७६,
धर्मशास्त्र के लेखकों ने नियम एवं परिसंख्या के सिद्धान्त का बहुधा प्रयोग किया है । मेधातिथि ( मनु० ३।४५, ऋतुकालाभिगामी स्यात् ) ने नियम एवं परिसंख्या पर एक लम्बी टिप्पणी की है, तन्त्रवार्तिक के एक श्लोक को उद्धृत किया है और पंचनख वाले पांच पशुओं की व्याख्या की है । मिताक्षरा ( याज्ञ० १| तस्मिन् युग्मास् संविशेत) अर्थात् रजस्वला होने से चौथी रात्रि के उपरान्त १६वीं तक प्रत्येक सम रात्रि में पति को पत्नी के पास जाना चाहिए) ने इस विषय पर लम्बा विवेचन उपस्थित किया है कि यह विधि है या नियम है या परिसंख्या है ; पुनः याज० ( ११८६ ) में भी वही बात आयी है । मिताक्षरा ने तीनों की व्याख्या गद्य में की है, उदाहरण दिये हैं और कहा है कि कुछ लोगों के विचार से यहाँ केवल परिसंख्या होती है, किन्तु मारुचि, विश्वरूप आदि ( मिताक्षरा भी सम्मिलित है ) ने मत प्रकाशित किया है कि याज्ञ० १।७६ एवं १।८१ में केवल नियमविधि है । आप० घ० सू० ( १ । १ । १७) ने भी याज्ञ० ( १७६ एवं ८१ ) के विषय का उल्लेख किया है और हरदत्त का कथन है कि यह नियम है, किन्तु अन्य इसे परिसंख्या कहते हैं, किन्तु यह किसी प्रकार एक शुद्ध विधि नहीं है । गौतम ( ५२ ) पर हरदत्त की टिप्पणी है कि आचार्य (अर्थात् हरदत्त) के मत से केवल परिसंख्या है ( सूत्र यह है -- सर्वत्र वा प्रतिसिद्धवर्जम् ) । मिलाइए याज्ञ० ( १।८१ : यथाकामी भवेद्वापि ), जिस पर मिताक्षरा ने बलपूर्वक कहा है कि गौतम एवं याज्ञ० दोनों में एक
११६
स्वर्गकाम इत्येवं रूपः ।' आश्व० गृ० (१।२।१ ) में व्यवस्था है : 'सायं प्रातः सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयात् ।' यहाँ पर 'जुहुयात्' उत्पत्तिविधि है 'सिद्धस्य हविष्यस्य विनियोगविधि होगी । अर्थसंग्रह ने प्रयोगविधि की एक अन्य परिभाषा दी है, यथा- 'अंगानां क्रमबोधको विधि प्रयोगविधिरित्यपि लक्षणम्' ( पृ० ११), अर्थात् प्रयोगविधि वह है जो प्रमुख कर्म में विभिन्न अंगों के क्रम का बोध कराती है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org