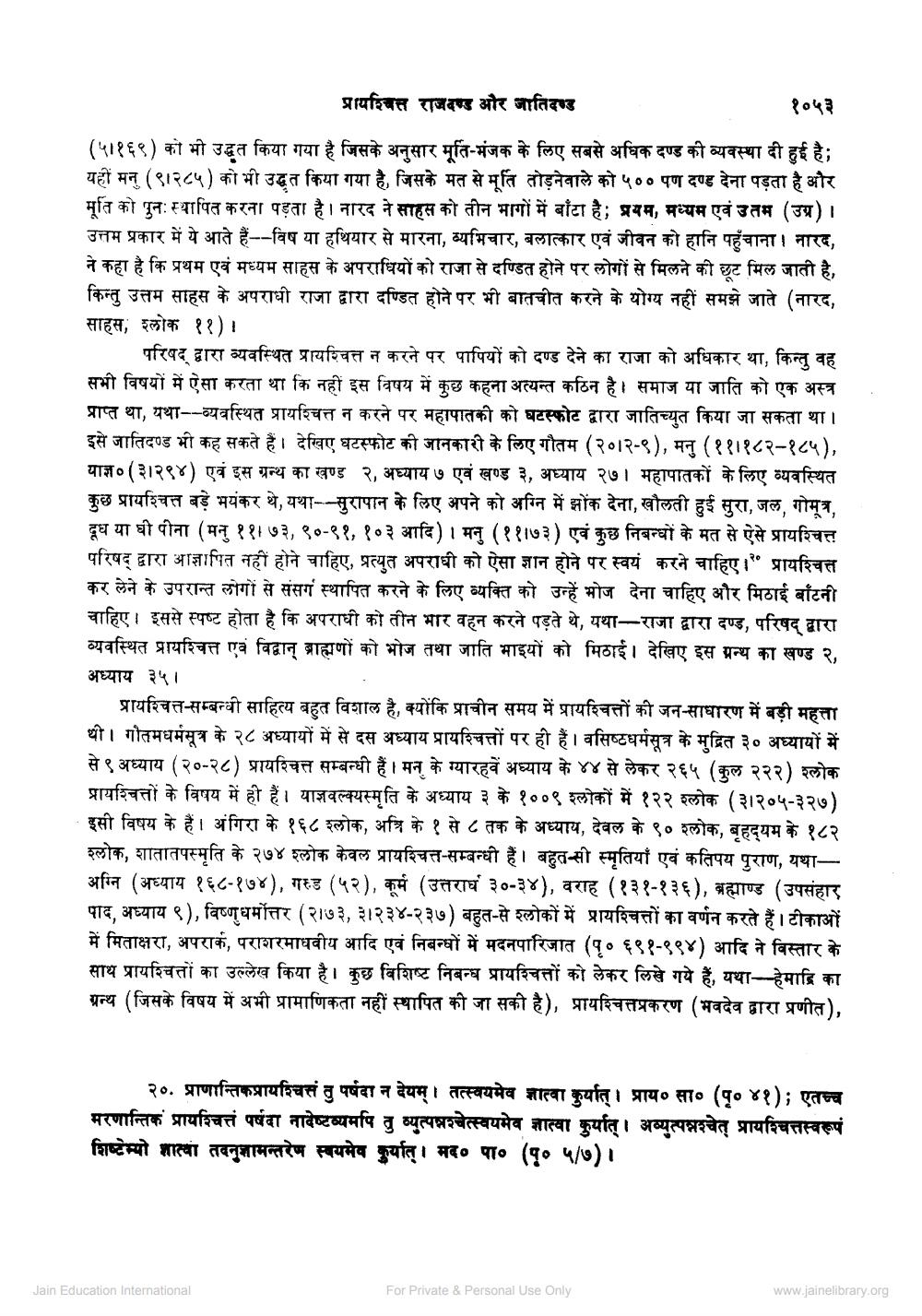________________
प्रायश्चित्त राजदण्ड और जातिदण्ड
१०५३
(५।१६९) को भी उद्धृत किया गया है जिसके अनुसार मूर्ति मंजक के लिए सबसे अधिक दण्ड की व्यवस्था दी हुई है; यहीं मनु (९।२८५) को भी उद्धृत किया गया है, जिसके मत से मूर्ति तोड़नेवाले को ५०० पण दण्ड देना पड़ता है और मूर्ति को पुनः स्थापित करना पड़ता है। नारद ने साहस को तीन भागों में बाँटा है; प्रथम, मध्यम एवं उतम ( उग्र ) । उत्तम प्रकार में ये आते हैं--विष या हथियार से मारना, व्यभिचार, बलात्कार एवं जीवन को हानि पहुँचाना। नारद, ने कहा है कि प्रथम एवं मध्यम साहस के अपराधियों को राजा से दण्डित होने पर लोगों से मिलने की छूट मिल जाती है, किन्तु उत्तम साहस के अपराधी राजा द्वारा दण्डित होने पर भी बातचीत करने के योग्य नहीं समझे जाते (नारद, साहस, श्लोक ११ ) ।
परिषद् द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर पापियों को दण्ड देने का राजा को अधिकार था, किन्तु वह सभी विषयों में ऐसा करता था कि नहीं इस विषय में कुछ कहना अत्यन्त कठिन है। समाज या जाति को एक अस्त्र प्राप्त था, यथा-- व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर महापातकी को घटस्फोट द्वारा जातिच्युत किया जा सकता था । इसे जातिदण्ड भी कह सकते हैं। देखिए घटस्फोट की जानकारी के लिए गौतम (२०१२-९), मनु ( ११।१८२ - १८५ ), याज्ञ० (३।२९४) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड २ अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय २७ । महापातकों के लिए व्यवस्थित कुछ प्रायश्चित बड़े भयंकर थे, यथा--सुरापान के लिए अपने को अग्नि में झोंक देना, खौलती हुई सुरा, जल, गोमूत्र, दूध या घी पीना (मनु ११।७३, ९०-९१, १०३ आदि) । मनु (११।७३ ) एवं कुछ निबन्धों के मत से ऐसे प्रायश्चित्त परिषद् द्वारा आज्ञापित नहीं होने चाहिए, प्रत्युत अपराधी को ऐसा ज्ञान होने पर स्वयं करने चाहिए।" प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त लोगों से संसर्ग स्थापित करने के लिए व्यक्ति को उन्हें भोज देना चाहिए और मिठाई बांटनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अपराधी को तीन भार वहन करने पड़ते थे, यथा-राजा द्वारा दण्ड, परिषद् द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्त एवं विद्वान् ब्राह्मणों को भोज तथा जाति भाइयों को मिठाई । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २,
अध्याय ३५ ।
प्रायश्चित्त-सम्बन्धी साहित्य बहुत विशाल है, क्योंकि प्राचीन समय में प्रायश्चित्तों की जन साधारण में बड़ी महत्ता थी । गौतमधर्मसूत्र के २८ अध्यायों में से दस अध्याय प्रायश्चित्तों पर ही हैं । वसिष्ठधर्मसूत्र के मुद्रित ३० अध्यायों में से ९ अध्याय (२०-२८) प्रायश्चित्त सम्बन्धी हैं। मन के ग्यारहवें अध्याय के ४४ से लेकर २६५ ( कुल २२२) श्लोक प्रायश्चित्तों के विषय में ही हैं । याज्ञवल्क्यस्मृति के अध्याय ३ के १००९ श्लोकों में १२२ श्लोक ( ३।२०५-३२७) इसी विषय के हैं । अंगिरा के १६८ श्लोक, अत्रि के १ से ८ तक के अध्याय, देवल के ९० श्लोक, बृहद्यम के १८२ श्लोक, शातातपस्मृति के २७४ श्लोक केवल प्रायश्चित्त-सम्बन्धी हैं। बहुत-सी स्मृतियाँ एवं कतिपय पुराण, यथाअग्नि (अध्याय १६८ - १७४), गरुड (५२), कूर्म ( उत्तरार्ध ३०-३४), वराह (१३१-१३६), ब्रह्माण्ड ( उपसंहार पाद, अध्याय ९), विष्णुधर्मोत्तर (२।७३, ३।२३४-२३७) बहुत से श्लोकों में प्रायश्चित्तों का वर्णन करते हैं। टीकाओं में मिताक्षरा, अपरार्क, पराशरमाधवीय आदि एवं निबन्धों में मदनपारिजात ( पृ० ६९१-९९४) आदि ने विस्तार के साथ प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया है। कुछ विशिष्ट निबन्ध प्रायश्चित्तों को लेकर लिखे गये हैं, यथा-हेमाद्रि का ग्रन्थ (जिसके विषय में अभी प्रामाणिकता नहीं स्थापित की जा सकी है), प्रायश्चित्तप्रकरण ( भवदेव द्वारा प्रणीत),
२०. प्राणान्तिकप्रायश्चित्तं तु पर्षदा न देयम् । तत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात् । प्राय० सा० ( पृ० ४१ ) ; एतच्च मरणान्तिकं प्रायश्चित्तं पर्षदा नावेष्टव्यमपि तु व्युत्पन्नश्चेत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात् । अव्युत्पन्नश्चेत् प्रायश्चित्तस्वरूपं शिष्टम्पो ज्ञात्वा तवनुज्ञामन्तरेण स्वयमेव कुर्यात् । मद० पा० ( पु० ५ / ७) ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org