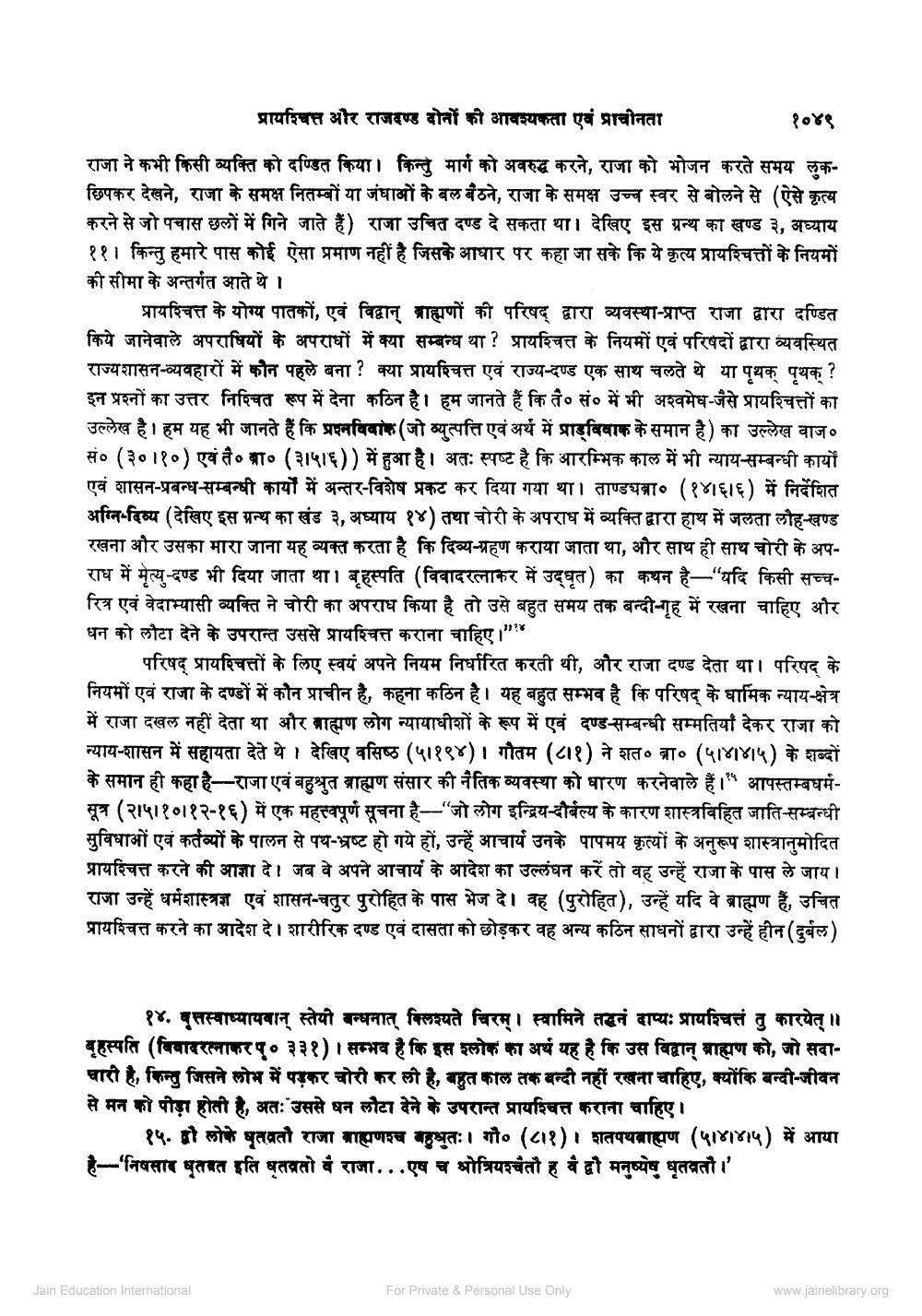________________
प्रायश्चित्त और राजदण्ड दोनों को आवश्यकता एवं प्राचीनता
१०४९
राजा ने कभी किसी व्यक्ति को दण्डित किया। किन्तु मार्ग को अवरुद्ध करने, राजा को भोजन करते समय लुकछिपकर देखने, राजा के समक्ष नितम्बों या जंघाओं के बल बैठने, राजा के समक्ष उच्च स्वर से बोलने से (ऐसे कृत्य करने से जो पचास छलों में गिने जाते हैं) राजा उचित दण्ड दे सकता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ११। किन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये कृत्य प्रायश्चित्तों के नियमों की सीमा के अन्तर्गत आते थे।
प्रायश्चित्त के योग्य पातकों, एवं विद्वान् ब्राह्मणों की परिषद् द्वारा व्यवस्था प्राप्त राजा द्वारा दण्डित किये जानेवाले अपराधियों के अपराधों में क्या सम्बन्ध था? प्रायश्चित्त के नियमों एवं परिषदों द्वारा व्यवस्थित राज्यशासन-व्यवहारों में कौन पहले बना? क्या प्रायश्चित्त एवं राज्य-दण्ड एक साथ चलते थे या पृथक् पृथक् ? इन प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप में देना कठिन है। हम जानते हैं कि तै० सं० में भी अश्वमेध-जैसे प्रायश्चित्तों का उल्लेख है। हम यह भी जानते हैं कि प्रश्नविवाक (जो व्युत्पत्ति एवं अर्थ में प्राविवाक के समान है) का उल्लेख वाज. सं० (३०।१०) एवं ते० प्रा० (३।५।६)) में हुआ है। अतः स्पष्ट है कि आरम्भिक काल में भी न्याय-सम्बन्धी कार्यों एवं शासन-प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्यों में अन्तर-विशेष प्रकट कर दिया गया था। ताण्ड्यबा० (१४१६।६) में निर्देशित अग्नि-दिव्य (देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १४) तथा चोरी के अपराध में व्यक्ति द्वारा हाथ में जलता लौह-खण्ड रखना और उसका मारा जाना यह व्यक्त करता है कि दिव्य-ग्रहण कराया जाता था, और साथ ही साथ चोरी के अपराध में मृत्यु-दण्ड भी दिया जाता था। बृहस्पति (विवादरत्नाकर में उद्धृत) का कथन है-“यदि किसी सच्चरित्र एवं वेदाभ्यासी व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया है तो उसे बहुत समय तक बन्दी-गृह में रखना चाहिए और धन को लौटा देने के उपरान्त उससे प्रायश्चित्त कराना चाहिए।१४
परिषद् प्रायश्चित्तों के लिए स्वयं अपने नियम निर्धारित करती थी, और राजा दण्ड देता था। परिषद् के नियमों एवं राजा के दण्डों में कौन प्राचीन है, कहना कठिन है। यह बहुत सम्भव है कि परिषद् के धार्मिक न्याय-क्षेत्र में राजा दखल नहीं देता था और ब्राह्मण लोग न्यायाधीशों के रूप में एवं दण्ड-सम्बन्धी सम्मतियां देकर राजा को न्याय-शासन में सहायता देते थे। देखिए वसिष्ठ (५।१९४)। गौतम (८३१) ने शत० ब्रा० (५।४।४।५) के शब्दों के समान ही कहा है-राजा एवं बहुश्रुत ब्राह्मण संसार की नैतिक व्यवस्था को धारण करनेवाले हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१०।१२-१६) में एक महत्त्वपूर्ण सूचना है-"जो लोग इन्द्रिय-दौर्बल्य के कारण शास्त्रविहित जाति-सम्बन्धी सुविधाओं एवं कर्तव्यों के पालन से पथ-भ्रष्ट हो गये हों, उन्हें आचार्य उनके पापमय कृत्यों के अनुरूप शास्त्रानुमोदित प्रायश्चित्त करने की आज्ञा दे। जब वे अपने आचार्य के आदेश का उल्लंघन करें तो वह उन्हें राजा के पास ले जाय। राजा उन्हें धर्मशास्त्रज्ञ एवं शासन-चतुर पुरोहित के पास भेज दे। वह (पुरोहित), उन्हें यदि वे ब्राह्मण हैं, उचित प्रायश्चित्त करने का आदेश दे। शारीरिक दण्ड एवं दासता को छोड़कर वह अन्य कठिन साधनों द्वारा उन्हें हीन (दुर्बल)
१४. वृत्तस्वाध्यायवान् स्तेयो बन्धनात् क्लिश्यते चिरम् । स्वामिने तदनं दाप्यः प्रायश्चित्तं तु कारयेत् ॥ बृहस्पति (विवादरत्नाकर प० ३३१) । सम्भव है कि इस श्लोक का अर्थ यह है कि उस विद्वान् ब्राह्मण को, जो सदाचारी है, किन्तु जिसने लोभ में पड़कर चोरी कर ली है, बहुत काल तक बन्दी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बन्दी-जीवन से मन को पीड़ा होती है, अतः उससे धन लौटा देने के उपरान्त प्रायश्चित्त कराना चाहिए।
१५. दो लोके धृतवतो राजा ब्राह्मणश्च बहुश्रुतः। गौ० (८३१)। शतपथब्राह्मण (५।४।४।५) में आया है-'निषसाद धृतवत इति षतव्रतो वै राजा...एष च श्रोत्रियश्चतौ ह वै द्वौ मनुष्येषु धृतव्रतौ।'
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org