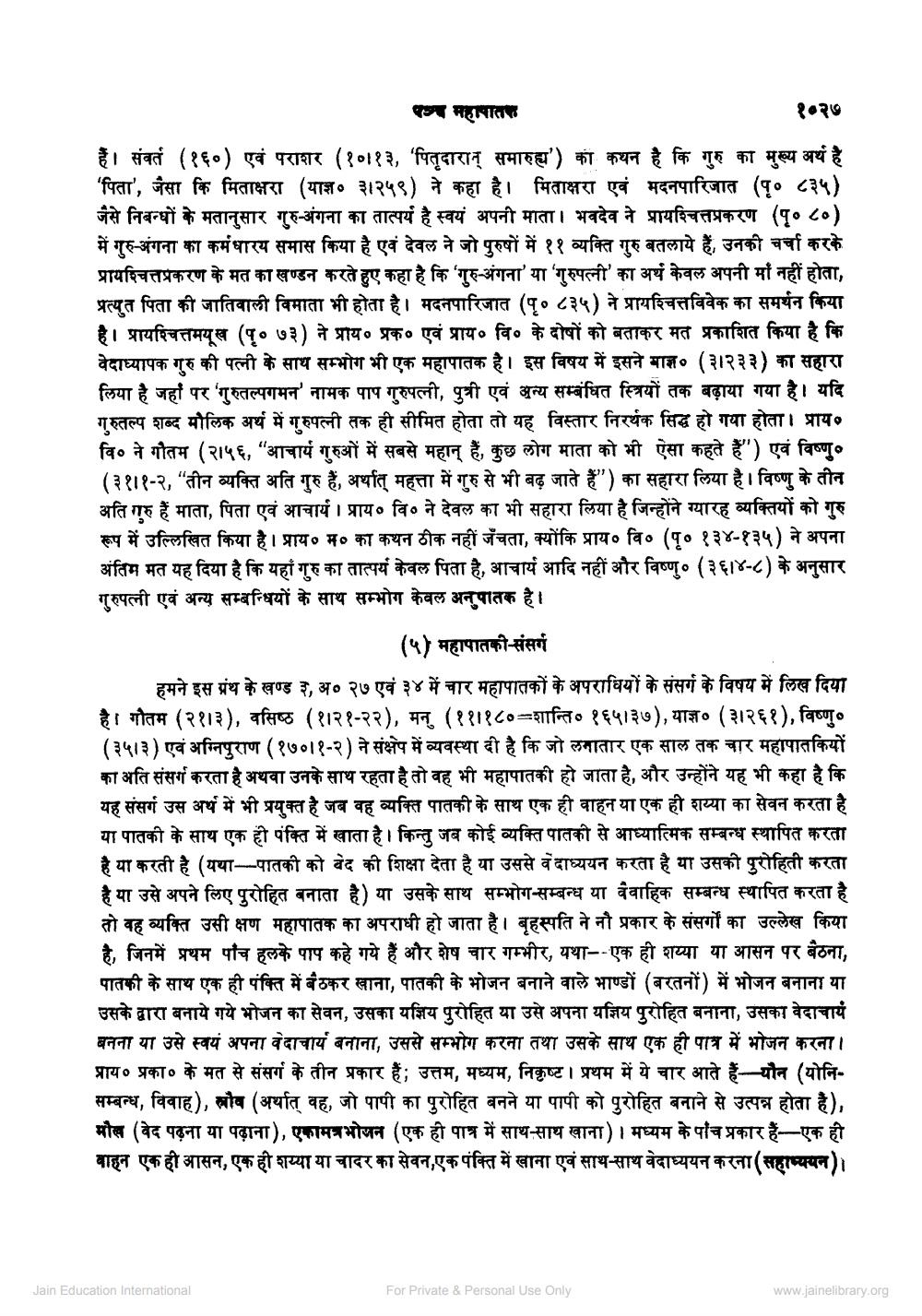________________
पञ्चमहापातक
१०२७
में
हैं । संवर्त (१६०) एवं पराशर (१०।१३, 'पितृदारात् समारुह्य' ) का कथन है कि गुरु का मुख्य अर्थ है 'पिता', जैसा कि मिताक्षरा ( याज्ञ० ३।२५९ ) ने कहा है । मिताक्षरा एवं मदनपारिजात ( पृ० ८३५ ) जैसे निबन्धों के मतानुसार गुरु-अंगना का तात्पर्य है स्वयं अपनी माता । भवदेव ने प्रायश्चित्तप्रकरण ( पृ० ८० ) गुरु-अंगना का कर्मधारय समास किया है एवं देवल ने जो पुरुषों में ११ व्यक्ति गुरु बतलाये हैं, उनकी चर्चा करके प्रायश्चित्तप्रकरण के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि 'गुरु-अंगना' या 'गुरुपत्नी' का अर्थ केवल अपनी माँ नहीं होता, प्रत्युत पिता की जातिवाली विमाता भी होता है। मदनपारिजात ( पृ० ८३५ ) ने प्रायश्चित्तविवेक का समर्थन किया है । प्रायश्चित्तमयूख ( पृ० ७३ ) ने प्राय० प्रक० एवं प्राय० वि० के दोषों को बताकर मत प्रकाशित किया है कि वेदाध्यापक गुरु की पत्नी के साथ सम्भोग भी एक महापातक है। इस विषय में इसने माज्ञ० ( ३।२३३ ) का सहारा लिया है जहाँ पर गुरुतल्पगमन' नामक पाप गुरुपत्नी, पुत्री एवं अन्य सम्बंधित स्त्रियों तक बढ़ाया गया है। यदि गुरुतल्प शब्द मौलिक अर्थ में गुरुपत्नी तक ही सीमित होता तो यह विस्तार निरर्थक सिद्ध हो गया होता। प्राय० वि० ने गौतम (२।५६, “ आचार्य गुरुओं में सबसे महान् हैं, कुछ लोग माता को भी ऐसा कहते हैं " ) एवं विष्णु ० ( ३१।१ - २, "तीन व्यक्ति अति गुरु हैं, अर्थात् महत्ता में गुरु से भी बढ़ जाते हैं") का सहारा लिया है। विष्णु के तीन अति गुरु हैं माता, पिता एवं आचार्य । प्राय० वि० ने देवल का भी सहारा लिया है जिन्होंने ग्यारह व्यक्तियों को गुरु रूप में उल्लिखित किया है। प्राय० म० का कथन ठीक नहीं जँचता, क्योंकि प्राय० वि० ( पृ० १३४ - १३५ ) ने अपना अंतिम मत यह दिया है कि यहाँ गुरु का तात्पर्य केवल पिता है, आचार्य आदि नहीं और विष्णु० (३६।४-८ ) के अनुसार गुरुपत्नी एवं अन्य सम्बन्धियों के साथ सम्भोग केवल अनुपातक है।
(५) महापातकी - संसर्ग
हमने इस ग्रंथ के खण्ड ३, अ० २७ एवं ३४ में चार महापातकों के अपराधियों के संसर्ग के विषय में लिख दिया है । गौतम (२१।३), वसिष्ठ ( १ । २१-२२ ), मनु ( ११।१८० = शान्ति० १६५ । ३७), याज्ञ० ( ३।२६१), विष्णु ० (३५।३) एवं अग्निपुराण (१७०।१-२ ) ने संक्षेप में व्यवस्था दी है कि जो लगातार एक साल तक चार महापातकियों का अति संसर्ग करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी महापातकी हो जाता है, और उन्होंने यह भी कहा है कि यह संसर्ग उस अर्थ में भी प्रयुक्त है जब वह व्यक्ति पातकी के साथ एक ही वाहन या एक ही शय्या का सेवन करता है। या पातकी के साथ एक ही पंक्ति में खाता है। किन्तु जब कोई व्यक्ति पातकी से आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करता है या करती है (यथा- पातकी को वेद की शिक्षा देता है या उससे वेदाध्ययन करता है या उसकी पुरोहिती करता है या उसे अपने लिए पुरोहित बनाता है) या उसके साथ सम्भोग सम्बन्ध या वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है तो वह व्यक्ति उसी क्षण महापातक का अपराधी हो जाता है। बृहस्पति ने नौ प्रकार के संसर्गों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रथम पाँच हलके पाप कहे गये हैं और शेष चार गम्भीर, यथा-- एक ही शय्या या आसन पर बैठना, पातकी के साथ एक ही पंक्ति में बैठकर खाना, पातकी के भोजन बनाने वाले भाण्डों ( बरतनों) में भोजन बनाना या उसके द्वारा बनाये गये भोजन का सेवन, उसका यज्ञिय पुरोहित या उसे अपना यज्ञिय पुरोहित बनाना, उसका वेदाचार्य बनना या उसे स्वयं अपना वेदाचार्य बनाना, उससे सम्भोग करना तथा उसके साथ एक ही पात्र में भोजन करना । प्रा० प्रका० के मत से संसर्ग के तीन प्रकार हैं; उत्तम, मध्यम, निकृष्ट । प्रथम में ये चार आते हैं—यौन (योनिसम्बन्ध, विवाह), लौव (अर्थात् वह, जो पापी का पुरोहित बनने या पापी को पुरोहित बनाने से उत्पन्न होता है),
(वेद पढ़ना या पढ़ाना), एकामत्र भोजन ( एक ही पात्र में साथ-साथ खाना)। मध्यम के पाँच प्रकार हैं - एक ही वाहन एक ही आसन, एक ही शय्या या चादर का सेवन, एक पंक्ति में खाना एवं साथ-साथ वेदाध्ययन करना (सहाध्ययन ) ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org