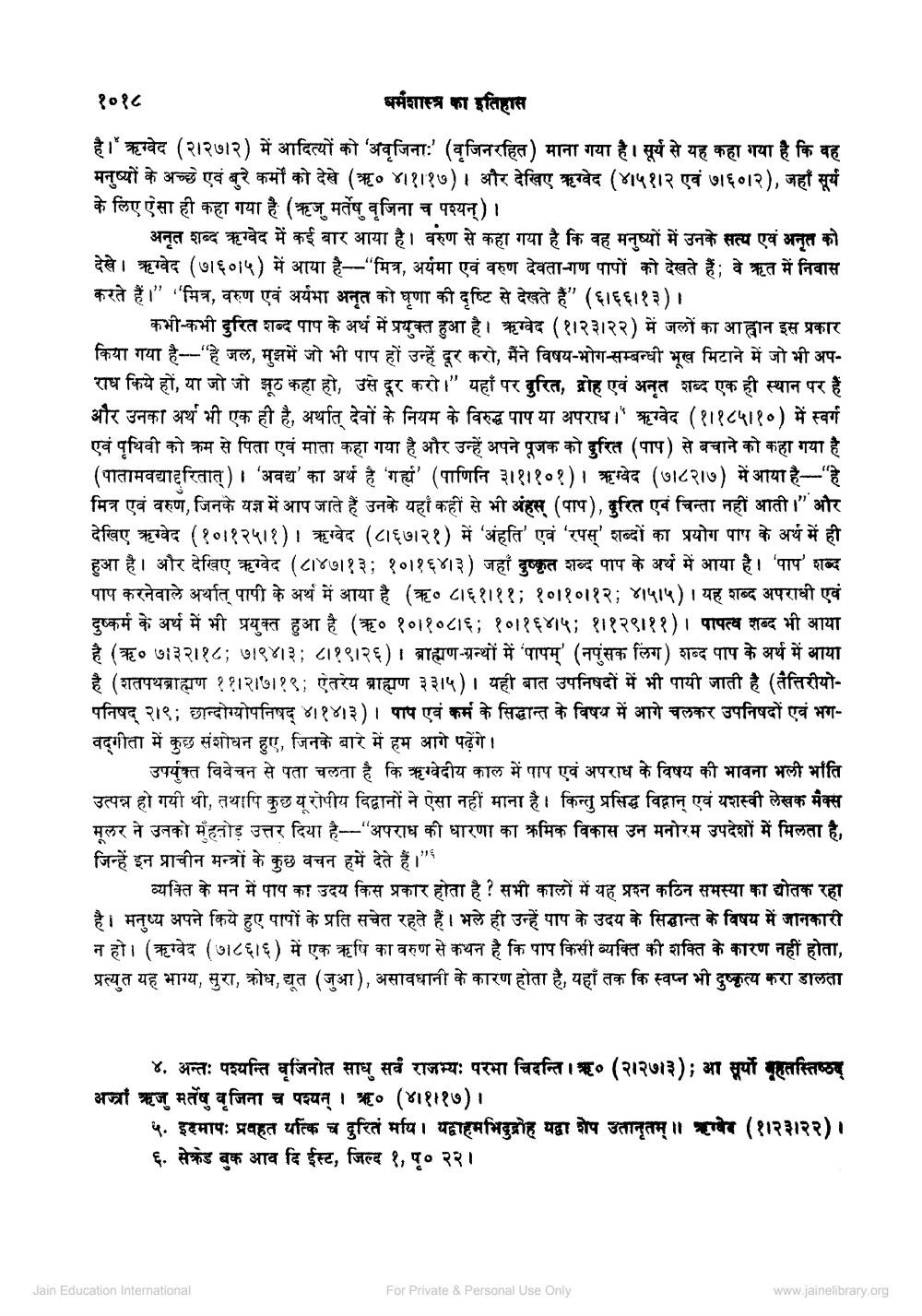________________
१०१८
धर्मशास्त्र का इतिहास
है। ऋग्वेद (२।२७।२) में आदित्यों को 'अवृजिना:' (वृजिनरहित) माना गया है। सूर्य से यह कहा गया है कि वह मनुष्यों के अच्छे एवं बुरे कर्मों को देखे ( ऋ० ४।१।१७ ) । और देखिए ऋग्वेद (४।५१।२ एवं ७ ६०/२), जहाँ सूर्य लिए ऐसा ही कहा गया है (ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन् ) ।
अनृत शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है। वरुण से कहा गया है कि वह मनुष्यों में उनके सत्य एवं अनृत को देखे । ऋग्वेद (७/६०/५ ) में आया है - "मित्र, अर्यमा एवं वरुण देवता- गण पापों को देखते हैं; वे ऋत में निवास करते हैं।" "मित्र, वरुण एवं अर्थभा अनृत को घृणा की दृष्टि से देखते हैं" (६।६६।१३) ।
कभी-कभी दुरित शब्द पाप के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद (१।२३।२२) में जलों का आह्वान इस प्रकार किया गया है -- " है जल, मुझमें जो भी पाप हों उन्हें दूर करो, मैंने विषय-भोग सम्बन्धी भूख मिटाने में जो भी अपराध किये हों, या जो जो झूठ कहा हो, उसे दूर करो।" यहाँ पर बुरित, द्रोह एवं अनृत शब्द एक ही स्थान पर हैं और उनका अर्थ भी एक ही है, अर्थात् देवों के नियम के विरुद्ध पाप या अपराध । ऋग्वेद (१।१८५।१०) में स्वर्ग एवं पृथिवी को क्रम से पिता एवं माता कहा गया है और उन्हें अपने पूजक को दुरित (पाप) से बचाने को कहा गया है ( पातामवद्यारितात्) । 'अवद्य' का अर्थ है 'ग' (पाणिनि ३।१।१०१) । ऋग्वेद ( ७१८२/७ ) में आया है - "हे मित्र एवं वरुण, जिनके यज्ञ में आप जाते हैं उनके यहाँ कहीं से भी अंहस् (पाप), दुरित एवं चिन्ता नहीं आती।" और देखिए ऋग्वेद (१०।१२५।१) । ऋग्वेद ( ८|६७।२१) में 'अंहति' एवं 'रपस्' शब्दों का प्रयोग पाप के अर्थ में ही हुआ है। और देखिए ऋग्वेद ( ८ ४७ १३ १० | १६४।३) जहाँ दुष्कृत शब्द पाप के अर्थ में आया है । 'पाप' शब्द पाप करनेवाले अर्थात् पापी के अर्थ में आया है (ऋ० ८ । ६१ ।११; १०।१०।१२; ४/५/५ ) | यह शब्द अपराधी एवं दुष्कर्म के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है ( ऋ० १० १०८/६; १० | १६४|५; १।१२९।११) । पापत्व शब्द भी आया है (ऋ० ७|३२|१८; ७१९४१३ ; ८।१९।२६ ) | ब्राह्मण-ग्रन्थों में 'पापम्' (नपुंसक लिंग) शब्द पाप के अर्थ में आया है (शतपथब्राह्मण ११/२/७/१९; ऐतरेय ब्राह्मण ३३।५ ) । यही बात उपनिषदों में भी पायी जाती है ( तैत्तिरीयोपनिषद् २।९; छान्दोग्योपनिषद् ४। १४१३) । पाप एवं कर्म के सिद्धान्त के विषय में आगे चलकर उपनिषदों एवं भगवद्गीता में कुछ संशोधन हुए, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
उपर्युक्त विवेचन से पता चलता है कि ऋग्वेदीय काल में पाप एवं अपराध के विषय की भावना भली भाँति उत्पन्न हो गयी थी, तथापि कुछ यूरोपीय विद्वानों ने ऐसा नहीं माना है। किन्तु प्रसिद्ध विद्वान् एवं यशस्वी लेखक मैक्स मूलर ने उनको मुँहतोड़ उत्तर दिया है--"अपराध की धारणा का क्रमिक विकास उन मनोरम उपदेशों में मिलता है, जिन्हें इन प्राचीन मन्त्रों के कुछ वचन हमें देते हैं ।'
१६
व्यक्ति के मन में पाप का उदय किस प्रकार होता है ? सभी कालों में यह प्रश्न कठिन समस्या का द्योतक रहा है। मनुष्य अपने किये हुए पापों के प्रति सचेत रहते हैं। भले ही उन्हें पाप के उदय के सिद्धान्त के विषय में जानकारी न हो। (ऋग्वेद (७।८६।६ ) में एक ऋषि का वरुण से कथन है कि पाप किसी व्यक्ति की शक्ति के कारण नहीं होता, प्रत्युत यह भाग्य, सुरा, क्रोध, द्यूत (जुआ), असावधानी के कारण होता है, यहाँ तक कि स्वप्न भी दुष्कृत्य करा डालता
४. अन्तः पश्यन्ति वृजिनोत साधु सर्वं राजभ्यः परमा चिदन्ति । ऋ० (२।२७१३ ) ; आ सूर्यो बृहतस्तिष्ठद् aat ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन् । ऋ० (४।१।१७ ) ।
५. इमापः प्रवहत थक्क च दुरितं मयि । यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेष उतानृतम् ॥ ऋग्वेद (१।२३।२२ ) । ६. सेक्रेड 'बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १, पृ० २२ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org