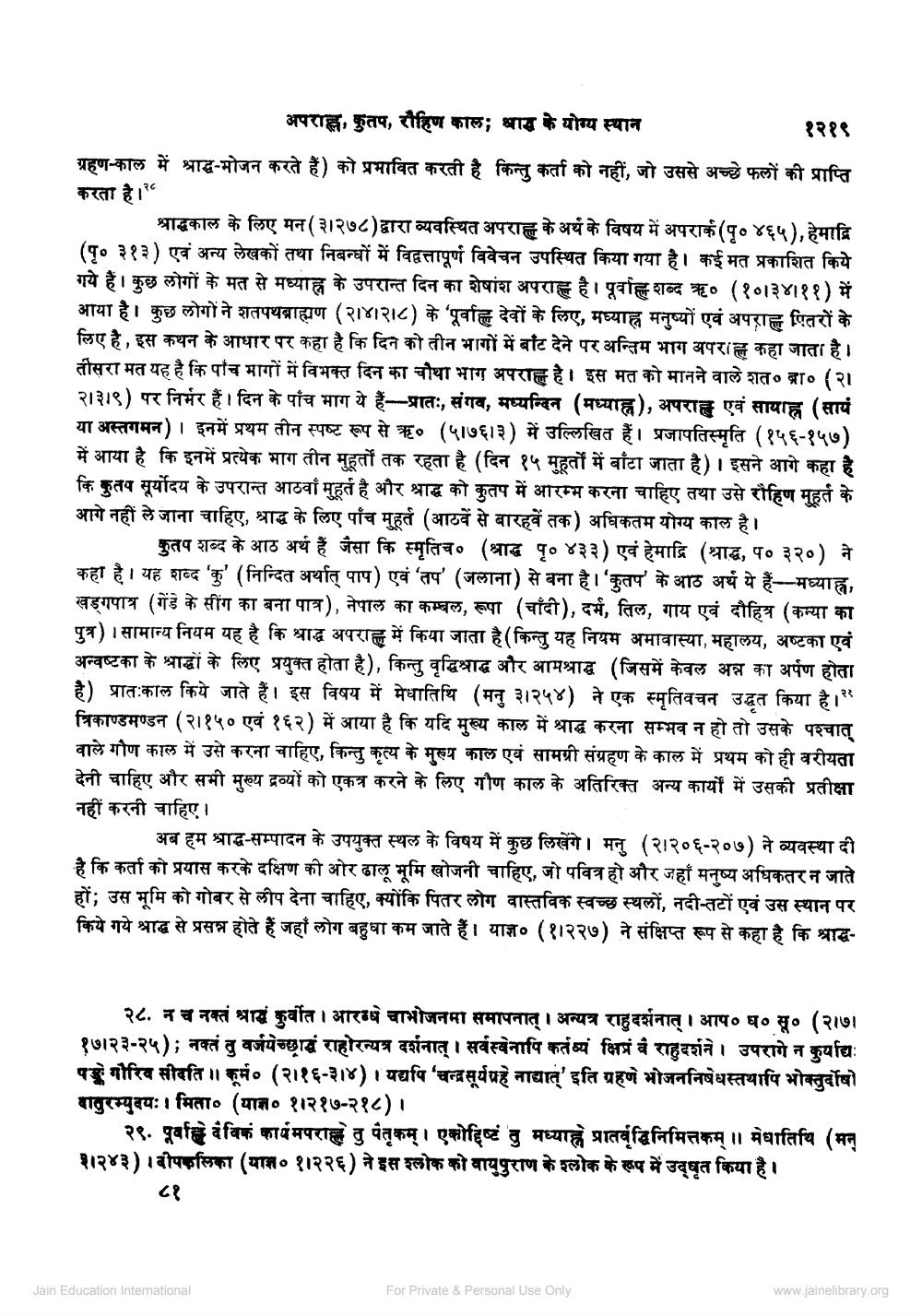________________
अपराह्न, कुतप, रौहिण काल; श्राद्ध के योग्य स्थान
१२१९
ग्रहण काल में श्राद्ध भोजन करते हैं) को प्रभावित करती है किन्तु कर्ता को नहीं, जो उससे अच्छे फलों की प्राप्ति करता है । "
२८
श्राद्धकाल के लिए मन ( ३।२७८) द्वारा व्यवस्थित अपराह्न के अर्थ के विषय में अपरार्क ( पृ० ४६५), हेमाद्रि ( पृ० ३१३ ) एवं अन्य लेखकों तथा निबन्धों में विद्वत्तापूर्ण विवेचन उपस्थित किया गया है। कई मत प्रकाशित किये गये हैं। कुछ लोगों के मत से मध्याह्न के उपरान्त दिन का शेषांश अपराह्न है । पूर्वाह्न शब्द ऋ० ( १०|३४|११ ) में आया है । कुछ लोगों ने शतपथब्राह्मण ( २/४/२८ ) के 'पूर्वाह्न देवों के लिए, मध्याह्न मनुष्यों एवं अपराह्न पितरों के लिए है, इस कथन के आधार पर कहा है कि दिन को तीन भागों में बाँट देने पर अन्तिम भाग अपराह्न कहा जाता है। तीसरा मत यह है कि पांच भागों में विभक्त दिन का चौथा भाग अपराह्न है। इस मत को मानने वाले शत० ब्रा० (२| २।३।९) पर निर्भर हैं। दिन के पाँच भाग ये हैं- प्रातः, संगव, मध्यन्दिन ( मध्याह्न), अपराह्न एवं सायाह्न (सायं या अस्तगमन) । इनमें प्रथम तीन स्पष्ट रूप से ऋ० (५/७६।३ ) में उल्लिखित हैं । प्रजापतिस्मृति ( १५६-१५७) में आया है कि इनमें प्रत्येक भाग तीन मुहूर्तों तक रहता है ( दिन १५ मुहूर्तों में बाँटा जाता है)। इसने आगे कहा है कि कुतप सूर्योदय के उपरान्त आठवाँ मुहूर्त है और श्राद्ध को कुतप में आरम्भ करना चाहिए तथा उसे रौहिण मुहूर्त के आगे नहीं ले जाना चाहिए, श्राद्ध के लिए पाँच मुहूर्त (आठवें से बारहवें तक) अधिकतम योग्य काल है।
तपशब्द के आठ अर्थ हैं जैसा कि स्मृतिच० ( श्राद्ध पृ० ४३३) एवं हेमाद्रि ( श्राद्ध, प० ३२० ) ने कहा है। यह शब्द 'कु' ( निन्दित अर्थात् पाप) एवं 'तप' (जलाना) से बना है। 'कुतप' के आठ अर्थ ये हैं-- मध्याह्न, खड्गपात्र (गेंडे के सींग का बना पात्र), नेपाल का कम्बल, रूपा (चाँदी), दर्भ, तिल, गाय एवं दौहित्र ( कन्या का पुत्र ) | सामान्य नियम यह है कि श्राद्ध अपराह्न में किया जाता है ( किन्तु यह नियम अमावास्या, महालय, अष्टका एवं अन्वष्टका के श्राद्धों के लिए प्रयुक्त होता है), किन्तु वृद्धिश्राद्ध और आमश्राद्ध ( जिसमें केवल अन्न का अर्पण होता है ) प्रातः काल किये जाते हैं । इस विषय में मेधातिथि ( मनु ३ । २५४ ) ने एक स्मृतिवचन उद्धृत किया है। " त्रिकाण्डमण्डन (२।१५० एवं १६२ ) में आया है कि यदि मुख्य काल में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो उसके पश्चात् वाले गौण काल में उसे करना चाहिए, किन्तु कृत्य के मुख्य काल एवं सामग्री संग्रहण के काल में प्रथम को ही वरीयता देनी चाहिए और सभी मुख्य द्रव्यों को एकत्र करने के लिए गौण काल के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।
अब हम श्राद्ध सम्पादन के उपयुक्त स्थल के विषय में कुछ लिखेंगे। मनु (२/२०६ -२०७) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को प्रयास करके दक्षिण की ओर ढालू भूमि खोजनी चाहिए, जो पवित्र हो और जहाँ मनुष्य अधिकतर न जाते हों; उस भूमि को गोबर से लीप देना चाहिए, क्योंकि पितर लोग वास्तविक स्वच्छ स्थलों, नदी-तटों एवं उस स्थान पर किये गये श्राद्ध से प्रसन्न होते हैं जहाँ लोग बहुधा कम जाते हैं। याज्ञ० (१।२२७) ने संक्षिप्त रूप से कहा है कि श्राद्ध
२८. न च नक्तं श्राद्धं कुर्वीत । आरम्धे चाभोजनमा समापनात् । अन्यत्र राहुदर्शनात् । आप० घ० सू० (२/७/ १७।२३-२५); नक्तं तु वर्जयेच्छ्राद्धं राहोरन्यत्र दर्शनात् । सर्वस्वेनापि कर्तव्यं क्षिप्रं वै राहुदर्शने । उपरागे न कुर्याद्यः पङ्के गौरिव सीदति ।। कूर्म ० ( २।१६-३।४) । यद्यपि 'चन्द्रसूर्य ग्रहे नाद्यात्' इति ग्रहणे भोजननिषेधस्तथापि भोक्तुर्दोषो वातुरम्युदयः । मिता० ( याश० १।२१७-२१८ ) ।
२९. पूर्वा वैविकं कार्यमपराह्णे तु पैतृकम् । एकोद्दिष्टं तु मध्याह्ने प्रातर्वृद्धिनिमित्तकम् । मेधातिथि ( मन् ३।२४३) । दीपकलिका (याश० १।२२६) ने इस श्लोक को वायुपुराण के श्लोक के रूप में उद्धृत किया है।
८१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org