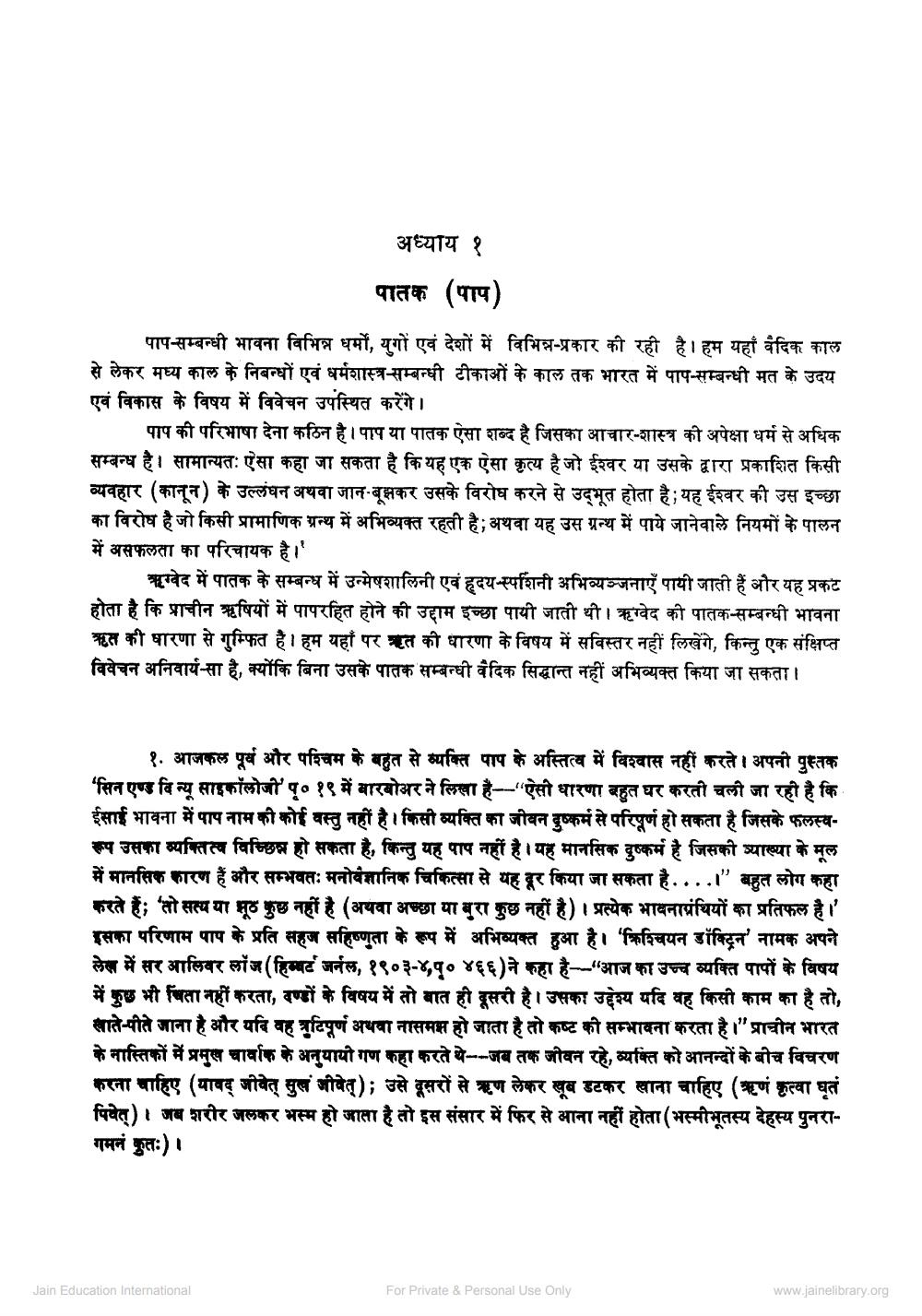________________
अध्याय १
पातक (पाप)
पाप-सम्बन्धी भावना विभिन्न धर्मों, युगों एवं देशों में विभिन्न प्रकार की रही है। हम यहाँ वैदिक काल से लेकर मध्य काल के निबन्धों एवं धर्मशास्त्र सम्बन्धी टीकाओं के काल तक भारत में पाप सम्बन्धी मत के उदय एवं विकास के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे।
पाप की परिभाषा देना कठिन है। पाप या पातक ऐसा शब्द है जिसका आचार-शास्त्र की अपेक्षा धर्म से अधिक सम्बन्ध है । सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा कृत्य है जो ईश्वर या उसके द्वारा प्रकाशित किसी व्यवहार (कानून) के उल्लंघन अथवा जान-बूझकर उसके विरोध करने से उद्भूत होता है; यह ईश्वर की उस इच्छा का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में अभिव्यक्त रहती है; अथवा यह उस ग्रन्थ में पाये जानेवाले नियमों के पालन में असफलता का परिचायक है । '
ॠग्वेद में पातक के सम्बन्ध में उन्मेषशालिनी एवं हृदय-स्पर्शनी अभिव्यञ्जनाएँ पायी जाती हैं और यह प्रकट होता है कि प्राचीन ऋषियों में पापरहित होने की उद्दाम इच्छा पायी जाती थी। ऋग्वेद की पातक-सम्बन्धी भावना ॠ की धारणा से गुम्फित है। हम यहाँ पर ऋत की धारणा के विषय में सविस्तर नहीं लिखेंगे, किन्तु एक संक्षिप्त विवेचन अनिवार्य - सा है, क्योंकि बिना उसके पातक सम्बन्धी वैदिक सिद्धान्त नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता।
१. आजकल पूर्व और पश्चिम के बहुत से व्यक्ति पाप के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। अपनी पुस्तक 'सिन एण्ड वि न्यू साइकॉलोजी' पृ० १९ में बारबोअर ने लिखा है- "ऐसी धारणा बहुत घर करती चली जा रही है कि ईसाई भावना में पाप नाम की कोई वस्तु नहीं है। किसी व्यक्ति का जीवन दुष्कर्म से परिपूर्ण हो सकता है जिसके फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व विच्छिन्न हो सकता है, किन्तु यह पाप नहीं है। यह मानसिक दुष्कर्म है जिसकी व्याख्या के मूल में मानसिक कारण हैं और सम्भवतः मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से यह दूर किया जा सकता है..." बहुत लोग 'कहा करते हैं; 'तो सत्य या झूठ कुछ नहीं है (अथवा अच्छा या बुरा कुछ नहीं है) । प्रत्येक भावनाग्रंथियों का प्रतिफल है।' इसका परिणाम पाप के प्रति सहज सहिष्णुता के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। 'क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन' नामक अपने लेख में सर आलिवर लॉज (हिम्बर्ट जर्नल, १९०३ -४, पृ० ४६६) ने कहा है---"आज का उच्च व्यक्ति पापों के विषय में कुछ भी बता नहीं करता, दण्डों के विषय में तो बात ही दूसरी है। उसका उद्देश्य यदि वह किसी काम का है तो, खाते-पीते जाना है और यदि वह त्रुटिपूर्ण अथवा नासमझ हो जाता है तो कष्ट की सम्भावना करता है।" प्राचीन भारत के नास्तिकों में प्रमुख चार्वाक के अनुयायी गण कहा करते थे-- जब तक जीवन रहे, व्यक्ति को आनन्दों के बीच विचरण करना चाहिए ( यावद् जीवेत् सुखं जीवेत्); उसे दूसरों से ऋण लेकर खूब डटकर खाना चाहिए (ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्) । जब शरीर जलकर भस्म हो जाता है तो इस संसार में फिर से आना नहीं होता ( भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ) ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org