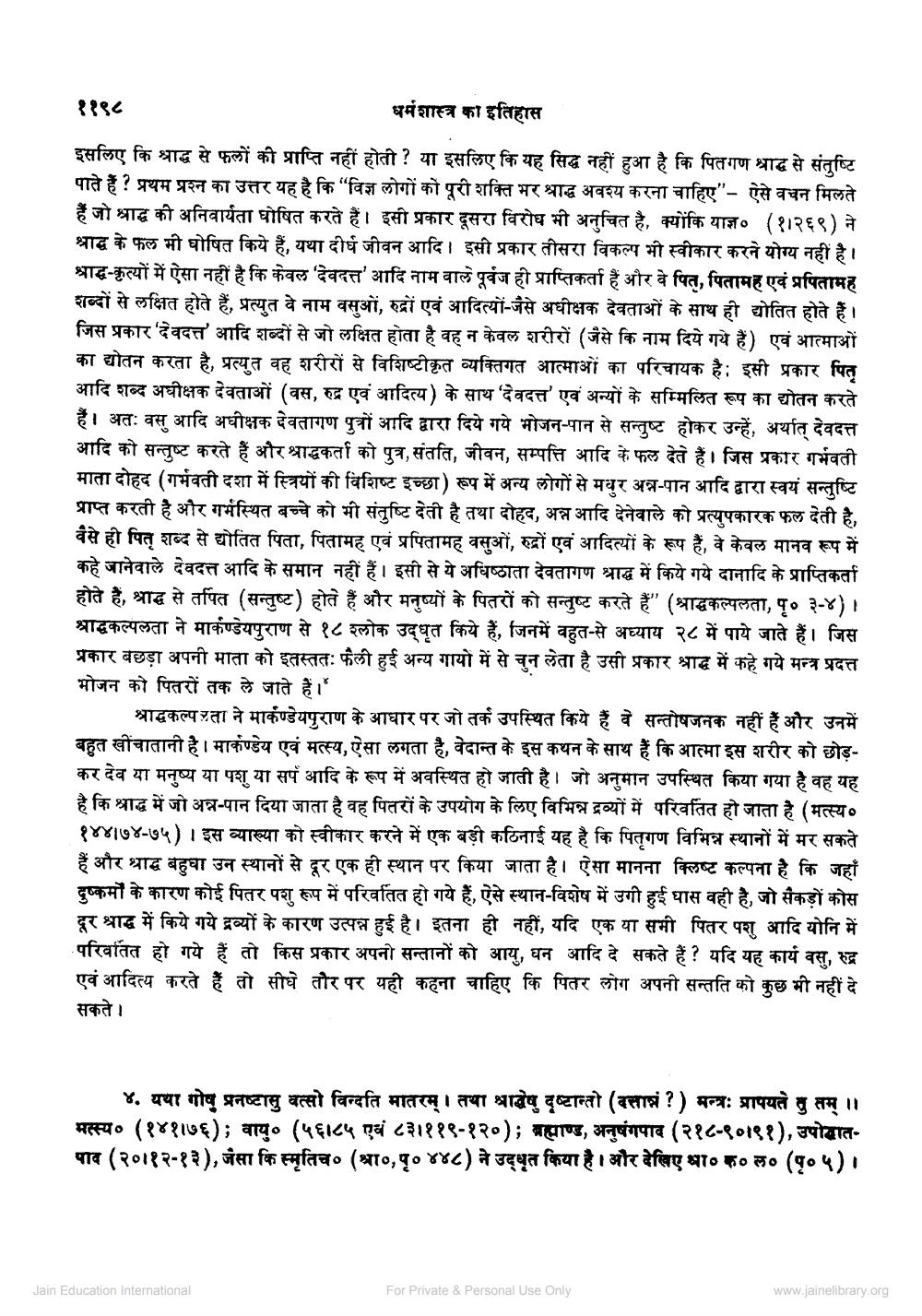________________
११९८
धर्मशास्त्र का इतिहास
इसलिए कि श्राद्ध से फलों की प्राप्ति नहीं होती? या इसलिए कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि पितगण श्राद्ध से संतुष्टि पाते हैं ? प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि "विज्ञ लोगों को पूरी शक्ति भर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए"- ऐसे वचन मिलते हैं जो श्राद्ध की अनिवार्यता घोषित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा विरोध भी अनुचित है, क्योंकि याज्ञ० (१।२६९) ने श्राद्ध के फल भी घोषित किये हैं, यथा दीर्घ जीवन आदि। इसी प्रकार तीसरा विकल्प भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। श्राद्ध-कृत्यों में ऐसा नहीं है कि केवल 'देवदत्त' आदि नाम वाले पूर्वज ही प्राप्तिकर्ता हैं और वे पित, पितामह एवं प्रपितामह शब्दों से लक्षित होते हैं, प्रत्युत वे नाम वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों-जैसे अधीक्षक देवताओं के साथ ही द्योतित होते हैं। जिस प्रकार 'देवदत्त आदि शब्दों से जो लक्षित होता है वह न केवल शरीरों (जैसे कि नाम दिये गये हैं) एवं आत्माओं का द्योतन करता है, प्रत्युत वह शरीरों से विशिष्टीकृत व्यक्तिगत आत्माओं का परिचायक है। इसी प्रकार पितृ आदि शब्द अधीक्षक देवताओं (वस, रुद्र एवं आदित्य) के साथ 'देवदत्त' एवं अन्यों के सम्मिलित रूप का द्योतन करते हैं। अतः वसु आदि अधीक्षक देवतागण पुत्रों आदि द्वारा दिये गये भोजन-पान से सन्तुष्ट होकर उन्हें, अर्थात् देवदत्त आदि को सन्तुष्ट करते हैं और श्राद्धकर्ता को पुत्र, संतति, जीवन, सम्पत्ति आदि के फल देते हैं। जिस प्रकार गर्भवती माता दोहद (गर्भवती दशा में स्त्रियों की विशिष्ट इच्छा) रूप में अन्य लोगों से मधुर अन्न-पान आदि द्वारा स्वयं सन्तुष्टि प्राप्त करती है और गर्मस्थित बच्चे को भी संतुष्टि देती है तथा दोहद, अन्न आदि देनेवाले को प्रत्युपकारक फल देती है, वैसे ही पितृ शब्द से द्योतित पिता, पितामह एवं प्रपितामह वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के रूप हैं, वे केवल मानव रूप में कहे जानेवाले देवदत्त आदि के समान नहीं हैं। इसी से ये अधिष्ठाता देवतागण श्राद्ध में किये गये दानादि के प्राप्तिकर्ता होते हैं, श्राद्ध से तर्पित (सन्तुष्ट) होते हैं और मनुष्यों के पितरों को सन्तुष्ट करते हैं" (श्राद्धकल्पलता, पृ० ३-४)। श्राद्धकल्पलता ने मार्कण्डेयपुराण से १८ श्लोक उद्धृत किये हैं, जिनमें बहुतसे अध्याय २८ में पाये जाते हैं। जिस प्रकार बछड़ा अपनी माता को इतस्ततः फैली हुई अन्य गायों में से चुन लेता है उसी प्रकार श्राद्ध में कहे गये मन्त्र प्रदत्त भोजन को पितरों तक ले जाते हैं।'
श्राद्धकल्परता ने मार्कण्डेयपुराण के आधार पर जो तर्क उपस्थित किये हैं वे सन्तोषजनक नहीं हैं और उनमें बहुत खींचातानी है। मार्कण्डेय एवं मत्स्य, ऐसा लगता है, वेदान्त के इस कथन के साथ हैं कि आत्मा इस शरीर को छोड़कर देव या मनुष्य या पशु या सर्प आदि के रूप में अवस्थित हो जाती है। जो अनुमान उपस्थित किया गया है वह यह है कि श्राद्ध में जो अन्न-पान दिया जाता है वह पितरों के उपयोग के लिए विभिन्न द्रव्यों में परिवर्तित हो जाता है (मत्स्य० १४४१७४-७५) । इस व्याख्या को स्वीकार करने में एक बड़ी कठिनाई यह है कि पितृगण विभिन्न स्थानों में मर सकते हैं और श्राद्ध बहुधा उन स्थानों से दूर एक ही स्थान पर किया जाता है। ऐसा मानना क्लिष्ट कल्पना है कि जहाँ दुष्कर्मों के कारण कोई पितर पशु रूप में परिवर्तित हो गये हैं, ऐसे स्थान-विशेष में उगी हुई घास वही है, जो सैकड़ों कोस दूर श्राद्ध में किये गये द्रव्यों के कारण उत्पन्न हुई है। इतना ही नहीं, यदि एक या सभी पितर पशु आदि योनि में परिवर्तित हो गये हैं तो किस प्रकार अपनो सन्तानों को आयु, धन आदि दे सकते हैं ? यदि यह कार्य वसु, रुद्र एवं आदित्य करते हैं तो सीधे तौर पर यही कहना चाहिए कि पितर लोग अपनी सन्तति को कुछ भी नहीं दे सकते।
४. यथा गोष प्रनष्टासु वत्सो विन्दति मातरम् । तथा श्राद्धेषु दृष्टान्तो (दत्तानं ?) मन्त्रः प्रापयते तु तम् ॥ मत्स्य० (१४११७६); वायु० (५६०८५ एवं ८३।११९-१२०); ब्रह्माण्ड, अनुषंगपाद (२१८-९०।९१), उपोतातपाव (२०१२-१३), जैसा कि स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४४८) ने उद्धृत किया है। और देखिए श्रा०क० ल० (पृ०५)।
For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org