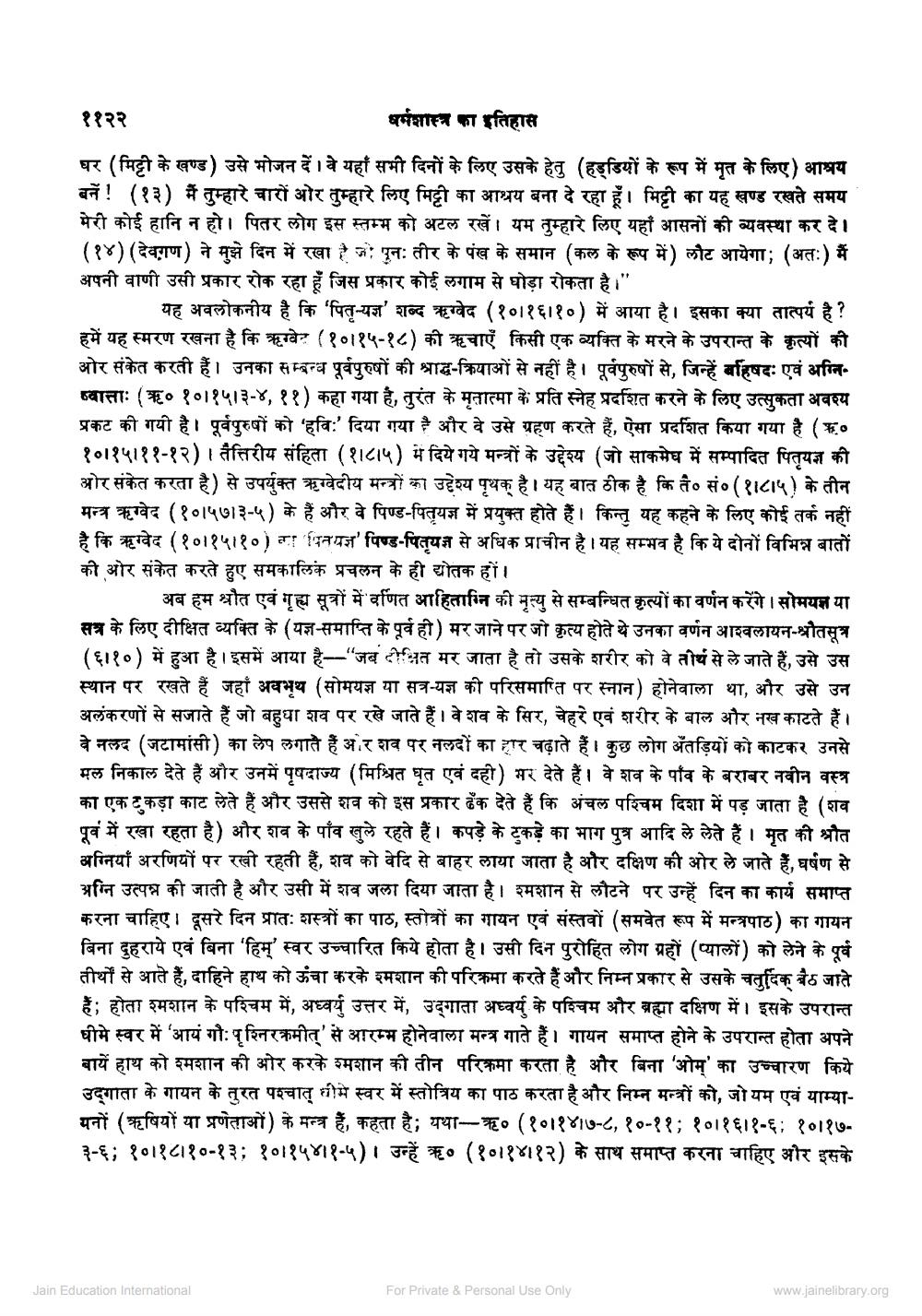________________
११२२
धर्मशास्त्र का इतिहास
घर (मिट्टी के खण्ड) उसे भोजन दें। वे यहाँ सभी दिनों के लिए उसके हेतु (हड्डियों के रूप में मृत के लिए) आश्रय बनें ! (१३) मैं तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे लिए मिट्टी का आश्रय बना दे रहा हूँ। मिट्टी का यह खण्ड रखते समय मेरी कोई हानि न हो। पितर लोग इस स्तम्म को अटल रखें। यम तुम्हारे लिए यहाँ आसनों की व्यवस्था कर दे। (१४) (देवगण) ने मुझे दिन में रखा है जो पुनः तीर के पंख के समान (कल के रूप में) लौट आयेगा; (अतः) मैं अपनी वाणी उसी प्रकार रोक रहा हूँ जिस प्रकार कोई लगाम से घोड़ा रोकता है।"
यह अवलोकनीय है कि 'पितृ-यज्ञ' शब्द ऋग्वेद (१०।१६।१०) में आया है। इसका क्या तात्पर्य है ? हमें यह स्मरण रखना है कि ऋग्वेट (१०।१५-१८) की ऋचाएँ किसी एक व्यक्ति के मरने के उपरान्त के कृत्यों की ओर संकेत करती हैं। उनका सम्बन्ध पूर्वपुरुषों की श्राद्ध-क्रियाओं से नहीं है। पूर्वपुरुषों से, जिन्हें बहिषदः एवं अग्निहवात्ताः (ऋ० १०।१५।३-४, ११) कहा गया है, तुरंत के मृतात्मा के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए उत्सुकता अवश्य प्रकट की गयी है। पूर्वपुरुषों को 'हवि:' दिया गया है और वे उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा प्रदर्शित किया गया है (फ.. १०।१५।११-१२) । तैत्तिरीय संहिता (११८५) में दिये गये मन्त्रों के उद्देश्य (जो साकमेघ में सम्पादित पितृयज्ञ की ओर संकेत करता है) से उपर्युक्त ऋग्वेदीय मन्त्रों का उद्देश्य पृथक् है। यह बात ठीक है कि तै० सं० (१९८५) के तीन मन्त्र ऋग्वेद (१०।५७।३-५) के हैं और वे पिण्ड-पितृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु यह कहने के लिए कोई तर्क नहीं है कि ऋग्वेद (१०।१५।१०) पिनयज्ञ' पिण्ड-पितृयज्ञ से अधिक प्राचीन है। यह सम्भव है कि ये दोनों विभिन्न बातों की ओर संकेत करते हुए समकालिकं प्रचलन के ही द्योतक हों।
अब हम श्रौत एवं गृह्य सूत्रों में वर्णित आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित कृत्यों का वर्णन करेंगे। सोमयज्ञ या सत्र के लिए दीक्षित व्यक्ति के (यज्ञ-समाप्ति के पूर्व ही) मर जाने पर जो कृत्य होते थे उनका वर्णन आश्वलायन-श्रौतसूत्र (६।१०) में हुआ है। इसमें आया है-"जब दीक्षित मर जाता है तो उसके शरीर को वे तीर्थ से ले जाते हैं, उसे उस स्थान पर रखते हैं जहाँ अवभृथ (सोमयज्ञ या सत्र-यज्ञ की परिसमाप्ति पर स्नान) होनेवाला था, और उसे उन अलंकरणों से सजाते हैं जो बहुधा शव पर रखे जाते हैं। वे शव के सिर, चेहरे एवं शरीर के बाल और नख काटते हैं। वे नलद (जटामांसी) का लेप लगाते हैं और शव पर नलदों का हार चढ़ाते हैं। कुछ लोग अंतड़ियों को काटकर उनसे मल निकाल देते हैं और उनमें पृषदाज्य (मिश्रित घृत एवं दही) भर देते हैं। वे शव के पाँव के बराबर नवीन वस्त्र का एक टुकड़ा काट लेते हैं और उससे शव को इस प्रकार ढंक देते हैं कि अंचल पश्चिम दिशा में पड़ जाता है (शव पूर्व में रखा रहता है) और शव के पाँव खुले रहते हैं। कपड़े के टुकड़े का भाग पुत्र आदि ले लेते हैं। मृत की श्रौत अग्नियाँ अरणियों पर रखी रहती हैं, शव को वेदि से बाहर लाया जाता है और दक्षिण की ओर ले जाते हैं, घर्षण से अग्नि उत्पन्न की जाती है और उसी में शव जला दिया जाता है। श्मशान से लौटने पर उन्हें दिन का कार्य समाप्त करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः शस्त्रों का पाठ, स्तोत्रों का गायन एवं संस्तवों (समवेत रूप में मन्त्रपाठ) का गायन बिना दुहराये एवं बिना 'हिम्' स्वर उच्चारित किये होता है। उसी दिन पुरोहित लोग ग्रहों (प्यालों) को लेने के पूर्व तीर्थों से आते हैं, दाहिने हाथ को ऊंचा करके श्मशान की परिक्रमा करते हैं और निम्न प्रकार से उसके चतुर्दिक बैठ जाते हैं; होता श्मशान के पश्चिम में, अध्वर्यु उत्तर में, उद्गाता अध्वर्यु के पश्चिम और ब्रह्मा दक्षिण में। इसके उपरान्त धीमे स्वर में 'आयं गौः पृश्निरक्रमीत्' से आरम्भ होनेवाला मन्त्र गाते हैं। गायन समाप्त होने के उपरान्त होता अपने बायें हाथ को श्मशान की ओर करके श्मशान की तीन परिक्रमा करता है और बिना 'ओम्' का उच्चारण किये उदगाता के गायन के तुरत पश्चात् धीमे स्वर में स्तोत्रिय का पाठ करता है और निम्न मन्त्रों को, जो यम एवं याम्यामनों (ऋषियों या प्रणेताओं) के मन्त्र हैं, कहता है; यथा-ऋ० (१०।१४१७-८, १०-११; १०।१६।१-६; १०।१७३-६; १०।१८।१०-१३; १०११५४।१-५)। उन्हें ऋ० (१०।१४।१२) के साथ समाप्त करना चाहिए और इसके
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org