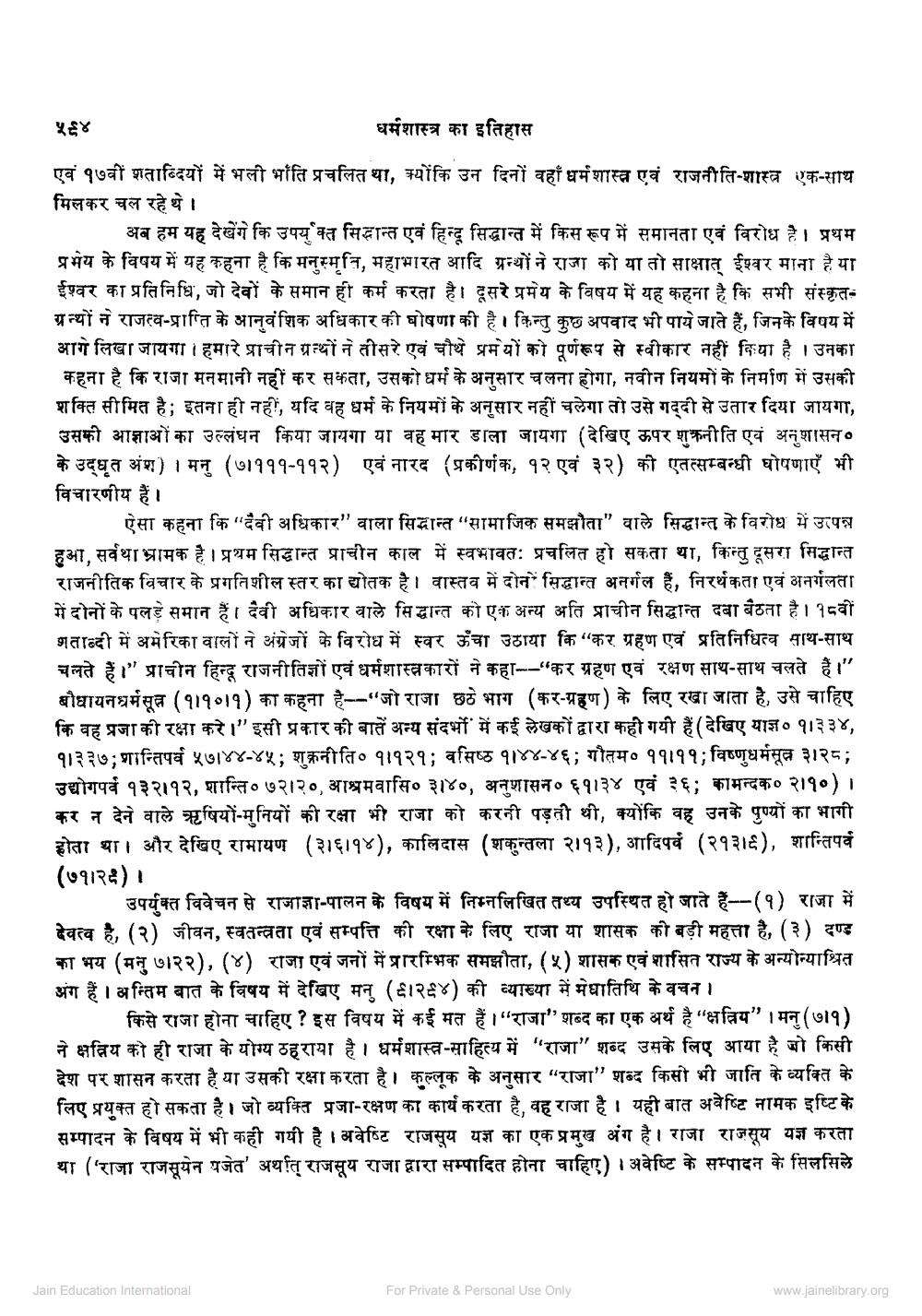________________
५६४
धर्मशास्त्र का इतिहास
एवं १७वीं शताब्दियों में भली भाँति प्रचलित था, क्योंकि उन दिनों वहाँ धर्मशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र एक-साथ मिलकर चल रहे थे ।
अब हम यह देखेंगे कि उपर्युक्त सिद्धान्त एवं हिन्दू सिद्धान्त में किस रूप में समानता एवं विरोध है। प्रथम प्रमेय के विषय में यह कहना है कि मनुस्मृति, महाभारत आदि ग्रन्थों ने राजा को या तो साक्षात् ईश्वर माना है या ईश्वर का प्रतिनिधि, जो देवों के समान ही कर्म करता है। दूसरे प्रमेय के विषय में यह कहना है कि सभी संस्कृतग्रन्थों ने राजत्व-प्राप्ति के आनुवंशिक अधिकार की घोषणा की है । किन्तु कुछ अपवाद भी पाये जाते हैं, जिनके विषय में आगे लिखा जायगा । हमारे प्राचीन ग्रन्थों ने तीसरे एवं चौथे प्रमेयों को पूर्णरूप से स्वीकार नहीं दिया है । उनका कहना है कि राजा मनमानी नहीं कर सकता, उसको धर्म के अनुसार चलना होगा, नवीन नियमों के निर्माण में उसकी शक्ति सीमित है; इतना ही नहीं, यदि वह धर्म के नियमों के अनुसार नहीं चलेगा तो उसे गद्दी से उतार दिया जायगा, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया जायगा या वह मार डाला जायगा (देखिए ऊपर शुक्रनीति एवं अनुशासन ० के उद्धृत अंश ) । मनु ( ७।१११ - ११२ ) एवं नारद ( प्रकीर्णक, १२ एवं ३२ ) की एतत्सम्बन्धी घोषणाएँ भी विचारणीय हैं ।
ऐसा कहना कि " दैवी अधिकार" वाला सिद्धान्त "सामाजिक समझौता " वाले सिद्धान्त के विरोध में उत्पन्न हुआ, , सर्वथा भ्रामक है। प्रथम सिद्धान्त प्राचीन काल में स्वभावत: प्रचलित हो सकता था, किन्तु दूसरा सिद्धान्त राजनीतिक विचार के प्रगतिशील स्तर का द्योतक है। वास्तव में दोनों सिद्धान्त अनर्गल हैं, निरर्थकता एवं अनर्गलता में दोनों के पलड़े समान हैं। देवी अधिकार वाले सिद्धान्त को एक अन्य अति प्राचीन सिद्धान्त दबा बैठता है । १८वीं शताब्दी में अमेरिका वालों ने अंग्रेजों के विरोध में स्वर ऊंचा उठाया कि "कर ग्रहण एवं प्रतिनिधित्व साथ-साथ चलते हैं।" प्राचीन हिन्दू राजनीतिज्ञों एवं धर्मशास्त्रकारों ने कहा- "कर ग्रहण एवं रक्षण साथ-साथ चलते हैं ।"
धर्मसूत्र ( 111०1१ ) का कहना है -- " जो राजा छठे भाग ( कर-ग्रहण) के लिए रखा जाता है, उसे चाहिए कि वह प्रजा की रक्षा करे ।" इसी प्रकार की बातें अन्य संदर्भों में कई लेखकों द्वारा कही गयी हैं (देखिए याज्ञ० १।३३४, १।३३७; शान्तिपर्व ५७।४४-४५; शुक्रनीति० १।१२१ ; वसिष्ठ १।४४ - ४६ ; गौतम ० ११११ ; विष्णुधर्मसूत्र ३१२८; उद्योगपर्व १३२।१२, शान्ति० ७२ २०, आश्रमवासि० ३।४०, अनुशासन० ६१।३४ एवं ३६ कामन्दक० २।१० ) । कर न देने वाले ऋषियों-मुनियों की रक्षा भी राजा को करनी पड़ती थी, क्योंकि वह उनके पुण्यों का भागी होता था । और देखिए रामायण ( ३।६।१४ ), कालिदास ( शकुन्तला २।१३), आदिपर्व ( २१३६ ), शान्तिपर्व (७१२६) ।
उपर्युक्त विवेचन से राजाज्ञा-पालन के विषय में निम्नलिखित तथ्य उपस्थित हो जाते हैं -- (१) राजा में देवत्व है, (२) जीवन, स्वतन्त्रता एवं सम्पत्ति की रक्षा के लिए राजा या शासक की बड़ी महत्ता है, (३) दण्ड का भय (मनु ७।२२), (४) राजा एवं जनों में प्रारम्भिक समझौता, (५) शासक एवं शासित राज्य के अन्योन्याश्रित अंग हैं । अन्तिम बात के विषय में देखिए मनु ( ६ | २६४ ) की व्याख्या में मेधातिथि के वचन ।
किसे राजा होना चाहिए ? इस विषय में कई मत हैं । "राजा" शब्द का एक अर्थ है "क्षत्रिय" । मनु ( ७19 ) ने क्षत्रिय को ही राजा के योग्य ठहराया है। धर्मशास्त्र - साहित्य में "राजा" शब्द उसके लिए आया है जो किसी देश पर शासन करता है या उसकी रक्षा करता है। कुल्लूक के अनुसार "राजा" शब्द किसी भी जाति के व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति प्रजा रक्षण का कार्य करता है, वह राजा है । यही बात अवेष्टि नामक इष्टि के सम्पादन के विषय में भी कही गयी है । अवेष्टि राजसूय यज्ञ का एक प्रमुख अंग है । राजा राजसूय यज्ञ करता था ( 'राजा राजसूयेन यजेत' अर्थात् राजसूय राजा द्वारा सम्पादित होना चाहिए ) । अवेष्टि के सम्पादन के सिलसिले
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org