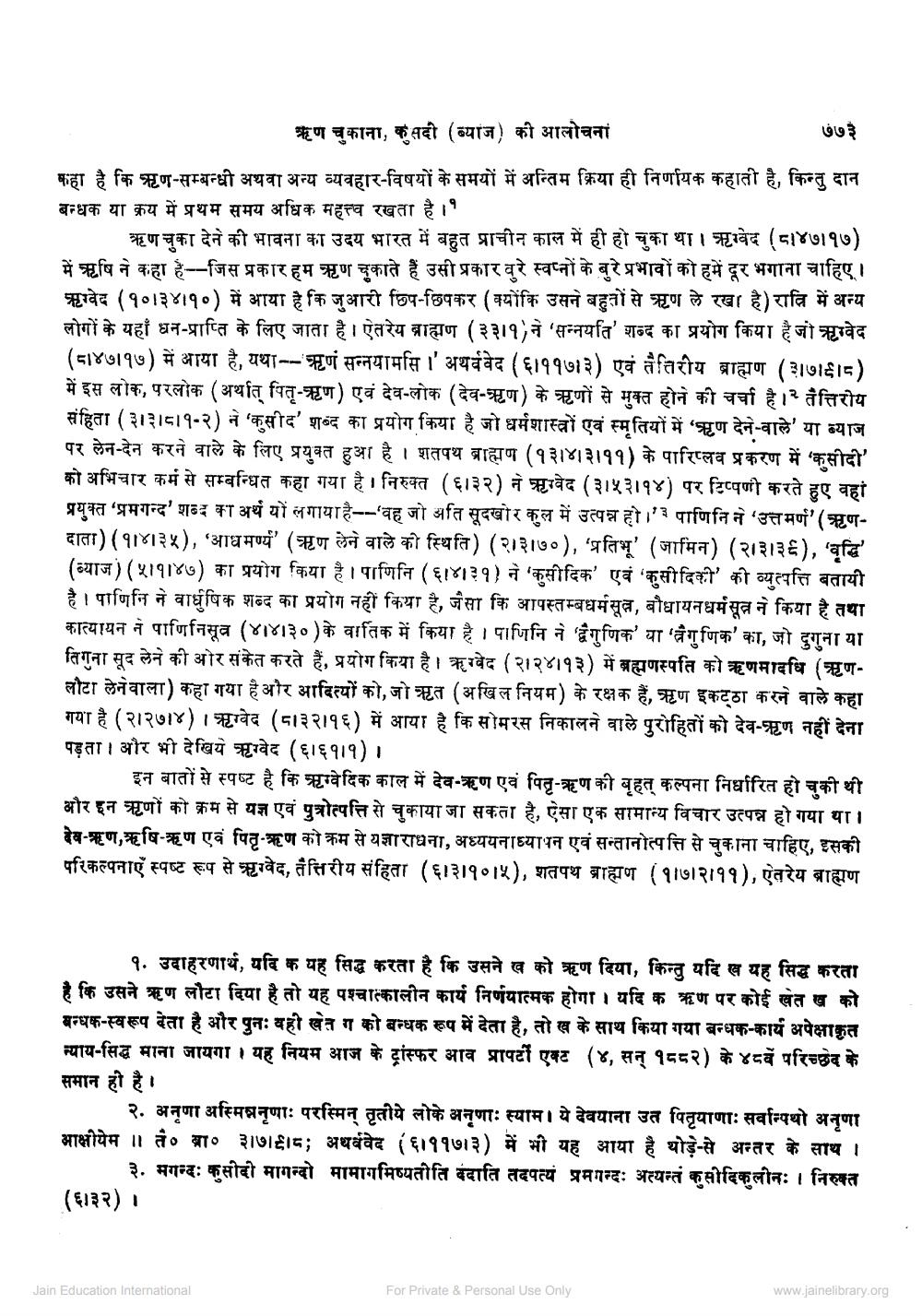________________
ऋण चुकाना, कुसदी (ब्याज) की आलोचना
७७३ कहा है कि ऋण-सम्बन्धी अथवा अन्य व्यवहार-विषयों के समयों में अन्तिम क्रिया ही निर्णायक कहाती है, किन्तु दान बन्धक या क्रय में प्रथम समय अधिक महत्त्व रखता है।
ऋण चुका देने की भावना का उदय भारत में बहुत प्राचीन काल में ही हो चुका था। ऋग्वेद (८४७।१७) में ऋषि ने कहा है-जिस प्रकार हम ऋण चुकाते हैं उसी प्रकार वुरे स्वप्नों के बुरे प्रभावों को हमें दूर भगाना चाहिए। ऋग्वेद (१०।३४।१०) में आया है कि जुआरी छिप-छिपकर (क्योंकि उसने बहुतों से ऋण ले रखा है) रात्रि में अन्य लोगों के यहाँ धन-प्राप्ति के लिए जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण (३३।१)ने 'सन्नयति' शब्द का प्रयोग किया है जो ऋग्वेद (८४७।१७) में आया है, यथा--ऋणं सन्नयामसि ।' अथर्ववेद (६।११७१३) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (३७६८) में इस लोक, परलोक (अर्थात् पितृ-ऋण) एवं देव-लोक (देव-ऋण) के ऋणों से मुक्त होने की चर्चा है। तैत्तिरीय संहिता (३।३।८।१-२) ने 'कुसीद' शब्द का प्रयोग किया है जो धर्मशास्त्रों एवं स्मृतियों में 'ऋण देने-वाले' या ब्याज पर लेन-देन करने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है । शतपथ ब्राह्मण (१३।४।३।११) के पारिप्लव प्रकरण में 'कुसीदी' को अभिचार कर्म से सम्बन्धित कहा गया है। निरुक्त (६।३२) ने ऋग्वेद (३।५३।१४) पर टिप्पणी करते हुए वहां प्रयुक्त 'प्रमगन्द' शब्द का अर्थ यों लगाया है--'वह जो अति सूदखोर कुल में उत्पन्न हो।'३ पाणिनि ने 'उत्तमर्ण' (ऋणदाता) (१।४।३५), 'आधमर्य' (ऋण लेने वाले को स्थिति) (२।३७०), 'प्रतिभू' (जामिन) (२।३।३६), 'वृद्धि' (ब्याज) (५।१।४७) का प्रयोग किया है। पाणिनि (६।४।३१) ने 'कुसीदिक' एवं 'कुसीदिकी' की व्युत्पत्ति बतायी है। पाणिनि ने वाधुषिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जैसा कि आपस्तम्बधर्मसूत्र, बौधायनधर्मसूत्र ने किया है तथा कात्यायन ने पाणिनिसूत्र (४।४।३०) के वार्तिक में किया है । पाणिनि ने 'द्वगुणिक' या 'गुणिक' का, जो दुगुना या तिगुना सूद लेने की ओर संकेत करते हैं, प्रयोग किया है। ऋग्वेद (२०२४।१३) में ब्रह्मणस्पति को ऋणमादधि (ऋणलौटा लेनेवाला) कहा गया है और आदित्यों को, जो ऋत (अखिल नियम) के रक्षक हैं, ऋण इकट्ठा करने वाले कहा गया है (२।२७।४) । ऋग्वेद (८।३२।१६) में आया है कि सोमरस निकालने वाले पुरोहितों को देव-ऋण नहीं देना पड़ता। और भी देखिये ऋग्वेद (६।६१।१)।
____ इन बातों से स्पष्ट है कि ऋग्वेदिक काल में देव-ऋण एवं पितृ-ऋण की बृहत् कल्पना निर्धारित हो चुकी थी और इन ऋणों को क्रम से यज्ञ एवं पुत्रोत्पत्ति से चुकाया जा सकता है, ऐसा एक सामान्य विचार उत्पन्न हो गया था। देव-ऋण,ऋषि-ऋण एवं पितृ ऋण को कम से यज्ञाराधना, अध्ययनाध्यापन एवं सन्तानोत्पत्ति से चुकाना चाहिए, इसकी परिकल्पनाएँ स्पष्ट रूप से ऋग्वेद, तैत्तिरीय संहिता (६।३।१०।५), शतपथ ब्राह्मण (१७।२।११), ऐतरेय ब्राह्मण
१. उदाहरणार्थ, यदि क यह सिद्ध करता है कि उसने ख को ऋण दिया, किन्तु यदि ख यह सिद्ध करता है कि उसने ऋण लौटा दिया है तो यह पश्चात्कालीन कार्य निर्णयात्मक होगा। यदि क ऋण पर कोई खेत ख को बन्धक-स्वरूप देता है और पुनः वही खेत ग को बन्धक रूप में देता है, तो ख के साथ किया गया बन्धक-कार्य अपेक्षाकृत न्याय-सिद्ध माना जायगा। यह नियम आज के ट्रांस्फर आव प्रापर्टी एक्ट (४, सन् १८८२) के ४८ परिच्छेद के समान ही है।
२. अनणा अस्मिन्ननणाः परस्मिन ततीये लोके अनणाः स्याम। ये देवयाना उत पितयाणाः सर्वान्यथो अनणा आक्षीयेम ॥ ब्रा० ३७ : अथर्ववेद ६११७१३) में भी यह आया है थोडे-से अन्तर के साथ ।
३. मगन्दः कुसीदो मागन्दो मामागमिष्यतीति वंदाति तदपत्यं प्रमगन्दः अत्यन्तं कुसोदिकुलीनः । निरुक्त (६३३२) ।
www.jainelibrary.org
For Private & Personal Use Only
Jain Education International