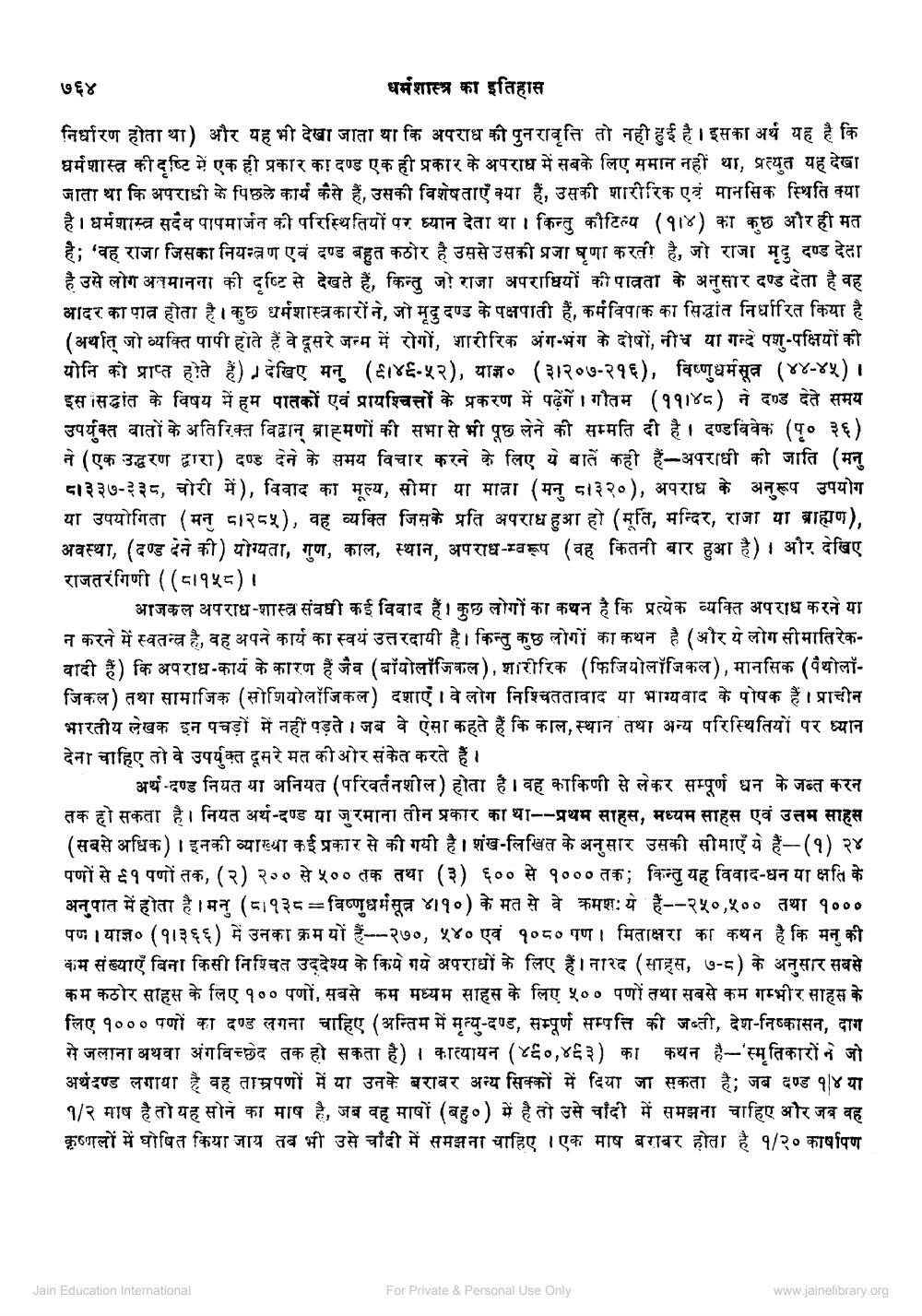________________
७६४
धर्मशास्त्र का इतिहास निर्धारण होता था) और यह भी देखा जाता था कि अपराध की पुनरावृत्ति तो नही हुई है। इसका अर्थ यह है कि धर्मशास्त्र की दृष्टि में एक ही प्रकार का दण्ड एक ही प्रकार के अपराध में सबके लिए समान नहीं था, प्रत्युत यह देखा जाता था कि अपराधी के पिछले कार्य कैसे हैं, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, उसकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति क्या है। धर्मशास्त्र सदैव पापमार्जन की परिस्थितियों पर ध्यान देता था। किन्तु कौटिल्य (१।४) का कुछ और ही मत है; 'वह राजा जिसका नियन्त्रण एवं दण्ड बहुत कठोर है उससे उसकी प्रजा घृणा करती है, जो राजा मृदु दण्ड देता है उसे लोग अवमानना की दृष्टि से देखते हैं, किन्तु जो राजा अपराधियों की पात्रता के अनुसार दण्ड देता है वह आदर का पात्र होता है। कुछ धर्मशास्त्रकारों ने, जो मृदु दण्ड के पक्षपाती हैं, कर्मविपाक का सिद्धांत निर्धारित किया है (अर्थात् जो व्यक्ति पापी होते हैं वे दूसरे जन्म में रोगों, शारीरिक अंग-भंग के दोषों, नीच या गन्दे पशु-पक्षियों की योनि को प्राप्त होते हैं)। देखिए मनु (६।४६-५२), याज्ञ० (३।२०७-२१६), विष्णुधर्मसूत्र (४४-४५) । इस सिद्धांत के विषय में हम पातकों एवं प्रायश्चित्तों के प्रकरण में पढ़ेंगें। गौतम (११।४८) ने दण्ड देते समय उपर्युक्त वातों के अतिरिक्त विद्वान ब्राह्मणों की सभा से भी पूछ लेने की सम्मति दी है। दण्डविवेक (पृ० ३६) ने (एक उद्धरण द्वारा) दण्ड देने के समय विचार करने के लिए ये बातें कही हैं-अपराधी को जाति (मनु ८.३३७-३३८, चोरी में), विवाद का मूल्य, सोमा या माना (मनु ८।३२०), अपराध के अनुरूप उपयोग या उपयोगिता (मनु ८।२८५), वह व्यक्ति जिसके प्रति अपराध हुआ हो (मूर्ति, मन्दिर, राजा या ब्राह्मण), अवस्था, (दण्ड देने की) योग्यता, गुण, काल, स्थान, अपराध-म्वरूप (वह कितनी बार हुआ है)। और देखिए राजतरंगिणी ((८।१५८)।
आजकल अपराध-शास्त्र संबंधी कई विवाद हैं। कुछ लोगों का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति अपराध करने या न करने में स्वतन्त्र है, वह अपने कार्य का स्वयं उत्तरदायी है। किन्तु कुछ लोगों का कथन है (और ये लोग सीमातिरेकवादी हैं) कि अपराध-कार्य के कारण हैं जैव (बॉयोलॉजिकल), शारीरिक (फिजियोलॉजिकल), मानसिक (पैथोलॉजिकल) तथा सामाजिक (सोशियोलॉजिकल) दशाएँ। वे लोग निश्चिततावाद या भाग्यवाद के पोषक हैं। प्राचीन भारतीय लेखक इन पचड़ों में नहीं पड़ते। जब वे ऐसा कहते हैं कि काल, स्थान तथा अन्य परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए तो वे उपर्युक्त दूसरे मत की ओर संकेत करते हैं।
अर्थ-दण्ड नियत या अनियत (परिवर्तनशील) होता है। वह काकिणी से लेकर सम्पूर्ण धन के जब्त करन तक हो सकता है। नियत अर्थ-दण्ड या जरमाना तीन प्रकार का था--प्रथम साहस, मध्यम साहस एवं उत्तम साहस (सबसे अधिक)। इनकी व्याख्या कई प्रकार से की गयी है। शंख-लिखित के अनुसार उसकी सीमाएँ ये हैं-(१) २४ पणों से ६१ पणों तक, (२) २०० से ५०० तक तथा (३) ६०० से १००० तक; किन्तु यह विवाद-धन या क्षति के अनुपात में होता है। मनु (८.१३८ = विष्णुधर्मसूत्र ४।१०) के मत से वे क्रमश: ये हैं--२५०,५०० तथा १००० पण । याज्ञ० (१।३६६) में उनका क्रम यों हैं--२७०, ५४० एवं १०८० पण। मिताक्षरा का कथन है कि मनु की कम संख्याएँ बिना किसी निश्चित उद्देश्य के किये गये अपराधों के लिए हैं। नारद (साहस, ७-८) के अनुसार सबसे कम कठोर साहस के लिए १०० पणों, सबसे कम मध्यम साहस के लिए ५०० पणों तथा सबसे कम गम्भीर साहस के लिए १००० पणों का दण्ड लगना चाहिए (अन्तिम में मृत्यु-दण्ड, सम्पूर्ण सम्पत्ति की जब्ती, देश-निष्कासन, दाग से जलाना अथवा अंगविच्छेद तक हो सकता है)। कात्यायन (४६०,४६३) का कथन है-'स्मृतिकारों ने जो अर्थदण्ड लगाया है वह ताम्रपणों में या उनके बराबर अन्य सिक्कों में दिया जा सकता है; जब दण्ड १/४ या १/२ माष है तो यह सोने का माष है, जब वह माषों (बहु०) में है तो उसे चाँदी में समझना चाहिए और जब वह कृष्णलों में घोषित किया जाय तब भी उसे चाँदी में समझना चाहिए । एक माष बराबर होता है १/२० कार्षापण
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org