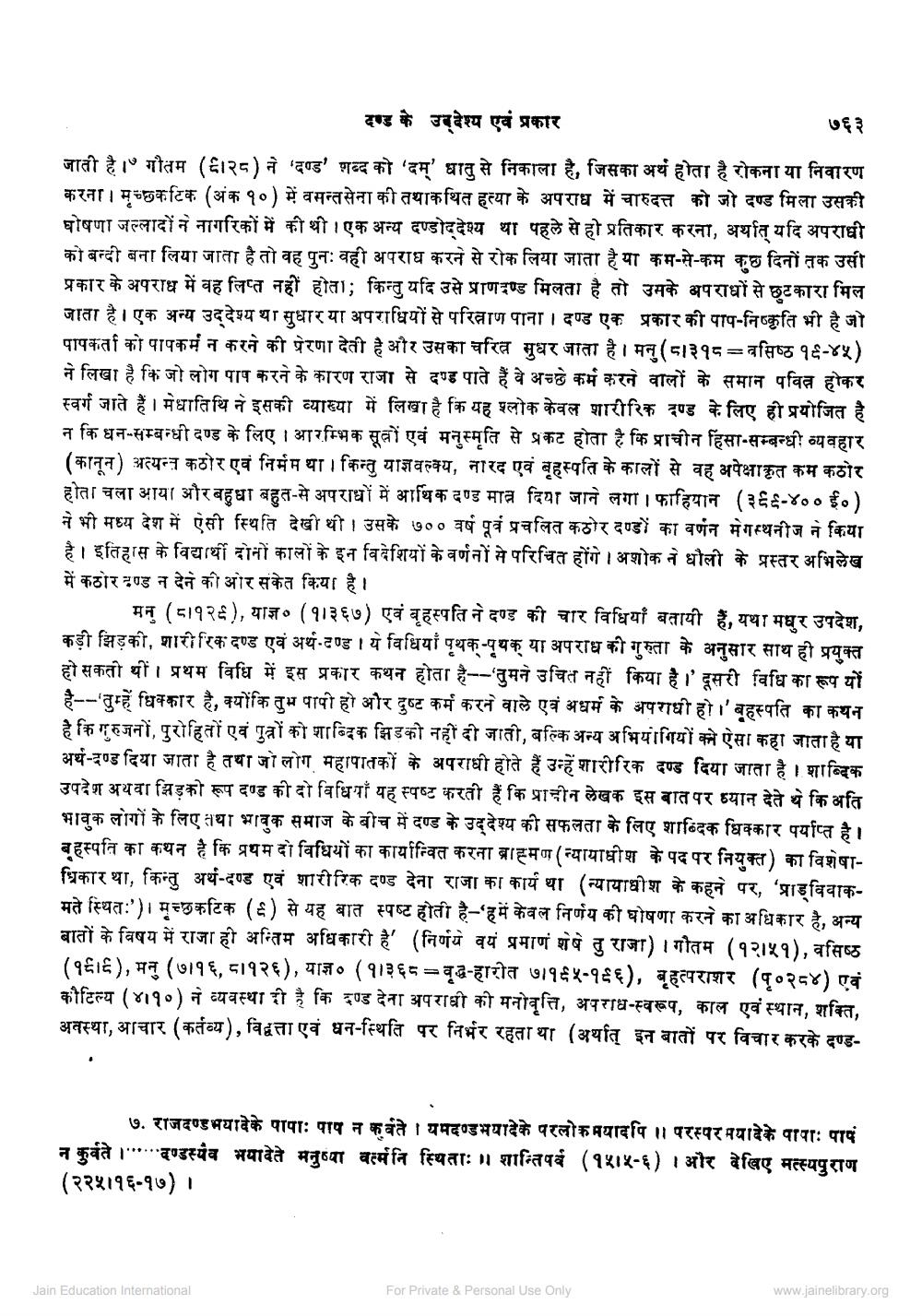________________
दण्ड के उदेश्य एवं प्रकार
७६३
प्रकार की पाप-निष्कृति भी है जो मनु ( ८ । ३१८ = वसिष्ठ १६-४५ )
जाती है । गौतम ( ६।२८) ने 'दण्ड' शब्द को 'दम्' धातु से निकाला है, जिसका अर्थ होता है रोकना या निवारण करना । मृच्छकटिक ( अंक १० ) में वसन्तसेना की तथाकथित हत्या के अपराध में चारुदत्त को जो दण्ड मिला उसकी घोषणा जल्लादों ने नागरिकों में की थी। एक अन्य दण्डोद्देश्य था पहले से हो प्रतिकार करना, अर्थात् यदि अपराधी hot बन्दी बना लिया जाता है तो वह पुनः वही अपराध करने से रोक लिया जाता है या कम-से-कम कुछ दिनों तक उसी प्रकार के अपराध में वह लिप्त नहीं होता; किन्तु यदि उसे प्राणदण्ड मिलता तो उसके अपराधों से छुटकारा मिल जाता है। एक अन्य उद्देश्य था सुधार या अपराधियों से परित्राण पाना । दण्ड एक पापकर्ता को पापकर्म न करने की प्रेरणा देती है और उसका चरित्र सुधर जाता है । ने लिखा है कि जो लोग पाप करने के कारण राजा से दण्ड पाते हैं वे अच्छे कर्म करने वालों के समान पवित्र होकर स्वर्ग जाते हैं । मेधातिथि ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि यह श्लोक केवल शारीरिक दण्ड के लिए ही प्रयोजित है न कि धन-सम्बन्धी दण्ड के लिए । आरम्भिक सूत्रों एवं मनुस्मृति से प्रकट होता है कि प्राचीन हिंसा-सम्बन्धी व्यवहार (कानून) अत्यन्त कठोर एवं निर्मम था । किन्तु याज्ञवल्क्य, नारद एवं बृहस्पति के कालों से वह अपेक्षाकृत कम कठोर होता चला आया और बहुधा बहुत से अपराधों में आर्थिक दण्ड मात्र दिया जाने लगा। फाहियान ( ३६६ -४००ई० ) ने भी मध्य देश में ऐसी स्थिति देखी थी। उसके ७०० वर्ष पूर्व प्रचलित कठोर दण्डों का वर्णन मेगस्थनीज ने किया है । इतिहास के विद्यार्थी दोनों कालों के इन विदेशियों के वर्णनों से परिचित होंगे। अशोक ने धौली के प्रस्तर अभिलेख में कठोर दण्ड न देने की ओर संकेत किया है ।
मनु (८।१२६), याज्ञ० ( १।३६७ ) एवं बृहस्पति ने दण्ड की चार विधियां बतायी हैं, यथा मधुर उपदेश, कड़ी झिड़की, शारीरिक दण्ड एवं अर्थ- दण्ड । ये विधियाँ पृथक्-पृथक् या अपराध की गुरुता के अनुसार साथ ही प्रयुक्त हो सकती थीं । प्रथम विधि में इस प्रकार कथन होता है--'तुमने उचित नहीं किया है।' दूसरी विधि का रूप यों है -- तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि तुम पापी हो और दुष्ट कर्म करने वाले एवं अधर्म के अपराधी हो ।' बृहस्पति का कथन है कि गुरुजनों, पुरोहितों एवं पुत्त्रों को शाब्दिक झिड़की नहीं दी जाती, बल्कि अन्य अभियोगियों को ऐसा कहा जाता है या अर्थ-दण्ड दिया जाता है तथा जो लोग महापातकों के अपराधी होते हैं उन्हें शारीरिक दण्ड दिया जाता है। शाब्दिक उपदेश अथवा झिड़को रूप दण्ड की दो विधियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि प्राचीन लेखक इस बात पर ध्यान देते थे कि अति भावुक लोगों के लिए तथा भावुक समाज के बीच में दण्ड के उद्देश्य की सफलता के लिए शाब्दिक धिक्कार पर्याप्त है। बृहस्पति का कथन है कि प्रथम दो विधियों का कार्यान्वित करना ब्राह्मण ( न्यायाधीश के पद पर नियुक्त) का विशेषाधिकार था, किन्तु अर्थ-दण्ड एवं शारीरिक दण्ड देना राजा का कार्य था ( न्यायाधीश के कहने पर, 'प्राड्विवाकते स्थितः ') । मृच्छकटिक (ई) से यह बात स्पष्ट होती है- 'हमें केवल निर्णय की घोषणा करने का अधिकार है, अन्य बातों के विषय में राजा ही अन्तिम अधिकारी है' (निर्णये वयं प्रमाणं शेषे तु राजा ) । गौतम ( १२ । ५१ ), वसिष्ठ (१६६), मनु (७।१६, ८।१२६), याज्ञ० ( १।३६८ वृद्ध हारीत ७।१६५ - १६६ ), बृहत्पराशर ( पृ०२८४) एवं कौटिल्य (४।१०) ने व्यवस्था दी है कि दण्ड देना अपराधी की मनोवृत्ति, अपराध स्वरूप, काल एवं स्थान, शक्ति, अवस्था, आचार ( कर्तव्य ), विद्वत्ता एवं धन स्थिति पर निर्भर रहता था ( अर्थात् इन बातों पर विचार करके दण्ड
७. राजदण्डभयादेके पापाः पाप न कुर्वते । यमदण्डभयादेके परलोक मयादपि ।। परस्पर मयादेके पापाः पा न कुर्वते । ...... दण्डस्यैव भयादेते मनुष्या वर्त्मनि स्थिताः ॥ शान्तिपर्व ( १५।५-६ ) । और देखिए मत्स्यपुराण (२२५।१६-१७) ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org