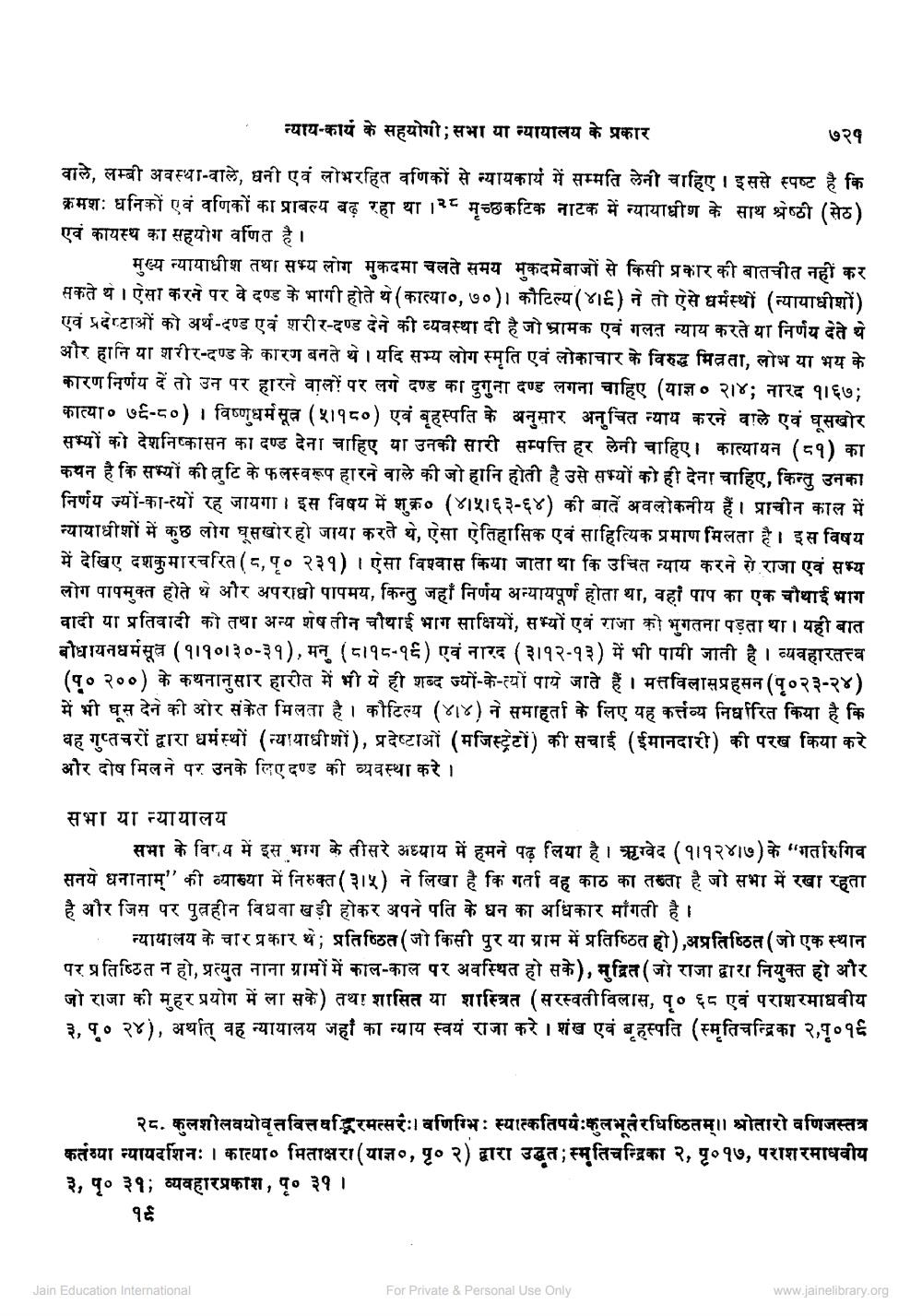________________
न्याय-कार्य के सहयोगी; सभा या न्यायालय के प्रकार
७२१
वाले, लम्बी अवस्था-वाले, धनी एवं लोभरहित वणिकों से न्यायकार्य में सम्मति लेनी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि क्रमशः धनिकों एवं वणिकों का प्राबल्य बढ़ रहा था । २८ मृच्छकटिक नाटक में न्यायाधीश के साथ श्रेष्ठी (सेठ) एवं कायस्थ का सहयोग वणित है।।
___ मुख्य न्यायाधीश तथा सभ्य लोग मुकदमा चलते समय मुकदमेबाजों से किसी प्रकार की बातचीत नहीं कर सकते थे। ऐसा करने पर वे दण्ड के भागी होते थे (कात्या०,७०)। कौटिल्य (४।६) ने तो ऐसे धर्मस्थों (न्यायाधीशों) एवं प्रदेष्टाओं को अर्थ-दण्ड एवं शरीर-दण्ड देने की व्यवस्था दी है जोभ्रामक एवं गलत न्याय करते या निर्णय देते थे और हानि या शरीर-दण्ड के कारण बनते थे । यदि सभ्य लोग स्मृति एवं लोकाचार के विरुद्ध मित्रता, लोभ या भय के कारण निर्णय दें तो उन पर हारने वालों पर लगे दण्ड का दुगुना दण्ड लगना चाहिए (याज्ञ० २।४; नारद १।६७; कात्या० ७६-८०) । विष्णुधर्म सूत्र (५।१८०) एवं बृहस्पति के अनुसार अनुचित न्याय करने वाले एवं घूसखोर सभ्यों को देशनिष्कासन का दण्ड देना चाहिए या उनकी सारी सम्पत्ति हर लेनी चाहिए। कात्यायन (८१) का कथन है कि सभ्यों की त्रुटि के फलस्वरूप हारने वाले की जो हानि होती है उसे सभ्यों को ही देना चाहिए, किन्तु उनका निर्णय ज्यों-का-त्यों रह जायगा। इस विषय में शुक्र० (४।५।६३-६४) की बातें अवलोकनीय हैं। प्राचीन काल में न्यायाधीशों में कुछ लोग घूसखोर हो जाया करते थे, ऐसा ऐतिहासिक एवं साहित्यिक प्रमाण मिलता है। इस विषय में देखिए दशकुमारचरित (८, पृ० २३१) । ऐसा विश्वास किया जाता था कि उचित न्याय करने से राजा एवं सभ्य लोग पापमुक्त होते थे और अपराधो पापमय, किन्तु जहाँ निर्णय अन्यायपूर्ण होता था, वहां पाप का एक चौथाई भाग वादी या प्रतिवादी को तथा अन्य शेष तीन चौथाई भाग साक्षियों, सभ्यों एवं राजा को भुगतना पड़ता था। यही बात बौधायनधर्मसूत्र (१।१०।३०-३१), मनु (८।१८-१६) एवं नारद (३।१२-१३) में भी पायी जाती है । व्यवहारतत्त्व (प० २००) के कथनानुसार हारीत में भी ये ही शब्द ज्यों-के-त्यों पाये जाते हैं । मत्तविलासप्रहसन (पृ०२३-२४) में भी घूस देने की ओर संकेत मिलता है। कौटिल्य (४१४) ने समाहर्ता के लिए यह कर्तव्य निर्धारित किया है कि वह गुप्तचरों द्वारा धर्मस्थों (न्यायाधीशों), प्रदेष्टाओं (मजिस्ट्रेटों) की सचाई (ईमानदारी) की परख किया करे और दोष मिलने पर उनके लिए दण्ड की व्यवस्था करे ।
सभा या न्यायालय
सभा के विषय में इस भाग के तीसरे अध्याय में हमने पढ़ लिया है। ऋग्वेद (१।१२४।७) के "गारुगिव सनये धनानाम्" की व्याख्या में निरुक्त (३।५) ने लिखा है कि गर्ता वह काठ का तख्ता है जो सभा में रखा रहता है और जिस पर पुत्रहीन विधवा खड़ी होकर अपने पति के धन का अधिकार माँगती है।
. न्यायालय के चार प्रकार थे; प्रतिष्ठित (जो किसी पुर या ग्राम में प्रतिष्ठित हो),अप्रतिष्ठित (जो एक स्थान पर प्रतिष्ठित न हो, प्रत्युत नाना ग्रामों में काल-काल पर अवस्थित हो सके), मुद्रित (जो राजा द्वारा नियुक्त हो और जो राजा की मुहर प्रयोग में ला सके) तथा शासित या शास्त्रित (सरस्वतीविलास, पृ० ६८ एवं पराशरमाधवीय ३, पृ० २४), अर्थात् वह न्यायालय जहाँ का न्याय स्वयं राजा करे । शंख एवं बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २,पृ०१६
२८. कुलशीलवयोवृत्तवित्तद्भिरमत्सरः। वणिग्भिः स्यात्कतिपयःकुलभूतैरधिष्ठितम्॥ श्रोतारो वणिजस्तत्र कर्तव्या न्यायदर्शिनः । कात्या० मिताक्षरा (याज्ञ०, पृ० २) द्वारा उद्धृत ; स्मृतिचन्द्रिका २, पृ०१७, पराशरमाधवीय ३, पृ० ३१; व्यवहारप्रकाश , पृ० ३१ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org