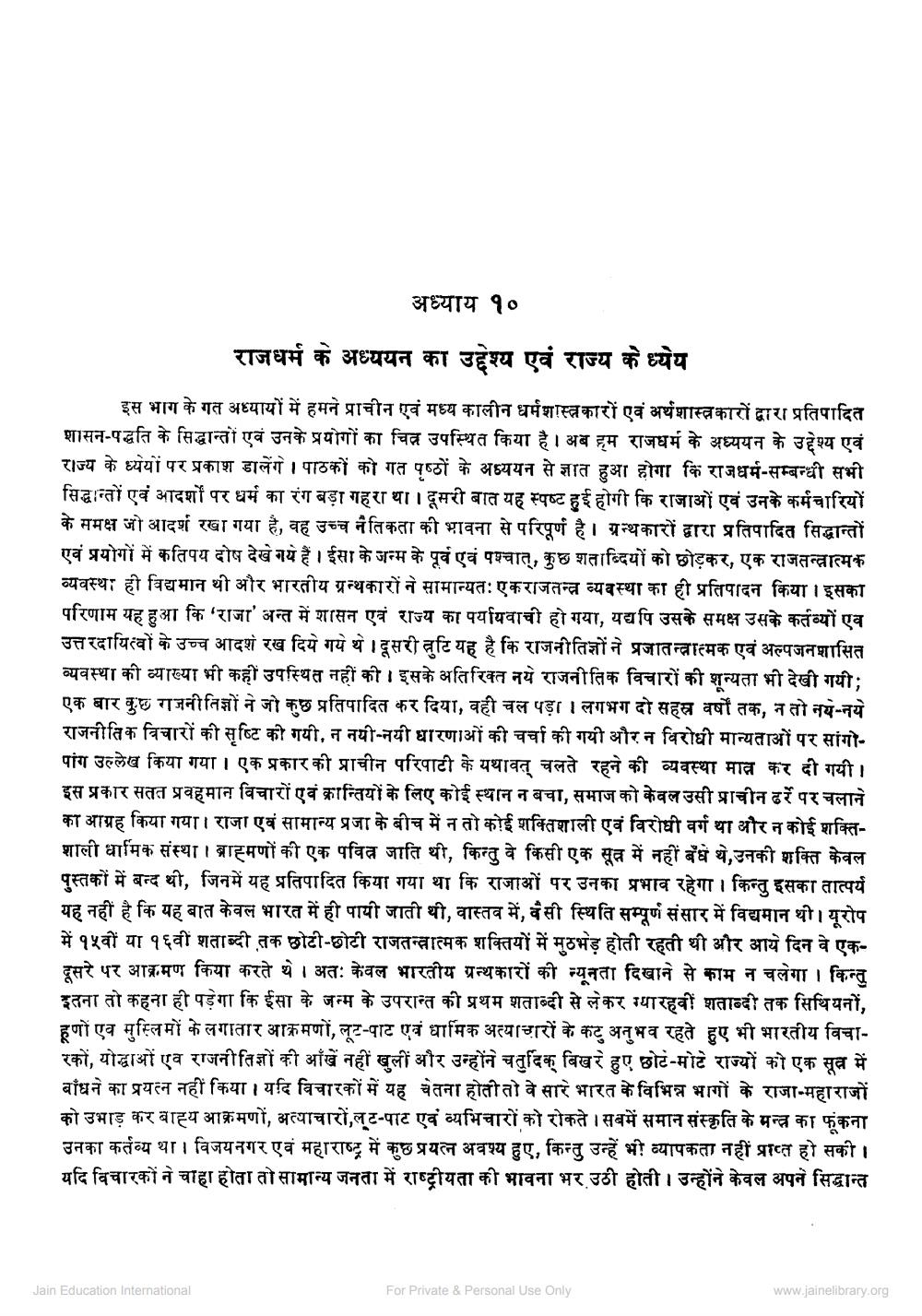________________
अध्याय १०
राजधर्म के अध्ययन का उद्देश्य एवं राज्य के ध्येय इस भाग के गत अध्यायों में हमने प्राचीन एवं मध्य कालीन धर्मशास्त्रकारों एवं अर्थशास्त्रकारों द्वारा प्रतिपादित शासन-पद्धति के सिद्धान्तों एवं उनके प्रयोगों का चिन्न उपस्थित किया है। अब हम राजधर्म के अध्ययन के उद्देश्य एवं राज्य के ध्येयों पर प्रकाश डालेंगे । पाठकों को गत पृष्ठों के अध्ययन से ज्ञात हुआ होगा कि राजधर्म-सम्बन्धी सभी सिद्धान्तों एवं आदर्शो पर धर्म का रंग बड़ा गहरा था। दूसरी बात यह स्पष्ट हुई होगी कि राजाओं एवं उनके कर्मचारियों के समक्ष जो आदर्श रखा गया है, वह उच्च नैतिकता की भावना से परिपूर्ण है। ग्रन्थकारों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं प्रयोगों में कतिपय दोष देखे गये हैं । ईसा के जन्म के पूर्व एवं पश्चात्, कुछ शताब्दियों को छोड़कर, एक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था ही विद्यमान थी और भारतीय ग्रन्थकारों ने सामान्यतः एकराजतन्त्र व्यवस्था का ही प्रतिपादन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 'राजा' अन्त में शासन एवं राज्य का पर्यायवाची हो गया, यद्यपि उसके समक्ष उसके कर्तव्यों एव उत्तरदायित्वों के उच्च आदर्श रख दिये गये थे। दूसरी त्रुटि यह है कि राजनीतिज्ञों ने प्रजातन्त्रात्मक एवं अल्पजनशासित व्यवस्था की व्याख्या भी कहीं उपस्थित नहीं की। इसके अतिरिक्त नये राजनीतिक विचारों की शून्यता भी देखी गयी; एक बार कुछ गजनीतिज्ञों ने जो कुछ प्रतिपादित कर दिया, वही चल पड़ा । लगभग दो सहस्र वर्षों तक, न तो नये-नये राजनीतिक विचारों की सृष्टि की गयी, न नयी-नयी धारणाओं की चर्चा की गयी और न विरोधी मान्यताओं पर सांगोपांग उल्लेख किया गया। एक प्रकार की प्राचीन परिपाटी के यथावत् चलते रहने की व्यवस्था मान कर दी गयी। इस प्रकार सतत प्रवहमान विचारों एवं क्रान्तियों के लिए कोई स्थान न बचा, समाज को केवल उसी प्राचीन ढर्रे पर चलाने का आग्रह किया गया। राजा एवं सामान्य प्रजा के बीच में न तो कोई शक्तिशाली एवं विरोधी वर्ग था और न कोई शक्तिशाली धार्मिक संस्था । ब्राह्मणों की एक पवित्र जाति थी, किन्तु वे किसी एक सूत्र में नहीं बंधे थे,उनकी शक्ति केवल पुस्तकों में बन्द थी, जिनमें यह प्रतिपादित किया गया था कि राजाओं पर उनका प्रभाव रहेगा। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह बात केवल भारत में ही पायी जाती थी, वास्तव में, वैसी स्थिति सम्पूर्ण संसार में विद्यमान थी। यूरोप में १५वीं या १६वीं शताब्दी तक छोटी-छोटी राजतन्त्रात्मक शक्तियों में मुठभेड़ होती रहती थी और आये दिन वे एकदूसरे पर आक्रमण किया करते थे । अतः केवल भारतीय ग्रन्थकारों की न्यूनता दिखाने से काम न चलेगा। किन्तु इतना तो कहना ही पड़ेगा कि ईसा के जन्म के उपरान्त की प्रथम शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक सिथियनों, हणों एव मुस्लिमों के लगातार आक्रमणों, लूट-पाट एवं धार्मिक अत्याचारों के कटु अनुभव रहते हुए भी भारतीय विचारकों, योद्धाओं एव राजनीतिज्ञों की आँखें नहीं खुलीं और उन्होंने चतुर्दिक् बिखरे हुए छोटे-मोटे राज्यों को एक सूत्र में बाँधने का प्रयत्न नहीं किया। यदि विचारकों में यह चेतना होती तो वे सारे भारत के विभिन्न भागों के राजा-महाराजों को उभाड़ कर बाह्य आक्रमणों, अत्याचारों,लट-पाट एवं व्यभिचारों को रोकते । सबमें समान संस्कृति के मन्त्र का फूंकना उनका कर्तव्य था। विजयनगर एवं महाराष्ट्र में कुछ प्रयत्न अवश्य हुए, किन्तु उन्हें भी व्यापकता नहीं प्राप्त हो सकी। यदि विचारकों ने चाहा होता तो सामान्य जनता में राष्ट्रीयता की भावना भर उठी होती। उन्होंने केवल अपने सिद्धान्त
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org