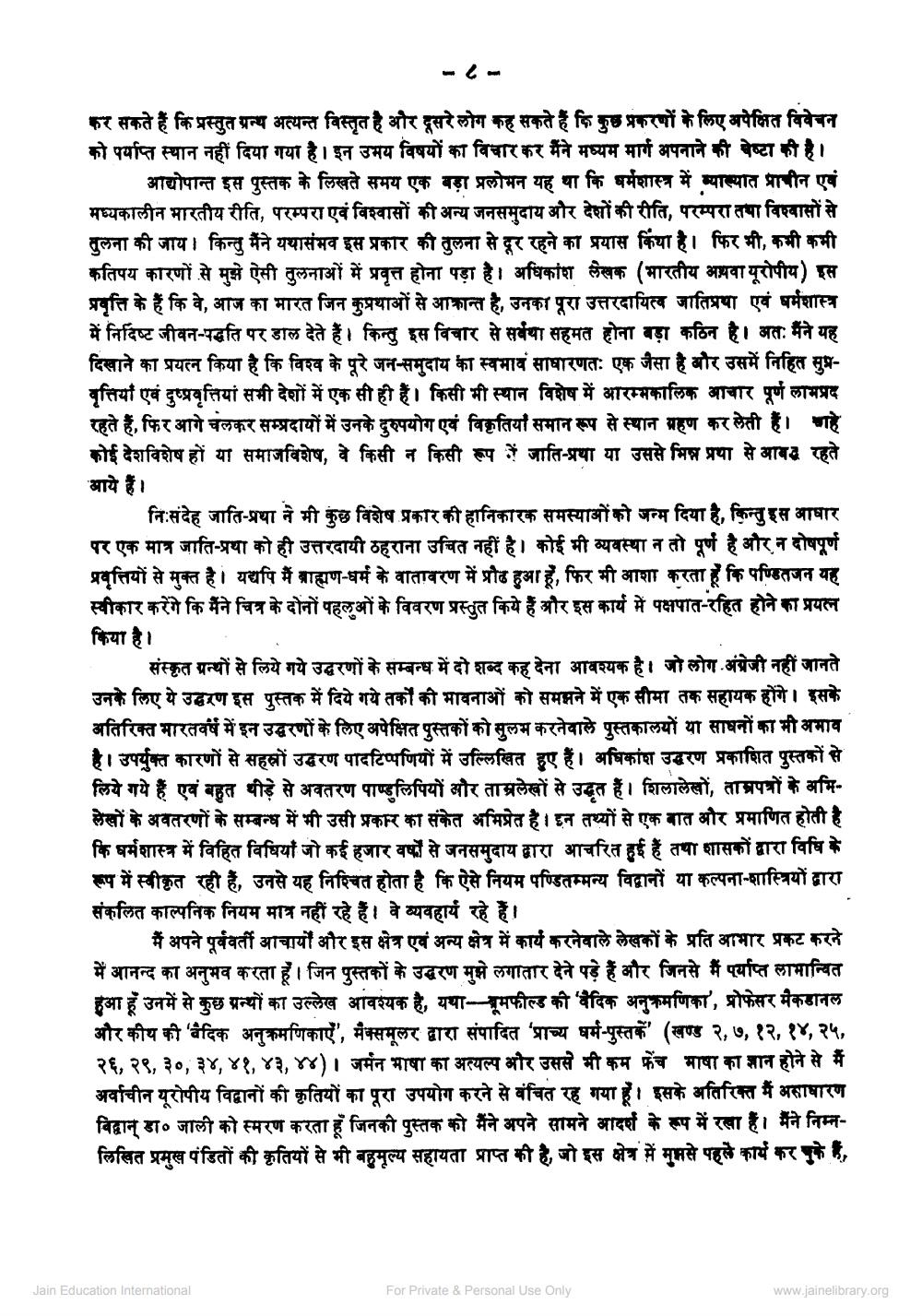________________
कर सकते हैं कि प्रस्तुत ग्रन्थ अत्यन्त विस्तृत है और दूसरे लोग कह सकते हैं कि कुछ प्रकरणों के लिए अपेक्षित विवेचन को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। इन उभय विषयों का विचार कर मैंने मध्यम मार्ग अपनाने की चेष्टा की है।
__ आद्योपान्त इस पुस्तक के लिखते समय एक बड़ा प्रलोभन यह था कि धर्मशास्त्र में व्याख्यात प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय रीति, परम्परा एवं विश्वासों की अन्य जनसमुदाय और देशों की रीति, परम्परा तथा विश्वासों से तुलना की जाय। किन्तु मैंने यथासंभव इस प्रकार की तुलना से दूर रहने का प्रयास किया है। फिर भी, कभी कमी कतिपय कारणों से मुझे ऐसी तुलनाओं में प्रवृत्त होना पड़ा है। अधिकांश लेखक (भारतीय अथवा यूरोपीय) इस प्रवृत्ति के हैं कि वे, आज का भारत जिन कुप्रथाओं से आक्रान्त है, उनका पूरा उत्तरदायित्व जातिप्रथा एवं धर्मशास्त्र में निर्दिष्ट जीवन-पद्धति पर डाल देते हैं। किन्तु इस विचार से सर्वथा सहमत होना बड़ा कठिन है। अतः मैंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि विश्व के पूरे जन-समुदाय का स्वभावं साधारणतः एक जैसा है और उसमें निहित सुभवृत्तियां एवं दुष्प्रवृत्तियां सभी देशों में एक सी ही हैं। किसी भी स्थान विशेष में आरम्भकालिक आचार पूर्ण लाभप्रद रहते हैं, फिर आगे चलकर सम्प्रदायों में उनके दुरुपयोग एवं विकृतियां समान रूप से स्थान ग्रहण कर लेती हैं। हे कोई देशविशेष हों या समाजविशेष, वे किसी न किसी रूप में जाति-प्रथा या उससे भिन्न प्रथा से आवत रहते आये हैं।
निःसंदेह जाति-प्रथा ने भी कुछ विशेष प्रकार की हानिकारक समस्याओं को जन्म दिया है, किन्तु इस आधार पर एक मात्र जाति-प्रथा को ही उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। कोई भी व्यवस्था न तो पूर्ण है और न दोषपूर्ण प्रवृत्तियों से मुक्त है। यद्यपि मैं ब्राह्मण-धर्म के वातावरण में प्रौढ हुआ हूँ, फिर भी आशा करता हूँ कि पण्डितजन यह स्वीकार करेंगे कि मैंने चित्र के दोनों पहलुओं के विवरण प्रस्तुत किये हैं और इस कार्य में पक्षपात-रहित होने का प्रयल किया है।
संस्कृत ग्रन्थों से लिये गये उद्धरणों के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना आवश्यक है। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते उनके लिए ये उद्धरण इस पुस्तक में दिये गये तकों की भावनाओं को समझने में एक सीमा तक सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में इन उद्धरणों के लिए अपेक्षित पुस्तकों को सुलभ करनेवाले पुस्तकालयों या साधनों का भी अभाव है। उपर्युक्त कारणों से सहस्रों उद्धरण पादटिप्पणियों में उल्लिखित हुए हैं। अधिकांश उद्धरण प्रकाशित पुस्तकों से लिये गये हैं एवं बहत थोडे से अवतरण पाण्डलिपियों और ताम्रलेखों से उद्धत हैं। शिलालेखों, ताम्रपत्रों के अभिलेखों के अवतरणों के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार का संकेत अभिप्रेत है। इन तथ्यों से एक बात और प्रमाणित होती है कि धर्मशास्त्र में विहित विधियों जो कई हजार वर्षों से जनसमुदाय द्वारा आचरित हुई हैं तथा शासकों द्वारा विधि के रूप में स्वीकृत रही हैं, उनसे यह निश्चित होता है कि ऐसे नियम पण्डितम्मन्य विद्वानों या कल्पना-शास्त्रियों द्वारा संकलित काल्पनिक नियम मात्र नहीं रहे हैं। वे व्यवहार्य रहे हैं।
मैं अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और इस क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में कार्य करनेवाले लेखकों के प्रति आभार प्रकट करने में आनन्द का अनुभव करता हूँ। जिन पुस्तकों के उद्धरण मुझे लगातार देने पड़े हैं और जिनसे मैं पर्याप्त लाभान्वित हुआ हूँ उनमें से कुछ अन्यों का उल्लेख आवश्यक है, यया-यूमफील्ड की 'वैदिक अनुक्रमणिका', प्रोफेसर मैकडानल
और कीथ की 'वैदिक अनुक्रमणिकाएँ', मैक्समूलर द्वारा संपादित 'प्राच्य धर्म-पुस्तकें' (खण्ड २, ७, १२, १४, २५, २६, २९, ३०, ३४, ४१, ४३, ४४)। जर्मन भाषा का अत्यल्प और उससे भी कम फ्रेंच भाषा का ज्ञान होने से मैं अर्वाचीन यूरोपीय विद्वानों की कृतियों का पूरा उपयोग करने से वंचित रह गया है। इसके अतिरिक्त मैं असाधारण विद्वान् डा० जाली को स्मरण करता हूँ जिनकी पुस्तक को मैंने अपने सामने आदर्श के रूप में रखा है। मैंने निम्नलिखित प्रमुख पंडितों की कृतियों से भी बहुमूल्य सहायता प्राप्त की है, जो इस क्षेत्र में मुमसे पहले कार्य कर चुके हैं,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org