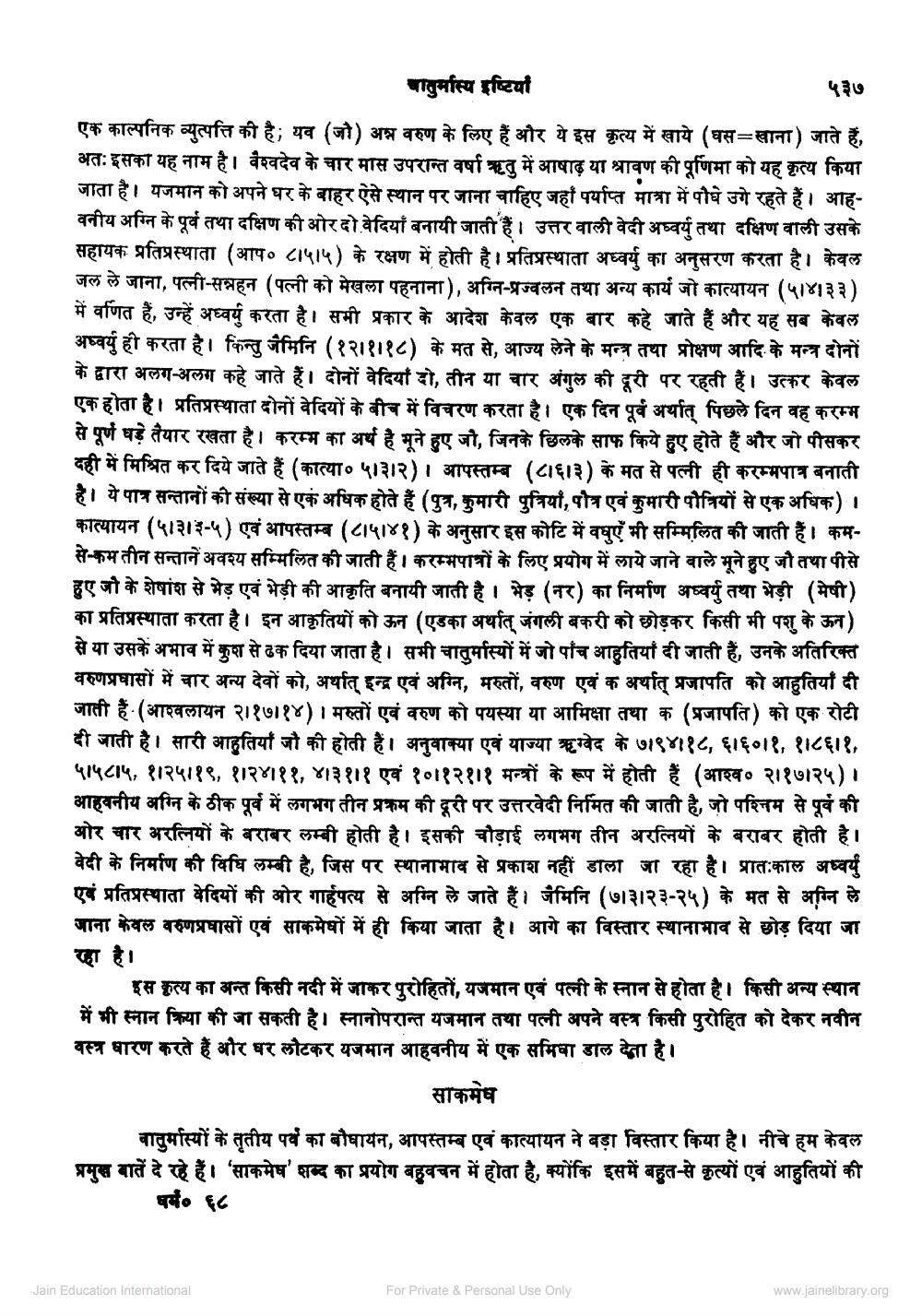________________
चातुर्मास्य इष्टियां
५३७ एक काल्पनिक व्युत्पत्ति की है; यव (जो) अन्न वरुण के लिए हैं और ये इस कृत्य में खाये (घस खाना) जाते हैं, अतः इसका यह नाम है। वैश्वदेव के चार मास उपरान्त वर्षा ऋतु में आषाढ़ या श्रावण की पूर्णिमा को यह कृत्य किया जाता है। यजमान को अपने घर के बाहर ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर्याप्त मात्रा में पौधे उगे रहते हैं। आहवनीय अग्नि के पूर्व तथा दक्षिण की ओर दो वेदियाँ बनायी जाती हैं। उत्तर वाली वेदी अध्वर्यु तथा दक्षिण वाली उसके सहायक प्रतिप्रस्थाता (आप० ८।५।५) के रक्षण में होती है। प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यु का अनुसरण करता है। केवल जल ले जाना, पत्नी-सन्नहन (पत्नी को मेखला पहनाना), अग्नि-प्रज्वलन तथा अन्य कार्य जो कात्यायन (५।४।३३) में वर्णित हैं, उन्हें अध्वर्यु करता है। सभी प्रकार के आदेश केवल एक बार कहे जाते हैं और यह सब केवल अध्वर्यु ही करता है। किन्तु जैमिनि (१२।१।१८) के मत से, आज्य लेने के मन्त्र तथा प्रोक्षण आदि के मन्त्र दोनों के द्वारा अलग-अलग कहे जाते हैं। दोनों वेदियाँ दो, तीन या चार अंगुल की दूरी पर रहती हैं। उत्कर केवल एक होता है। प्रतिप्रस्थाता दोनों वेदियों के बीच में विचरण करता है। एक दिन पूर्व अर्थात् पिछले दिन वह करम्म से पूर्ण घड़े तैयार रखता है। करम्भ का अर्थ है भूने हुए जौ, जिनके छिलके साफ किये हुए होते हैं और जो पीसकर दही में मिश्रित कर दिये जाते हैं (कात्या० ५।३।२)। आपस्तम्ब (८६३) के मत से पत्नी ही करम्मपात्र बनाती है। ये पात्र सन्तानों की संख्या से एक अधिक होते हैं (पुत्र, कुमारी पुत्रियां, पौत्र एवं कुमारी पौत्रियों से एक अधिक)। कात्यायन (५।३।३-५) एवं आपस्तम्ब (८।५।४१) के अनुसार इस कोटि में वधुएँ भी सम्मिलित की जाती हैं। कमसे-कम तीन सन्ताने अवश्य सम्मिलित की जाती हैं। करम्मपात्रों के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले भूने हुए जौ तथा पीसे हुए जो के शेषांश से भेड़ एवं भेड़ी की आकृति बनायी जाती है । भेड़ (नर) का निर्माण अध्वर्यु तथा भेड़ी (मेषी) का प्रतिप्रस्थाता करता है। इन आकृतियों को ऊन (एडका अर्थात् जंगली बकरी को छोड़कर किसी भी पशु के ऊन) से या उसके अभाव में कुश से ढक दिया जाता है। सभी चातुर्मास्यों में जो पाँच आहुतियां दी जाती हैं, उनके अतिरिक्त वरुणप्रघासों में चार अन्य देवों को, अर्थात् इन्द्र एवं अग्नि, मरुतों, वरुण एवं क अर्थात् प्रजापति को आहुतियां दी जाती हैं (आश्वलायन २।१७।१४) । मरुतों एवं वरुण को पयस्या या आमिक्षा तथा क (प्रजापति) को एक रोटी दी जाती है। सारी आहुतियाँ जौ की होती हैं। अनुवाक्या एवं याज्या ऋग्वेद के ७१९४११८, ६।६०।१, ११८६।१, ५।५८।५, १२५।१९, १०२४।११, ४।३१।१ एवं १०।१२।१ मन्त्रों के रूप में होती हैं (आश्व० २।१७।२५)। आहवनीय अग्नि के ठीक पूर्व में लगभग तीन प्रक्रम की दूरी पर उत्तरवेदी निर्मित की जाती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर चार अरलियों के बराबर लम्बी होती है। इसकी चौड़ाई लगभग तीन अरनियों के बराबर होती है। वेदी के निर्माण की विधि लम्बी है, जिस पर स्थानामाव से प्रकाश नहीं डाला जा रहा है। प्रातःकाल अध्वर्यु एवं प्रतिप्रस्थाता वेदियों की ओर गार्हपत्य से अग्नि ले जाते हैं। जैमिनि (७।३।२३-२५) के मत से अग्नि ले जाना केवल वरुणप्रयासों एवं साकमेषों में ही किया जाता है। आगे का विस्तार स्थानाभाव से छोड़ दिया जा
___ इस कृत्य का अन्त किसी नदी में जाकर पुरोहितों, यजमान एवं पत्नी के स्नान से होता है। किसी अन्य स्थान में भी स्नान क्रिया की जा सकती है। स्नानोपरान्त यजमान तथा पत्नी अपने वस्त्र किसी पुरोहित को देकर नवीन वस्त्र धारण करते हैं और घर लौटकर यजमान आहवनीय में एक समिधा डाल देता है।
साकमेष चातुर्मास्यों के तृतीय पर्व का बौधायन, आपस्तम्ब एवं कात्यायन ने बड़ा विस्तार किया है। नीचे हम केवल प्रमुख बातें दे रहे हैं। 'साकमेष' शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, क्योंकि इसमें बहुत-से कृत्यों एवं आहुतियों की
धर्व० ६८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org